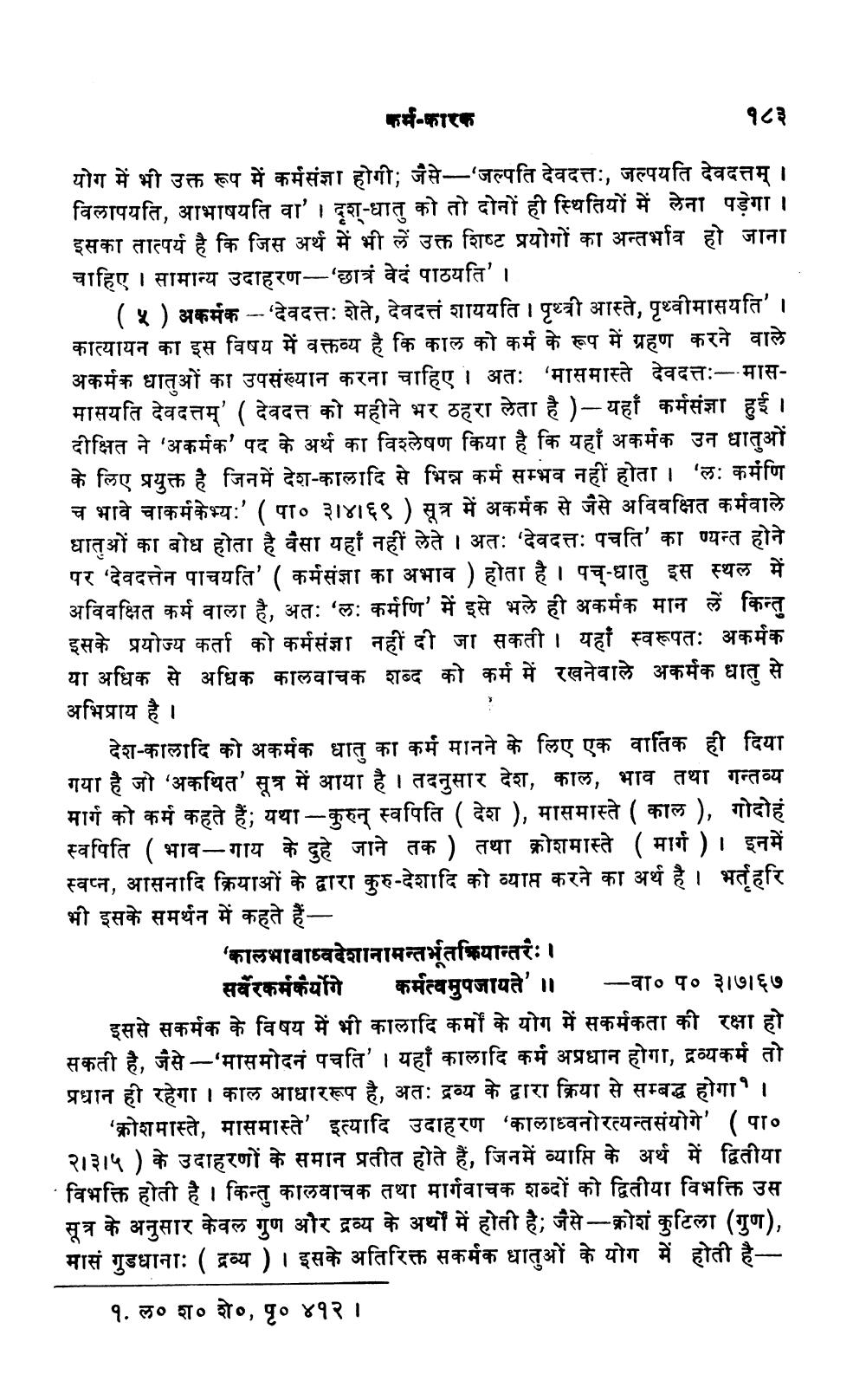________________
कर्म-कारक
१८३
योग में भी उक्त रूप में कर्मसंज्ञा होगी; जैसे-'जल्पति देवदत्तः, जल्पयति देवदत्तम् । विलापयति, आभाषयति वा । दृश्-धातु को तो दोनों ही स्थितियों में लेना पड़ेगा। इसका तात्पर्य है कि जिस अर्थ में भी लें उक्त शिष्ट प्रयोगों का अन्तर्भाव हो जाना चाहिए । सामान्य उदाहरण-'छात्रं वेदं पाठयति' ।
(५) अकर्मक -- 'देवदत्तः शेते, देवदत्तं शाययति । पृथ्वी आस्ते, पृथ्वीमासयति' । कात्यायन का इस विषय में वक्तव्य है कि काल को कर्म के रूप में ग्रहण करने वाले अकर्मक धातुओं का उपसंख्यान करना चाहिए। अतः 'मासमास्ते देवदत्त:--मासमासयति देवदत्तम्' ( देवदत्त को महीने भर ठहरा लेता है )- यहाँ कर्मसंज्ञा हुई। दीक्षित ने 'अकर्मक' पद के अर्थ का विश्लेषण किया है कि यहाँ अकर्मक उन धातुओं के लिए प्रयुक्त है जिनमें देश-कालादि से भिन्न कर्म सम्भव नहीं होता। 'लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः' ( पा० ३।४।६९ ) सूत्र में अकर्मक से जैसे अविवक्षित कर्मवाले धातुओं का बोध होता है वैसा यहाँ नहीं लेते । अत: 'देवदत्तः पचति' का ण्यन्त होने पर 'देवदत्तेन पाचयति' ( कर्मसंज्ञा का अभाव ) होता है। पच्-धातु इस स्थल में अविवक्षित कर्म वाला है, अतः 'लः कर्मणि' में इसे भले ही अकर्मक मान लें किन्तु इसके प्रयोज्य कर्ता को कर्मसंज्ञा नहीं दी जा सकती। यहां स्वरूपतः अकर्मक या अधिक से अधिक कालवाचक शब्द को कर्म में रखनेवाले अकर्मक धातु से अभिप्राय है।
देश-कालादि को अकर्मक धातु का कर्म मानने के लिए एक वार्तिक ही दिया गया है जो 'अकथित' सूत्र में आया है । तदनुसार देश, काल, भाव तथा गन्तव्य मार्ग को कर्म कहते हैं; यथा-कुरुन् स्वपिति ( देश ), मासमास्ते ( काल ), गोदोहं स्वपिति ( भाव-गाय के दुहे जाने तक ) तथा क्रोशमास्ते ( मार्ग)। इनमें स्वप्न, आसनादि क्रियाओं के द्वारा कुरु-देशादि को व्याप्त करने का अर्थ है। भर्तृहरि भी इसके समर्थन में कहते हैं
'कालभावाध्वदेशानामन्तर्भूतक्रियान्तरः।
सर्वेरकर्मकोंगे कर्मत्वमुपजायते' ॥ -वा०प० ३१७१६७ __ इससे सकर्मक के विषय में भी कालादि कर्मों के योग में सकर्मकता की रक्षा हो सकती है, जैसे-'मासमोदनं पचति' । यहाँ कालादि कर्म अप्रधान होगा, द्रव्यकर्म तो प्रधान ही रहेगा। काल आधाररूप है, अतः द्रव्य के द्वारा क्रिया से सम्बद्ध होगा।
'क्रोशमास्ते, मासमास्ते' इत्यादि उदाहरण 'कालाध्वनोरत्यन्तसंयोगे' (पा० २।३।५ ) के उदाहरणों के समान प्रतीत होते हैं, जिनमें व्याप्ति के अर्थ में द्वितीया विभक्ति होती है । किन्तु कालवाचक तथा मार्गवाचक शब्दों को द्वितीया विभक्ति उस सूत्र के अनुसार केवल गुण और द्रव्य के अर्थों में होती है; जैसे-क्रोशं कुटिला (गुण), मासं गुडधानाः (द्रव्य ) । इसके अतिरिक्त सकर्मक धातुओं के योग में होती है
१. ल० श० शे०, पृ० ४१२ ।