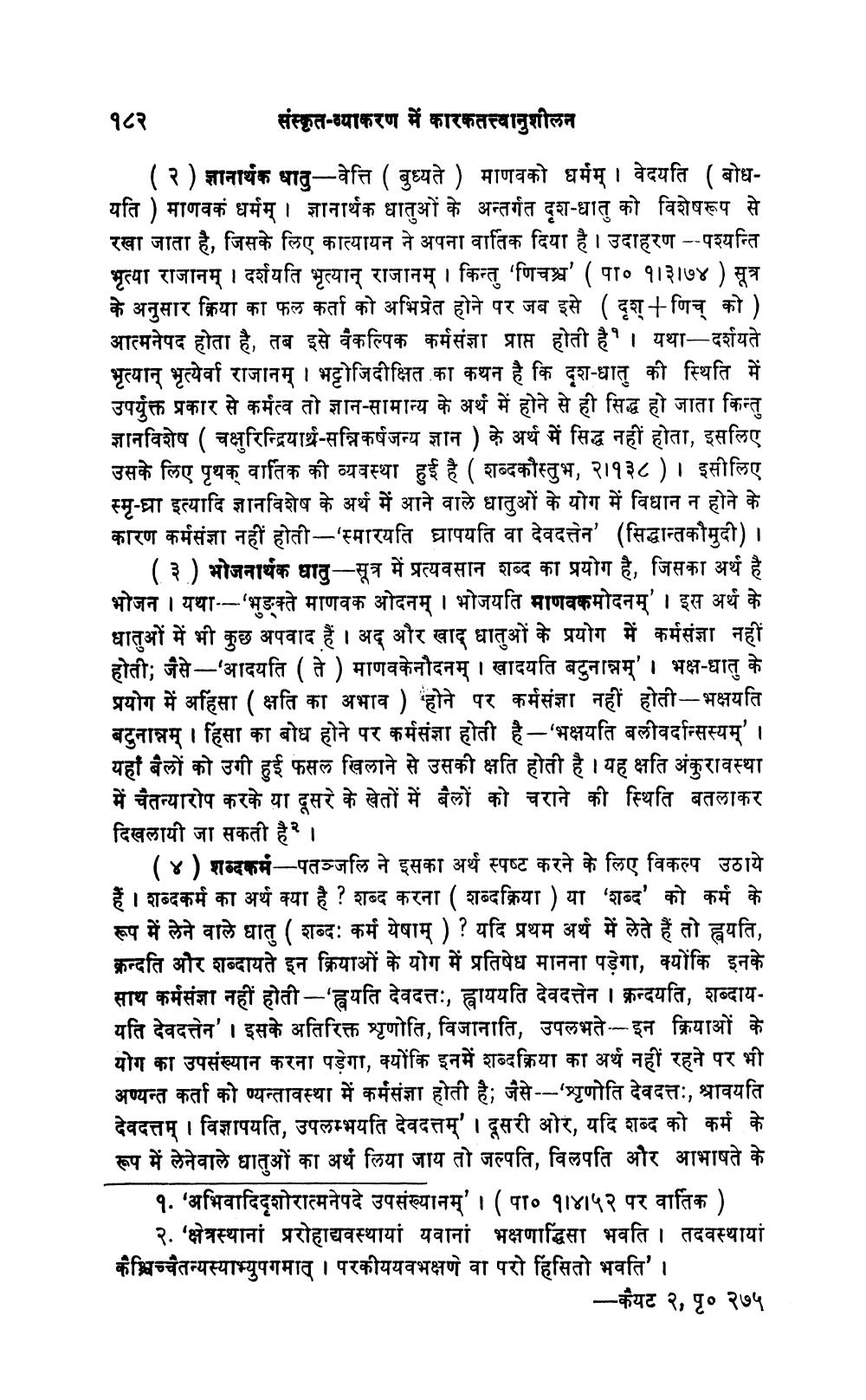________________
संस्कृत-व्याकरण में कारकतत्त्वानुशीलन
(२) ज्ञानार्थक धातु - वेत्ति ( बुध्यते ) माणवको धर्मम् । वेदयति ( बोधयति ) माणवकं धर्मम् । ज्ञानार्थक धातुओं के अन्तर्गत दृश-धातु को विशेषरूप से रखा जाता है, जिसके लिए कात्यायन ने अपना वार्तिक दिया है । उदाहरण - पश्यन्ति भृत्या राजानम् । दर्शयति भृत्यान् राजानम् । किन्तु ' णिचश्व' ( पा० १।३।७४ ) सूत्र के अनुसार क्रिया का फल कर्ता को अभिप्रेत होने पर जब इसे ( दृश् + णिच् को ) आत्मनेपद होता है, तब इसे वैकल्पिक कर्मसंज्ञा प्राप्त होती है' । यथा— दर्शयते भृत्यान् भृत्येर्वा राजानम् । भट्टोजिदीक्षित का कथन है कि दृश-धातु की स्थिति में उपर्युक्त प्रकार से कर्मत्व तो ज्ञान- सामान्य के अर्थ में होने से ही सिद्ध हो जाता किन्तु ज्ञानविशेष ( चक्षुरिन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्य ज्ञान ) के अर्थ में सिद्ध नहीं होता, इसलिए उसके लिए पृथक् वार्तिक की व्यवस्था हुई है ( शब्दकौस्तुभ २।१३८ ) । इसीलिए स्मृघ्रा इत्यादि ज्ञानविशेष के अर्थ में आने वाले धातुओं के योग में विधान न होने के कारण कर्मसंज्ञा नहीं होती - ' स्मारयति घ्रापयति वा देवदत्तेन' (सिद्धान्तकौमुदी ) ।
( ३ ) भोजनार्थक धातु — सूत्र में प्रत्यवसान शब्द का प्रयोग है, जिसका अर्थ है भोजन । यथा--' - 'भुङ्क्ते माणवक ओदनम् । भोजयति माणवकमोदनम् ' । इस अर्थ के धातुओं में भी कुछ अपवाद हैं । अद् और खाद् धातुओं के प्रयोग में कर्मसंज्ञा नहीं होती; जैसे – 'आदयति ( ते ) माणवकेनौदनम् । खादयति बटुनान्नम् ' । भक्ष-धातु के प्रयोग में अहिंसा ( क्षति का अभाव ) होने पर कर्मसंज्ञा नहीं होती - भक्षयति बनान्नम् । हिंसा का बोध होने पर कर्मसंज्ञा होती है - ' भक्षयति बलीवर्दान्सस्यम्' । यहाँ बैलों को उगी हुई फसल खिलाने से उसकी क्षति होती है । यह क्षति अंकुरावस्था में चैतन्यारोप करके या दूसरे के खेतों में बैलों को चराने की स्थिति बतलाकर दिखलायी जा सकती है ।
१८२
( ४ ) शब्दकर्म - पतञ्जलि ने इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए विकल्प उठाये हैं । शब्दकर्म का अर्थ क्या है ? शब्द करना ( शब्द क्रिया ) या 'शब्द' को कर्म के रूप में लेने वाले धातु ( शब्द: कर्म येषाम् ) ? यदि प्रथम अर्थ में लेते हैं तो ह्वयति, क्रन्दति और शब्दायते इन क्रियाओं के योग में प्रतिषेध मानना पड़ेगा, क्योंकि इनके साथ कर्मसंज्ञा नहीं होती – 'ह्वयति देवदत्तः, ह्वाययति देवदत्तेन । क्रन्दयति, शब्दाययति देवदत्तेन' । इसके अतिरिक्त शृणोति, विजानाति, उपलभते - इन क्रियाओं के योग का उपसंख्यान करना पड़ेगा, क्योंकि इनमें शब्दक्रिया का अर्थ नहीं रहने पर भी अण्यन्त कर्ता को ण्यन्तावस्था में कर्मसंज्ञा होती है; जैसे--' शृणोति देवदत्तः, श्रावयति देवदत्तम् । विज्ञापयति, उपलम्भयति देवदत्तम्' । दूसरी ओर, यदि शब्द को कर्म के रूप में लेनेवाले धातुओं का अर्थं लिया जाय तो जल्पति, विलपति और आभाषते के
१. 'अभिवादिदृशोरात्मनेपदे उपसंख्यानम्' । ( पा० १|४|५२ पर वार्तिक ) २. 'क्षेत्रस्थानां प्ररोहाद्यवस्थायां यवानां भक्षणाद्धिसा भवति । तदवस्थायां कैश्विचैतन्यस्याभ्युपगमात् । परकीययवभक्षणे वा परो हिंसितो भवति' ।
— कैयट २, पृ० २७५