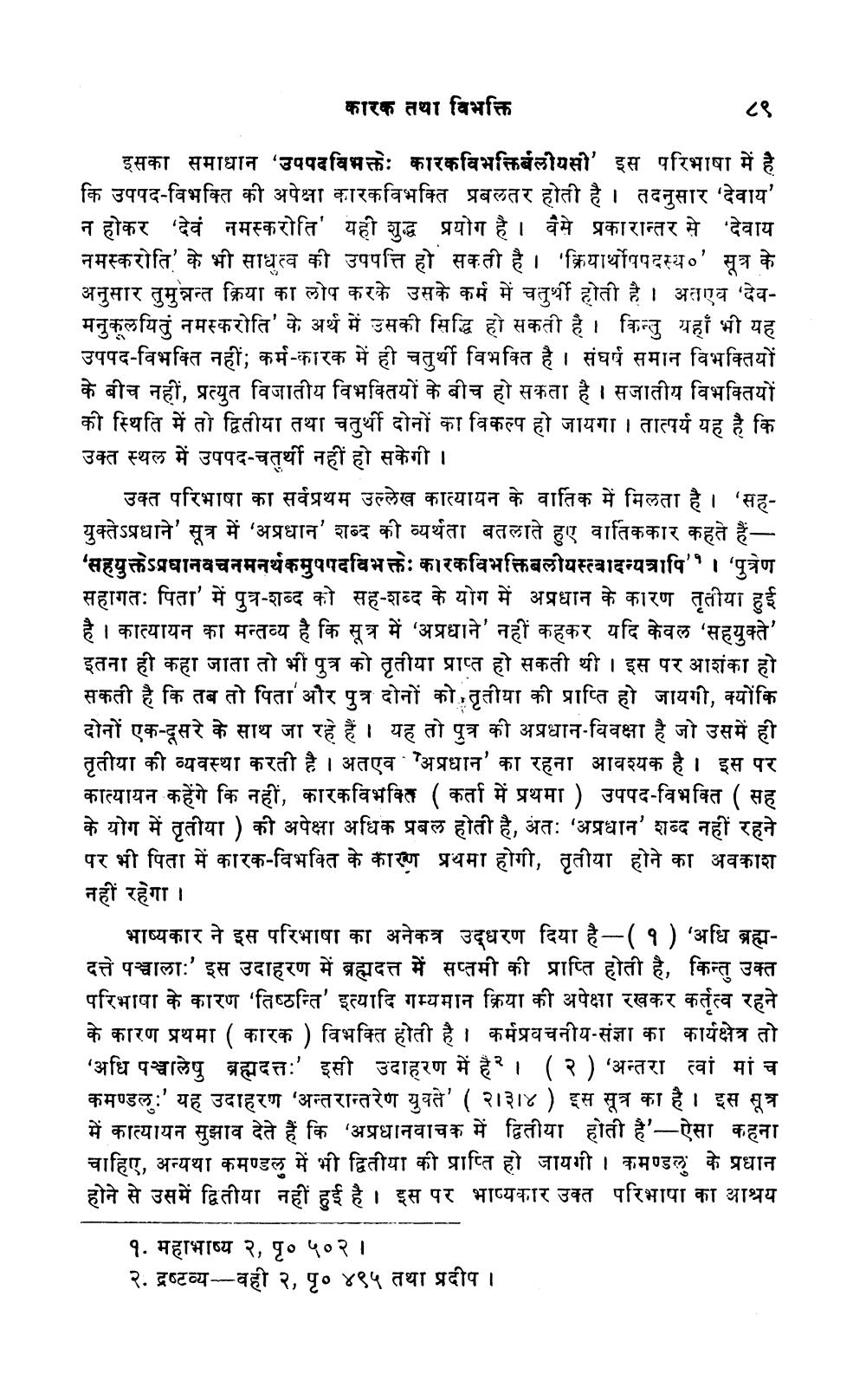________________
कारक तथा विभक्ति
८९
इसका समाधान 'उपपदविभक्तः कारकविभक्तिबलीयसी' इस परिभाषा में है कि उपपद-विभक्ति की अपेक्षा कारकविभक्ति प्रबलतर होती है। तदनुसार 'देवाय' न होकर 'देवं नमस्करोति' यही शुद्ध प्रयोग है। वैसे प्रकारान्तर से 'देवाय नमस्करोति' के भी साधुत्व की उपपत्ति हो सकती है। 'क्रियार्थोषपदस्थ०' सूत्र के अनुसार तुमुन्नन्त क्रिया का लोप करके उसके कर्म में चतुर्थी होती है। अतएव 'देवमनुकूलयितुं नमस्करोति' के अर्थ में उसकी सिद्धि हो सकती है। किन्तु यहाँ भी यह उपपद-विभक्ति नहीं; कर्म-कारक में ही चतुर्थी विभक्ति है । संघर्ष समान विभक्तियों के बीच नहीं, प्रत्युत विजातीय विभक्तियों के बीच हो सकता है । सजातीय विभक्तियों की स्थिति में तो द्वितीया तथा चतुर्थी दोनों का विकल्प हो जायगा । तात्पर्य यह है कि उक्त स्थल में उपपद-चतुर्थी नहीं हो सकेगी।
उक्त परिभाषा का सर्वप्रथम उल्लेख कात्यायन के वार्तिक में मिलता है। 'सहयुक्तेऽप्रधाने' सूत्र में 'अप्रधान' शब्द की व्यर्थता बतलाते हुए वार्तिककार कहते हैं'सहयुक्तेऽप्रधानवचनमनर्थकमुषपदविभक्तेः कारकविभक्तिबलीयस्त्वादन्यत्रापि''। 'पुत्रेण सहागतः पिता' में पुत्र-शब्द को सह-शब्द के योग में अप्रधान के कारण तृतीया हुई है। कात्यायन का मन्तव्य है कि सूत्र में 'अप्रधाने' नहीं कहकर यदि केवल ‘सहयुक्ते' इतना ही कहा जाता तो भी पुत्र को तृतीया प्राप्त हो सकती थी। इस पर आशंका हो सकती है कि तब तो पिता और पुत्र दोनों को तृतीया की प्राप्ति हो जायगी, क्योंकि दोनों एक-दूसरे के साथ जा रहे हैं। यह तो पुत्र की अप्रधान-विवक्षा है जो उसमें ही तृतीया की व्यवस्था करती है । अतएव 'अप्रधान' का रहना आवश्यक है। इस पर कात्यायन कहेंगे कि नहीं, कारकविभक्ति ( कर्ता में प्रथमा) उपपद-विभक्ति ( सह के योग में तृतीया ) की अपेक्षा अधिक प्रबल होती है, अंत: 'अप्रधान' शब्द नहीं रहने पर भी पिता में कारक-विभक्ति के कारण प्रथमा होगी, तृतीया होने का अवकाश नहीं रहेगा।
भाष्यकार ने इस परिभाषा का अनेकत्र उद्धरण दिया है-(१) 'अधि ब्रह्मदत्ते पञ्चालाः' इस उदाहरण में ब्रह्मदत्त में सप्तमी की प्राप्ति होती है, किन्तु उक्त परिभाषा के कारण तिष्ठन्ति' इत्यादि गम्यमान क्रिया की अपेक्षा रखकर कर्तत्व रहने के कारण प्रथमा ( कारक ) विभक्ति होती है। कर्मप्रवचनीय-संज्ञा का कार्यक्षेत्र तो 'अधि पञ्चालेषु ब्रह्मदत्तः' इसी उदाहरण में है। (२) 'अन्तरा त्वां मां च कमण्डलुः' यह उदाहरण 'अन्तरान्तरेण युक्ते' ( २।३।४) इस सूत्र का है। इस सूत्र में कात्यायन सुझाव देते हैं कि 'अप्रधानवाचक में द्वितीया होती है'-ऐसा कहना चाहिए, अन्यथा कमण्डल में भी द्वितीया की प्राप्ति हो जायगी। कमण्डलु के प्रधान होने से उसमें द्वितीया नहीं हुई है। इस पर भाष्यकार उक्त परिभाषा का आश्रय
१. महाभाष्य २, पृ० ५०२ । २. द्रष्टव्य--वही २, पृ० ४९५ तथा प्रदीप ।