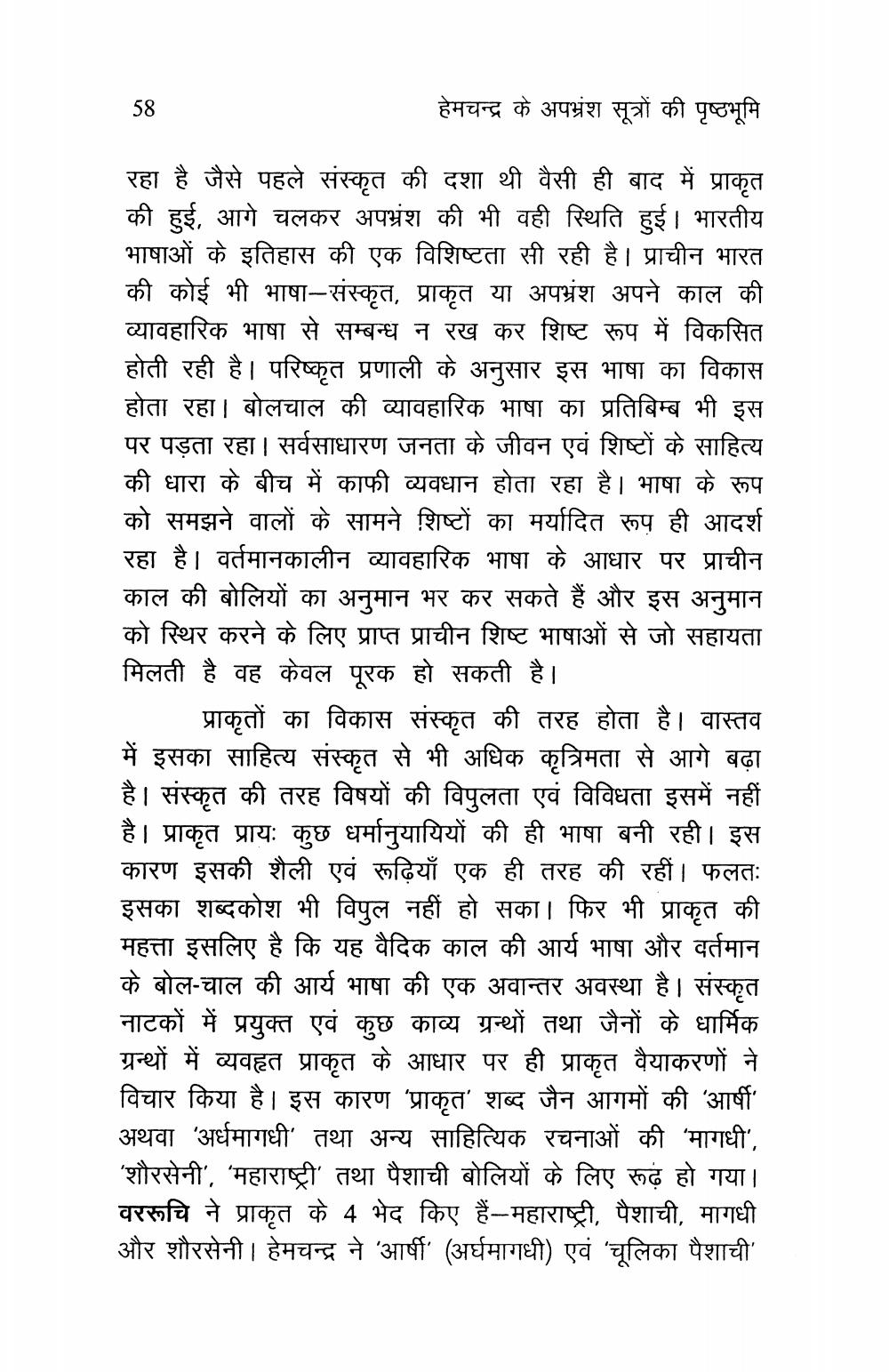________________
हेमचन्द्र के अपभ्रंश सूत्रों की पृष्ठभूमि
रहा है जैसे पहले संस्कृत की दशा थी वैसी ही बाद में प्राकृत की हुई, आगे चलकर अपभ्रंश की भी वही स्थिति हुई । भारतीय भाषाओं के इतिहास की एक विशिष्टता सी रही है । प्राचीन भारत की कोई भी भाषा - संस्कृत, प्राकृत या अपभ्रंश अपने काल की व्यावहारिक भाषा से सम्बन्ध न रख कर शिष्ट रूप में विकसित होती रही है। परिष्कृत प्रणाली के अनुसार इस भाषा का विकास होता रहा । बोलचाल की व्यावहारिक भाषा का प्रतिबिम्ब भी इस पर पड़ता रहा। सर्वसाधारण जनता के जीवन एवं शिष्टों के साहित्य की धारा के बीच में काफी व्यवधान होता रहा है। भाषा के रूप को समझने वालों के सामने शिष्टों का मर्यादित रूप ही आदर्श रहा है। वर्तमानकालीन व्यावहारिक भाषा के आधार पर प्राचीन काल की बोलियों का अनुमान भर कर सकते हैं और इस अनुमान को स्थिर करने के लिए प्राप्त प्राचीन शिष्ट भाषाओं से जो सहायता मिलती है वह केवल पूरक हो सकती है ।
58
प्राकृतों का विकास संस्कृत की तरह होता है । वास्तव में इसका साहित्य संस्कृत से भी अधिक कृत्रिमता से आगे बढ़ा है । संस्कृत की तरह विषयों की विपुलता एवं विविधता इसमें नहीं है। प्राकृत प्रायः कुछ धर्मानुयायियों की ही भाषा बनी रही। इस कारण इसकी शैली एवं रूढ़ियाँ एक ही तरह की रहीं । फलतः इसका शब्दकोश भी विपुल नहीं हो सका। फिर भी प्राकृत की महत्ता इसलिए है कि यह वैदिक काल की आर्य भाषा और वर्तमान के बोल-चाल की आर्य भाषा की एक अवान्तर अवस्था है। संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त एवं कुछ काव्य ग्रन्थों तथा जैनों के धार्मिक ग्रन्थों में व्यवहृत प्राकृत के आधार पर ही प्राकृत वैयाकरणों ने विचार किया है। इस कारण 'प्राकृत' शब्द जैन आगमों की 'आर्षी' अथवा 'अर्धमागधी' तथा अन्य साहित्यिक रचनाओं की 'मागधी', 'शौरसेनी', 'महाराष्ट्री' तथा पैशाची बोलियों के लिए रूढ़ हो गया । वररुचि ने प्राकृत के 4 भेद किए हैं- महाराष्ट्री, पैशाची, मागधी और शौरसेनी । हेमचन्द्र ने 'आर्षी' (अर्धमागधी) एवं 'चूलिका पैशाची'