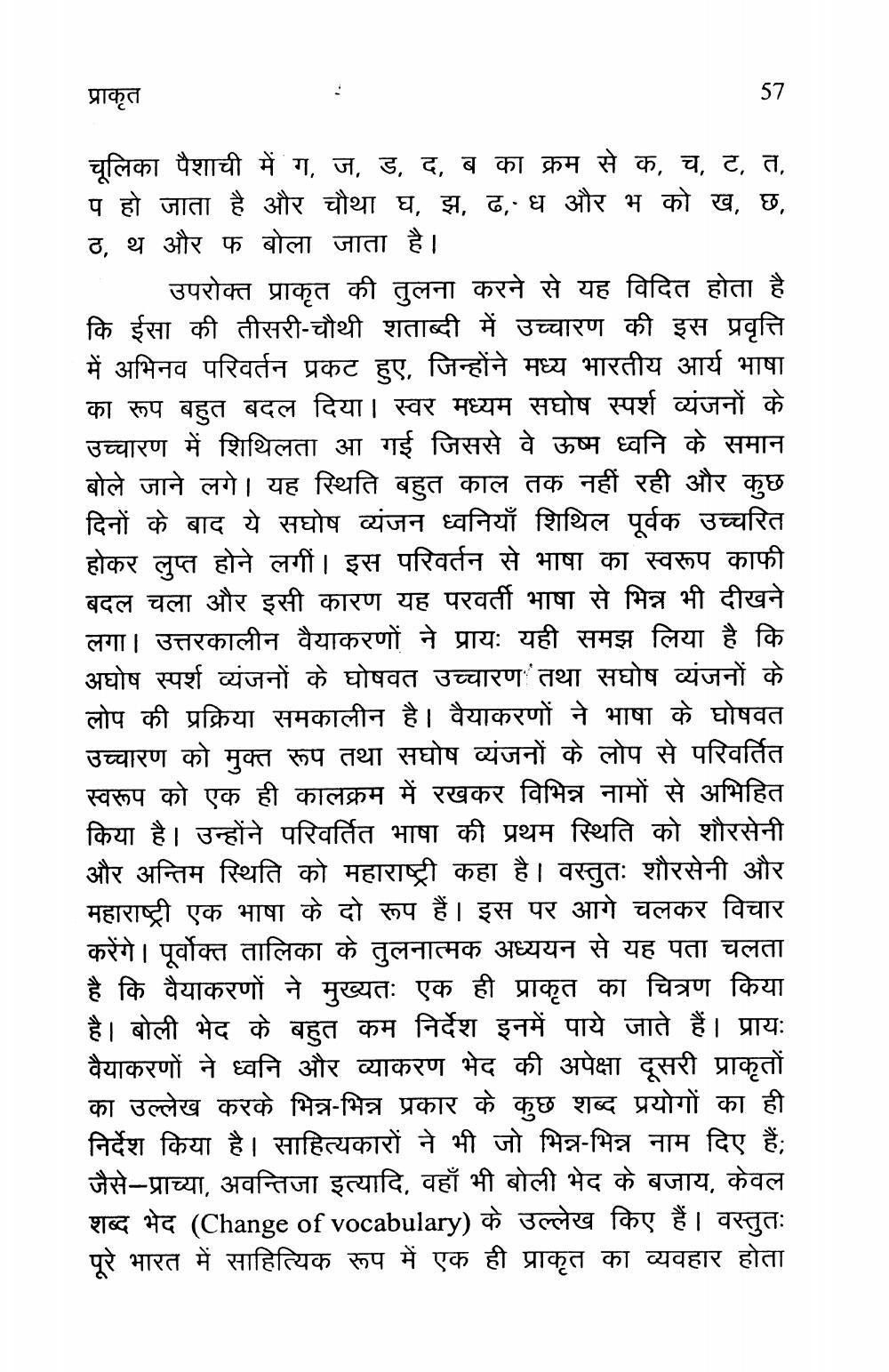________________
प्राकृत
57
चूलिका पैशाची में ग, ज, ड, द, ब का क्रम से क, च, ट, त, प हो जाता है और चौथा घ, झ, ढ, ध और भ को ख, छ, ठ, थ और फ बोला जाता है।
उपरोक्त प्राकृत की तुलना करने से यह विदित होता है कि ईसा की तीसरी-चौथी शताब्दी में उच्चारण की इस प्रवृत्ति में अभिनव परिवर्तन प्रकट हुए, जिन्होंने मध्य भारतीय आर्य भाषा का रूप बहुत बदल दिया। स्वर मध्यम सघोष स्पर्श व्यंजनों के उच्चारण में शिथिलता आ गई जिससे वे ऊष्म ध्वनि के समान बोले जाने लगे। यह स्थिति बहुत काल तक नहीं रही और कुछ दिनों के बाद ये सघोष व्यंजन ध्वनियाँ शिथिल पूर्वक उच्चरित होकर लुप्त होने लगीं। इस परिवर्तन से भाषा का स्वरूप काफी बदल चला और इसी कारण यह परवर्ती भाषा से भिन्न भी दीखने लगा। उत्तरकालीन वैयाकरणों ने प्रायः यही समझ लिया है कि अघोष स्पर्श व्यंजनों के घोषवत उच्चारण तथा सघोष व्यंजनों के लोप की प्रक्रिया समकालीन है। वैयाकरणों ने भाषा के घोषवत उच्चारण को मुक्त रूप तथा सघोष व्यंजनों के लोप से परिवर्तित स्वरूप को एक ही कालक्रम में रखकर विभिन्न नामों से अभिहित किया है। उन्होंने परिवर्तित भाषा की प्रथम स्थिति को शौरसेनी
और अन्तिम स्थिति को महाराष्ट्री कहा है। वस्तुतः शौरसेनी और महाराष्ट्री एक भाषा के दो रूप हैं। इस पर आगे चलकर विचार करेंगे। पूर्वोक्त तालिका के तुलनात्मक अध्ययन से यह पता चलता है कि वैयाकरणों ने मुख्यतः एक ही प्राकृत का चित्रण किया है। बोली भेद के बहुत कम निर्देश इनमें पाये जाते हैं। प्रायः वैयाकरणों ने ध्वनि और व्याकरण भेद की अपेक्षा दूसरी प्राकृतों का उल्लेख करके भिन्न-भिन्न प्रकार के कुछ शब्द प्रयोगों का ही निर्देश किया है। साहित्यकारों ने भी जो भिन्न-भिन्न नाम दिए हैं; जैसे-प्राच्या, अवन्तिजा इत्यादि, वहाँ भी बोली भेद के बजाय, केवल शब्द भेद (Change of vocabulary) के उल्लेख किए हैं। वस्तुतः पूरे भारत में साहित्यिक रूप में एक ही प्राकृत का व्यवहार होता