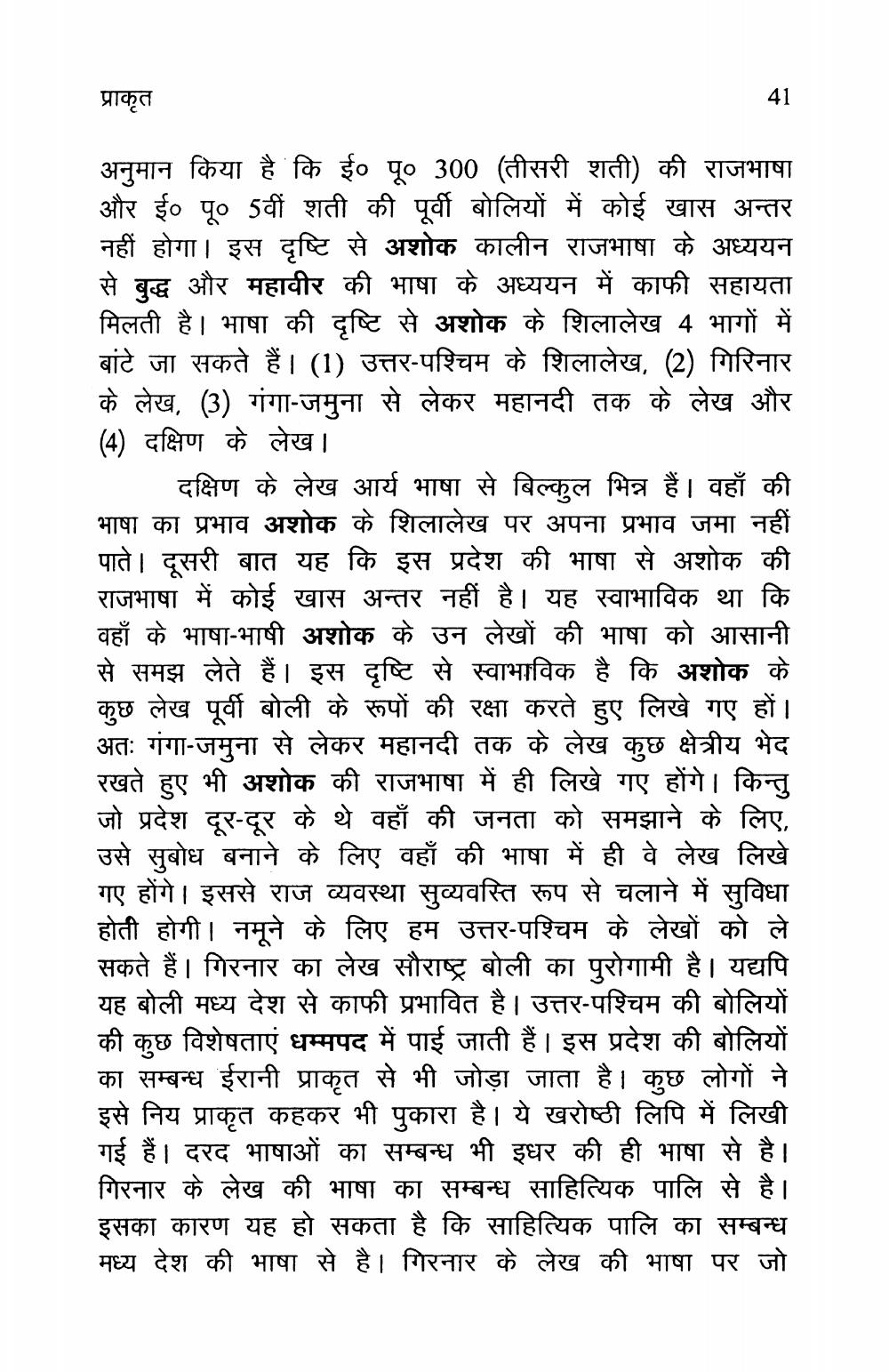________________
प्राकृत
41
अनुमान किया है कि ई० पू० 300 (तीसरी शती) की राजभाषा और ई० पू० 5वीं शती की पूर्वी बोलियों में कोई खास अन्तर नहीं होगा। इस दृष्टि से अशोक कालीन राजभाषा के अध्ययन से बुद्ध और महावीर की भाषा के अध्ययन में काफी सहायता मिलती है। भाषा की दृष्टि से अशोक के शिलालेख 4 भागों में बांटे जा सकते हैं। (1) उत्तर-पश्चिम के शिलालेख, (2) गिरिनार के लेख, (3) गंगा-जमुना से लेकर महानदी तक के लेख और (4) दक्षिण के लेख।
दक्षिण के लेख आर्य भाषा से बिल्कुल भिन्न हैं। वहाँ की भाषा का प्रभाव अशोक के शिलालेख पर अपना प्रभाव जमा नहीं पाते। दूसरी बात यह कि इस प्रदेश की भाषा से अशोक की राजभाषा में कोई खास अन्तर नहीं है। यह स्वाभाविक था कि वहाँ के भाषा-भाषी अशोक के उन लेखों की भाषा को आसानी से समझ लेते हैं। इस दृष्टि से स्वाभाविक है कि अशोक के कुछ लेख पूर्वी बोली के रूपों की रक्षा करते हुए लिखे गए हों। अतः गंगा-जमुना से लेकर महानदी तक के लेख कुछ क्षेत्रीय भेद रखते हुए भी अशोक की राजभाषा में ही लिखे गए होंगे। किन्तु जो प्रदेश दूर-दूर के थे वहाँ की जनता को समझाने के लिए, उसे सुबोध बनाने के लिए वहाँ की भाषा में ही वे लेख लिखे गए होंगे। इससे राज व्यवस्था सुव्यवस्ति रूप से चलाने में सुविधा होती होगी। नमूने के लिए हम उत्तर-पश्चिम के लेखों को ले सकते हैं। गिरनार का लेख सौराष्ट्र बोली का पुरोगामी है। यद्यपि यह बोली मध्य देश से काफी प्रभावित है। उत्तर-पश्चिम की बोलियों की कुछ विशेषताएं धम्मपद में पाई जाती हैं। इस प्रदेश की बोलियों का सम्बन्ध ईरानी प्राकृत से भी जोड़ा जाता है। कुछ लोगों ने इसे निय प्राकृत कहकर भी पुकारा है। ये खरोष्ठी लिपि में लिखी गई हैं। दरद भाषाओं का सम्बन्ध भी इधर की ही भाषा से है। गिरनार के लेख की भाषा का सम्बन्ध साहित्यिक पालि से है। इसका कारण यह हो सकता है कि साहित्यिक पालि का सम्बन्ध मध्य देश की भाषा से है। गिरनार के लेख की भाषा पर जो