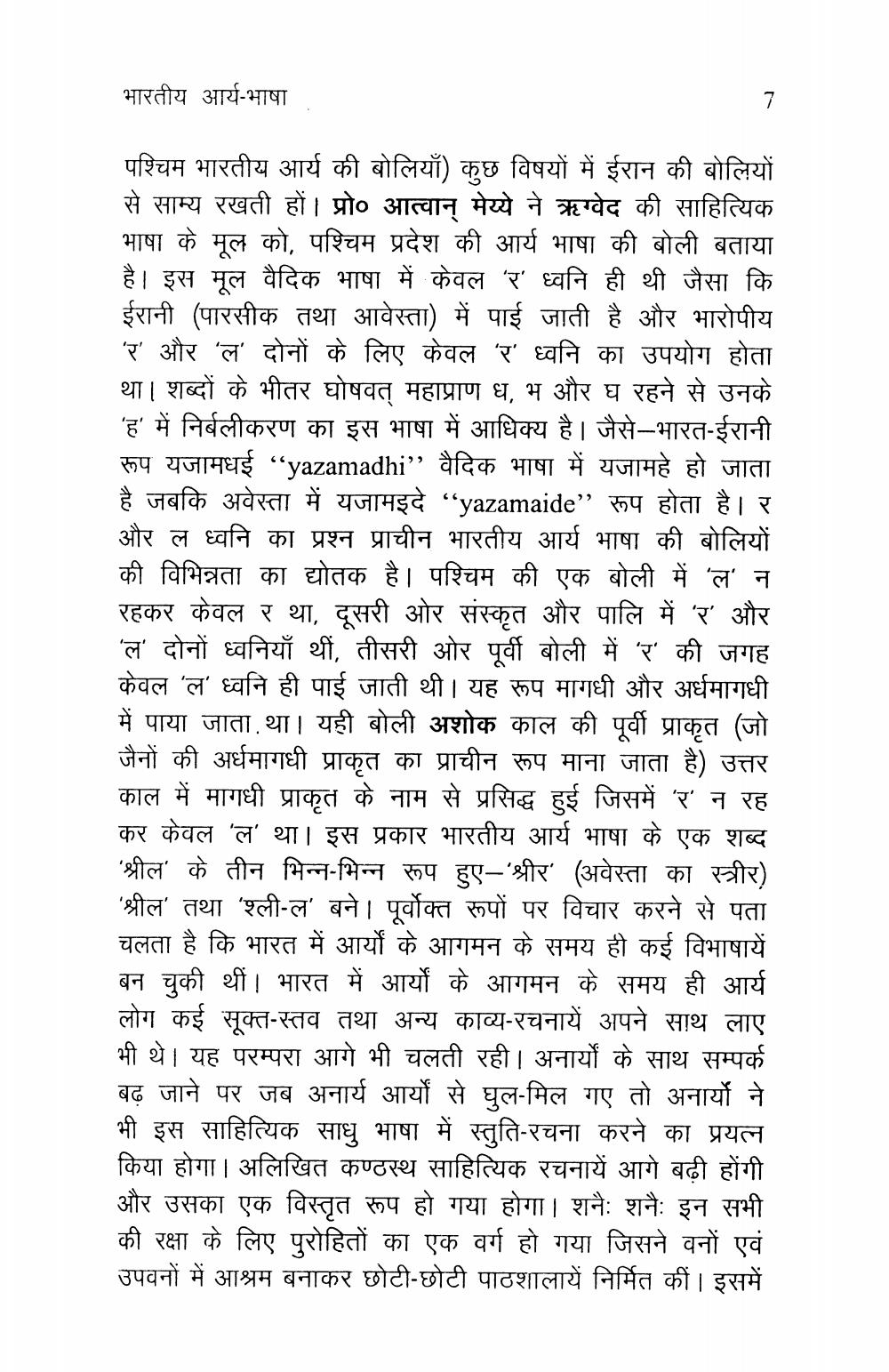________________
भारतीय आर्य-भाषा
पश्चिम भारतीय आर्य की बोलियाँ) कुछ विषयों में ईरान की बोलियों से साम्य रखती हों। प्रो० आत्वान् मेय्ये ने ऋग्वेद की साहित्यिक भाषा के मूल को, पश्चिम प्रदेश की आर्य भाषा की बोली बताया है । इस मूल वैदिक भाषा में केवल 'र' ध्वनि ही थी जैसा कि ईरानी ( पारसीक तथा आवेस्ता) में पाई जाती है और भारोपीय 'र' और 'ल' दोनों के लिए केवल 'र' ध्वनि का उपयोग होता था । शब्दों के भीतर घोषवत् महाप्राण ध, भ और घ रहने से उनके 'ह' में निर्बलीकरण का इस भाषा में आधिक्य है । जैसे - भारत-ईरानी रूप यजामधई “ yazamadhi" वैदिक भाषा में यजामहे हो जाता है जबकि अवेस्ता में यजामइदे “ yazamaide " रूप होता है। र और ल ध्वनि का प्रश्न प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की बोलियों की विभिन्नता का द्योतक है। पश्चिम की एक बोली में 'ल' न रहकर केवल र था, दूसरी ओर संस्कृत और पालि में 'र' और 'ल' दोनों ध्वनियाँ थीं, तीसरी ओर पूर्वी बोली में 'र' की जगह केवल 'ल' ध्वनि ही पाई जाती थी । यह रूप मागधी और अर्धमागधी में पाया जाता था । यही बोली अशोक काल की पूर्वी प्राकृत (जो जैनों की अर्धमागधी प्राकृत का प्राचीन रूप माना जाता है) उत्तर काल में मागधी प्राकृत के नाम से प्रसिद्ध हुई जिसमें 'र' न रह कर केवल 'ल' था । इस प्रकार भारतीय आर्य भाषा के एक शब्द 'श्रील' के तीन भिन्न-भिन्न रूप हुए- 'श्रीर' (अवेस्ता का स्त्रीर) 'श्रील' तथा 'श्ली-ल' बने । पूर्वोक्त रूपों पर विचार करने से पता चलता है कि भारत में आर्यों के आगमन के समय ही कई विभाषायें बन चुकी थीं। भारत में आर्यों के आगमन के समय ही आर्य लोग कई सूक्त - स्तव तथा अन्य काव्य रचनायें अपने साथ लाए भी थे । यह परम्परा आगे भी चलती रही। अनार्यों के साथ सम्पर्क बढ़ जाने पर जब अनार्य आर्यों से घुल-मिल गए तो अनार्यो ने भी इस साहित्यिक साधु भाषा में स्तुति- रचना करने का प्रयत्न किया होगा । अलिखित कण्ठस्थ साहित्यिक रचनायें आगे बढ़ी होंगी और उसका एक विस्तृत रूप हो गया होगा । शनैः शनैः इन सभी की रक्षा के लिए पुरोहितों का एक वर्ग हो गया जिसने वनों एवं उपवनों में आश्रम बनाकर छोटी-छोटी पाठशालायें निर्मित कीं। इसमें
I
7