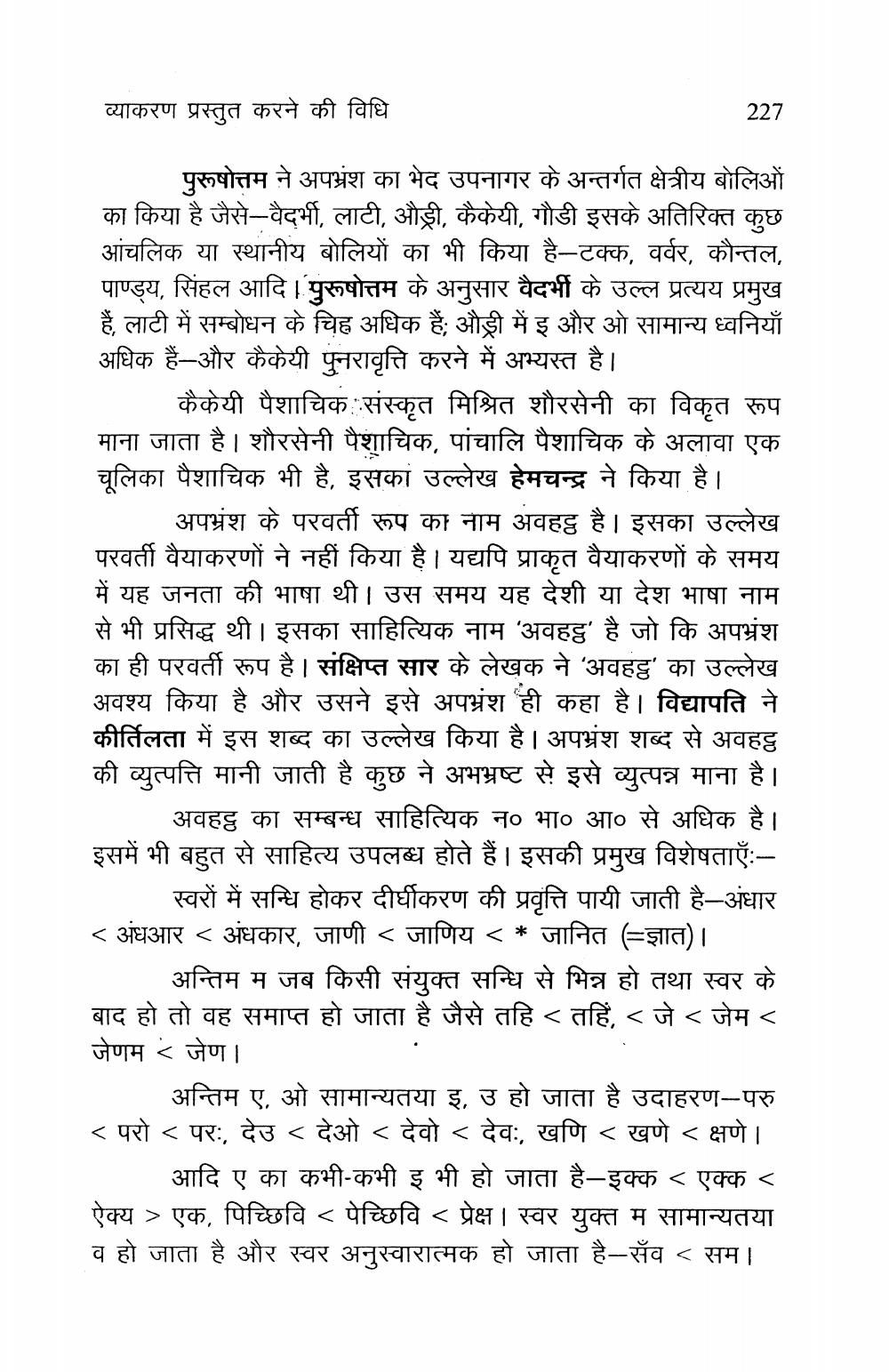________________
व्याकरण प्रस्तुत करने की विधि
227
पुरूषोत्तम ने अपभ्रंश का भेद उपनागर के अन्तर्गत क्षेत्रीय बोलिओं का किया है जैसे-वैदर्भी, लाटी, औड्री, कैकेयी, गौडी इसके अतिरिक्त कुछ आंचलिक या स्थानीय बोलियों का भी किया है-टक्क, वर्वर, कौन्तल, पाण्ड्य, सिंहल आदि । पुरूषोत्तम के अनुसार वैदर्भी के उल्ल प्रत्यय प्रमुख हैं, लाटी में सम्बोधन के चिह्न अधिक हैं; औड्री में इ और ओ सामान्य ध्वनियाँ अधिक हैं और कैकेयी पुनरावृत्ति करने में अभ्यस्त है।
कैकेयी पैशाचिक संस्कृत मिश्रित शौरसेनी का विकृत रूप माना जाता है। शौरसेनी पैशाचिक, पांचालि पैशाचिक के अलावा एक चूलिका पैशाचिक भी है, इसका उल्लेख हेमचन्द्र ने किया है।
___ अपभ्रंश के परवर्ती रूप का नाम अवहट्ट है। इसका उल्लेख परवर्ती वैयाकरणों ने नहीं किया है। यद्यपि प्राकृत वैयाकरणों के समय में यह जनता की भाषा थी। उस समय यह देशी या देश भाषा नाम से भी प्रसिद्ध थी। इसका साहित्यिक नाम 'अवहट्ट' है जो कि अपभ्रंश का ही परवर्ती रूप है। संक्षिप्त सार के लेखक ने 'अवहट्ट' का उल्लेख अवश्य किया है और उसने इसे अपभ्रंश ही कहा है। विद्यापति ने कीर्तिलता में इस शब्द का उल्लेख किया है। अपभ्रंश शब्द से अवहट्ट की व्युत्पत्ति मानी जाती है कुछ ने अभभ्रष्ट से इसे व्युत्पन्न माना है।
अवहट्ट का सम्बन्ध साहित्यिक न० भा० आ० से अधिक है। इसमें भी बहुत से साहित्य उपलब्ध होते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएँ:
स्वरों में सन्धि होकर दीर्धीकरण की प्रवृत्ति पायी जाती है-अंधार < अंधआर < अंधकार, जाणी < जाणिय < * जानित (=ज्ञात)।
___ अन्तिम म जब किसी संयुक्त सन्धि से भिन्न हो तथा स्वर के बाद हो तो वह समाप्त हो जाता है जैसे तहि < तहिं, < जे < जेम < जेणम < जेण।
अन्तिम ए, ओ सामान्यतया इ, उ हो जाता है उदाहरण-परु < परो < परः, देउ < देओ < देवो < देवः, खणि < खणे < क्षणे।
आदि ए का कभी-कभी इ भी हो जाता है-इक्क < एक्क < ऐक्य > एक, पिच्छिवि < पेच्छिवि < प्रेक्ष । स्वर युक्त म सामान्यतया व हो जाता है और स्वर अनुस्वारात्मक हो जाता है-सँव < सम ।