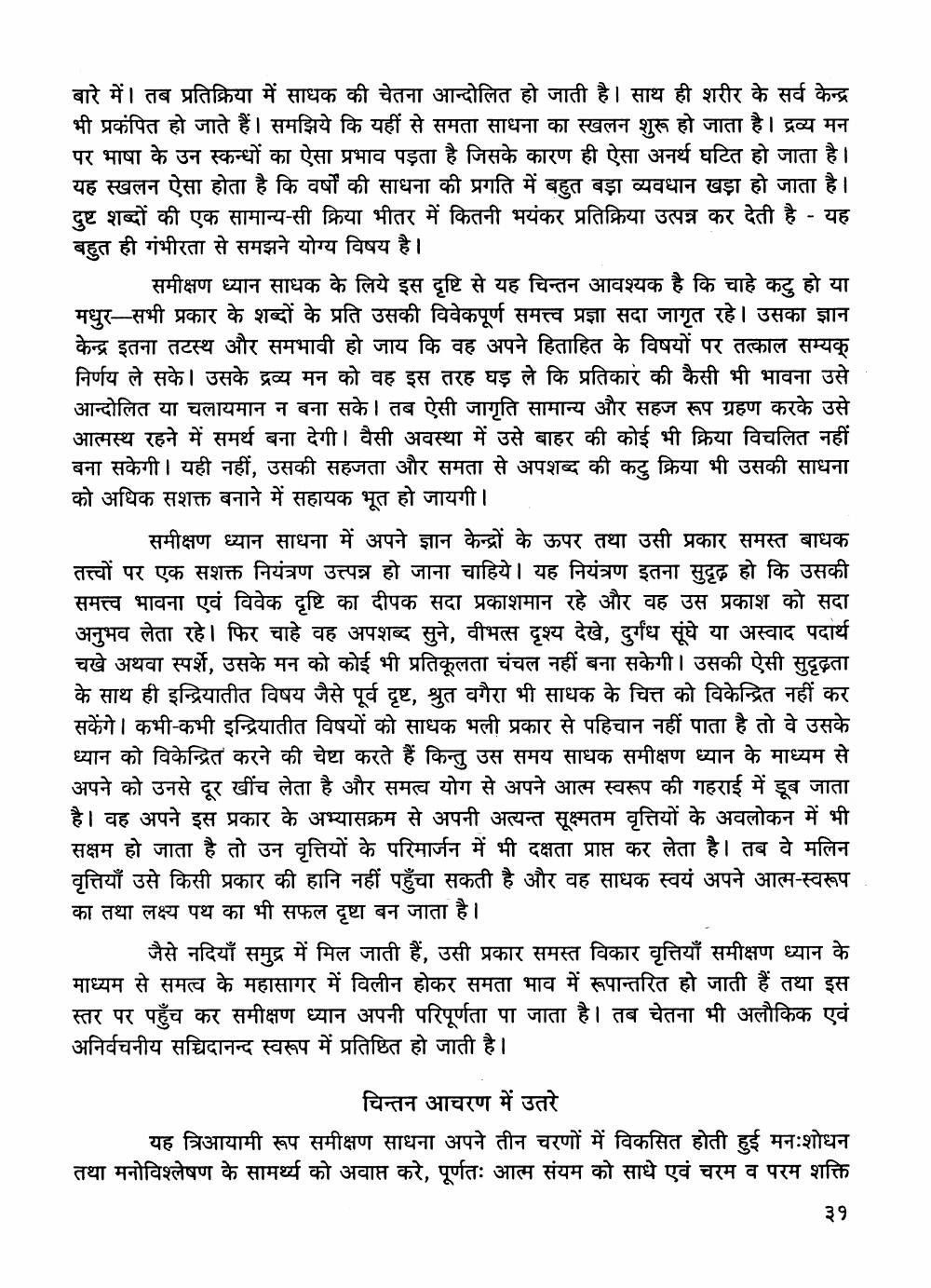________________
बारे में। तब प्रतिक्रिया में साधक की चेतना आन्दोलित हो जाती है। साथ ही शरीर के सर्व केन्द्र भी प्रकंपित हो जाते हैं। समझिये कि यहीं से समता साधना का स्खलन शुरू हो जाता है। द्रव्य मन पर भाषा के उन स्कन्धों का ऐसा प्रभाव पड़ता है जिसके कारण ही ऐसा अनर्थ घटित हो जाता है। यह स्खलन ऐसा होता है कि वर्षों की साधना की प्रगति में बहुत बड़ा व्यवधान खड़ा हो जाता है। दुष्ट शब्दों की एक सामान्य-सी क्रिया भीतर में कितनी भयंकर प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देती है - यह बहुत ही गंभीरता से समझने योग्य विषय है।
समीक्षण ध्यान साधक के लिये इस दृष्टि से यह चिन्तन आवश्यक है कि चाहे कटु हो या मधुर—सभी प्रकार के शब्दों के प्रति उसकी विवेकपूर्ण समत्त्व प्रज्ञा सदा जागृत रहे। उसका ज्ञान केन्द्र इतना तटस्थ और समभावी हो जाय कि वह अपने हिताहित के विषयों पर तत्काल सम्यक् निर्णय ले सके। उसके द्रव्य मन को वह इस तरह घड़ ले कि प्रतिकार की कैसी भी भावना उसे आन्दोलित या चलायमान न बना सके। तब ऐसी जागृति सामान्य और सहज रूप ग्रहण करके उसे आत्मस्थ रहने में समर्थ बना देगी। वैसी अवस्था में उसे बाहर की कोई भी क्रिया विचलित नहीं बना सकेगी। यही नहीं, उसकी सहजता और समता से अपशब्द की कटु क्रिया भी उसकी साधना को अधिक सशक्त बनाने में सहायक भत हो जायगी।
समीक्षण ध्यान साधना में अपने ज्ञान केन्द्रों के ऊपर तथा उसी प्रकार समस्त बाधक तत्त्वों पर एक सशक्त नियंत्रण उत्पन्न हो जाना चाहिये। यह नियंत्रण इतना सुदृढ़ हो कि उसकी समत्त्व भावना एवं विवेक दृष्टि का दीपक सदा प्रकाशमान रहे और वह उस प्रकाश को सदा अनुभव लेता रहे। फिर चाहे वह अपशब्द सुने, वीभत्स दृश्य देखे, दुर्गंध सूंघे या अस्वाद पदार्थ चखे अथवा स्पर्श, उसके मन को कोई भी प्रतिकूलता चंचल नहीं बना सकेगी। उसकी ऐसी सदढ़ता के साथ ही इन्द्रियातीत विषय जैसे पूर्व दृष्ट, श्रुत वगैरा भी साधक के चित्त को विकेन्द्रित नहीं कर सकेंगे। कभी-कभी इन्द्रियातीत विषयों को साधक भली प्रकार से पहिचान नहीं पाता है तो वे उसके ध्यान को विकेन्द्रित करने की चेष्टा करते हैं किन्तु उस समय साधक समीक्षण ध्यान के माध्यम से अपने को उनसे दूर खींच लेता है और समत्व योग से अपने आत्म स्वरूप की गहराई में डूब जाता है। वह अपने इस प्रकार के अभ्यासक्रम से अपनी अत्यन्त सूक्ष्मतम वृत्तियों के अवलोकन में भी सक्षम हो जाता है तो उन वृत्तियों के परिमार्जन में भी दक्षता प्राप्त कर लेता है। तब वे मलिन वृत्तियाँ उसे किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचा सकती है और वह साधक स्वयं अपने आत्म-स्वरूप का तथा लक्ष्य पथ का भी सफल दृष्टा बन जाता है।
जैसे नदियाँ समुद्र में मिल जाती हैं, उसी प्रकार समस्त विकार वृत्तियाँ समीक्षण ध्यान के माध्यम से समत्व के महासागर में विलीन होकर समता भाव में रूपान्तरित हो जाती हैं तथा इस स्तर पर पहुँच कर समीक्षण ध्यान अपनी परिपूर्णता पा जाता है। तब चेतना भी अलौकिक एवं अनिर्वचनीय सच्चिदानन्द स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाती है।
चिन्तन आचरण में उतरे यह त्रिआयामी रूप समीक्षण साधना अपने तीन चरणों में विकसित होती हुई मनःशोधन तथा मनोविश्लेषण के सामर्थ्य को अवाप्त करे, पूर्णतः आत्म संयम को साधे एवं चरम व परम शक्ति
३१