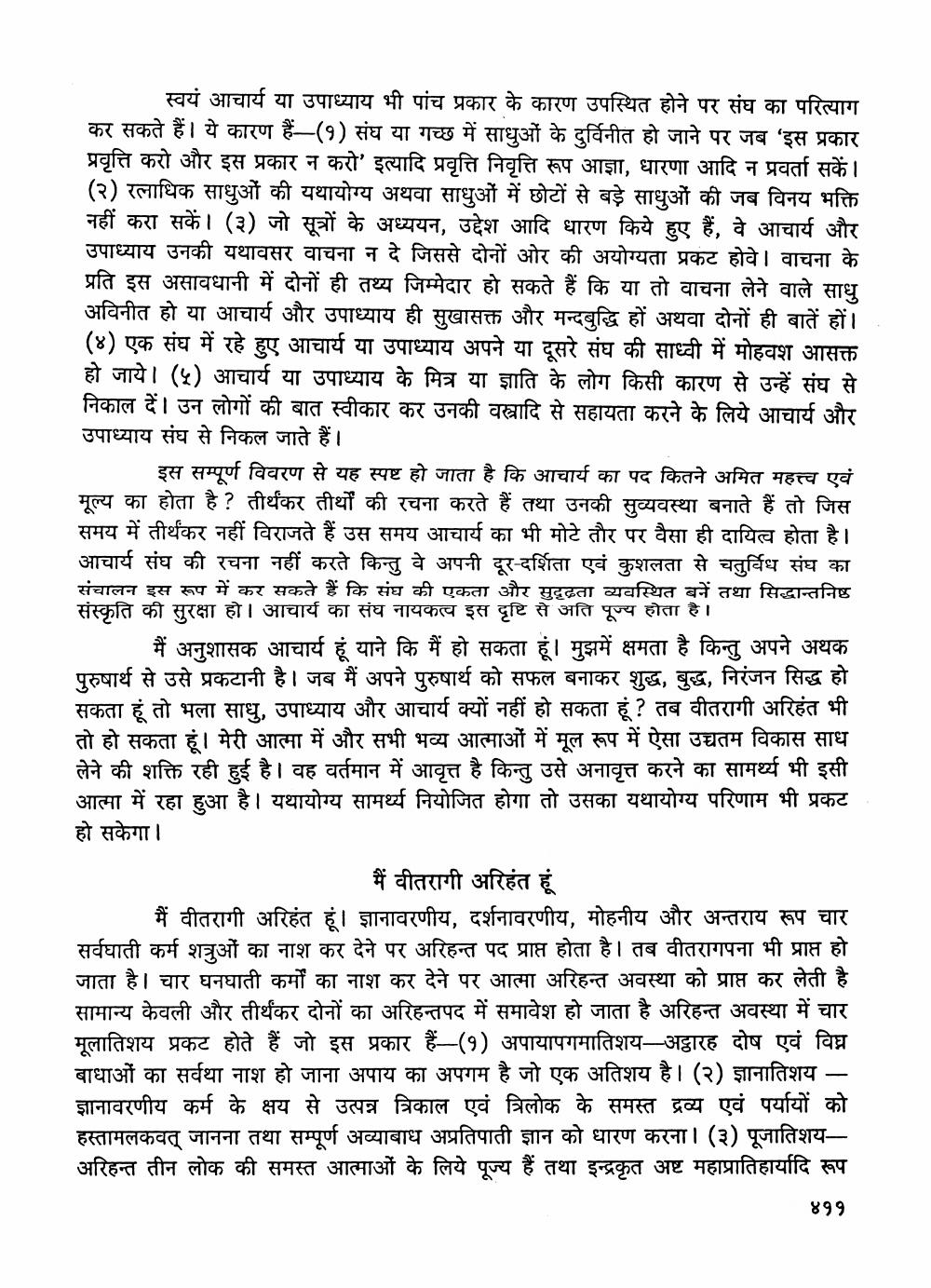________________
स्वयं आचार्य या उपाध्याय भी पांच प्रकार के कारण उपस्थित होने पर संघ का परित्याग कर सकते हैं। ये कारण हैं—(१) संघ या गच्छ में साधुओं के दुर्विनीत हो जाने पर जब 'इस प्रकार प्रवृत्ति करो और इस प्रकार न करो' इत्यादि प्रवृत्ति निवृत्ति रूप आज्ञा, धारणा आदि न प्रवर्ता सकें। (२) रत्नाधिक साधुओं की यथायोग्य अथवा साधुओं में छोटों से बड़े साधुओं की जब विनय भक्ति नहीं करा सकें। (३) जो सूत्रों के अध्ययन, उद्देश आदि धारण किये हुए हैं, वे आचार्य और उपाध्याय उनकी यथावसर वाचना न दे जिससे दोनों ओर की अयोग्यता प्रकट होवे। वाचना के प्रति इस असावधानी में दोनों ही तथ्य जिम्मेदार हो सकते हैं कि या तो वाचना लेने वाले साधु अविनीत हो या आचार्य और उपाध्याय ही सुखासक्त और मन्दबुद्धि हों अथवा दोनों ही बातें हों। (४) एक संघ में रहे हुए आचार्य या उपाध्याय अपने या दूसरे संघ की साध्वी में मोहवश आसक्त हो जाये। (५) आचार्य या उपाध्याय के मित्र या ज्ञाति के लोग किसी कारण से उन्हें संघ से निकाल दें। उन लोगों की बात स्वीकार कर उनकी वस्त्रादि से सहायता करने के लिये आचार्य और उपाध्याय संघ से निकल जाते हैं।
इस सम्पूर्ण विवरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि आचार्य का पद कितने अमित महत्त्व एवं मूल्य का होता है? तीर्थंकर तीर्थों की रचना करते हैं तथा उनकी सुव्यवस्था बनाते हैं तो जिस समय में तीर्थंकर नहीं विराजते हैं उस समय आचार्य का भी मोटे तौर पर वैसा ही दायित्व होता है। आचार्य संघ की रचना नहीं करते किन्तु वे अपनी दूर-दर्शिता एवं कुशलता से चतुर्विध संघ का संचालन इस रूप में कर सकते हैं कि संघ की एकता और सुदृढ़ता व्यवस्थित बनें तथा सिद्धान्तनिष्ठ संस्कृति की सुरक्षा हो। आचार्य का संघ नायकत्व इस दृष्टि से अति पूज्य होता है।
मैं अनुशासक आचार्य हूं याने कि मैं हो सकता हूं। मुझमें क्षमता है किन्तु अपने अथक पुरुषार्थ से उसे प्रकटानी है। जब मैं अपने पुरुषार्थ को सफल बनाकर शुद्ध, बुद्ध, निरंजन सिद्ध हो सकता हूं तो भला साधु, उपाध्याय और आचार्य क्यों नहीं हो सकता हूं? तब वीतरागी अरिहंत भी तो हो सकता हूं। मेरी आत्मा में और सभी भव्य आत्माओं में मूल रूप में ऐसा उच्चतम विकास साध लेने की शक्ति रही हुई है। वह वर्तमान में आवृत्त है किन्तु उसे अनावृत्त करने का सामर्थ्य भी इसी आत्मा में रहा हुआ है। यथायोग्य सामर्थ्य नियोजित होगा तो उसका यथायोग्य परिणाम भी प्रकट हो सकेगा।
मैं वीतरागी अरिहंत हूं मैं वीतरागी अरिहंत हूं। ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय और अन्तराय रूप चार सर्वघाती कर्म शत्रुओं का नाश कर देने पर अरिहन्त पद प्राप्त होता है। तब वीतरागपना भी प्राप्त हो जाता है। चार घनघाती कर्मों का नाश कर देने पर आत्मा अरिहन्त अवस्था को प्राप्त कर लेती है सामान्य केवली और तीर्थंकर दोनों का अरिहन्तपद में समावेश हो जाता है अरिहन्त अवस्था में चार मूलातिशय प्रकट होते हैं जो इस प्रकार हैं-(१) अपायापगमातिशय—अट्ठारह दोष एवं विघ्न बाधाओं का सर्वथा नाश हो जाना अपाय का अपगम है जो एक अतिशय है। (२) ज्ञानातिशय - ज्ञानावरणीय कर्म के क्षय से उत्पन्न त्रिकाल एवं त्रिलोक के समस्त द्रव्य एवं पर्यायों को हस्तामलकवत् जानना तथा सम्पूर्ण अव्याबाध अप्रतिपाती ज्ञान को धारण करना। (३) पूजातिशयअरिहन्त तीन लोक की समस्त आत्माओं के लिये पूज्य हैं तथा इन्द्रकृत अष्ट महाप्रातिहार्यादि रूप
४११