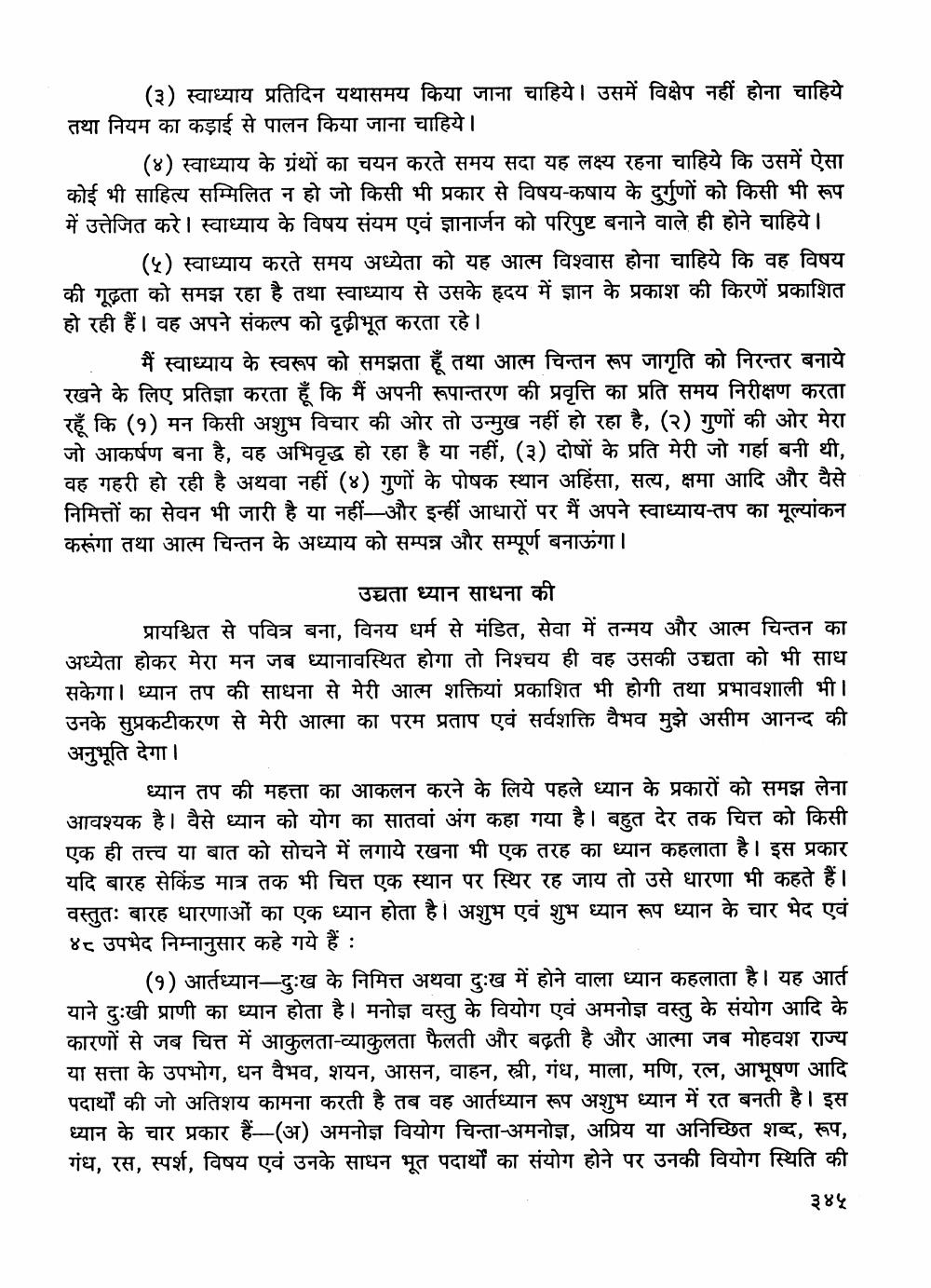________________
(३) स्वाध्याय प्रतिदिन यथासमय किया जाना चाहिये। उसमें विक्षेप नहीं होना चाहिये तथा नियम का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिये।
(४) स्वाध्याय के ग्रंथों का चयन करते समय सदा यह लक्ष्य रहना चाहिये कि उसमें ऐसा कोई भी साहित्य सम्मिलित न हो जो किसी भी प्रकार से विषय-कषाय के दुर्गुणों को किसी भी रूप में उत्तेजित करे। स्वाध्याय के विषय संयम एवं ज्ञानार्जन को परिपुष्ट बनाने वाले ही होने चाहिये।
(५) स्वाध्याय करते समय अध्येता को यह आत्म विश्वास होना चाहिये कि वह विषय की गूढ़ता को समझ रहा है तथा स्वाध्याय से उसके हृदय में ज्ञान के प्रकाश की किरणें प्रकाशित हो रही हैं। वह अपने संकल्प को दृढ़ीभूत करता रहे।
... मैं स्वाध्याय के स्वरूप को समझता हूँ तथा आत्म चिन्तन रूप जागृति को निरन्तर बनाये रखने के लिए प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं अपनी रूपान्तरण की प्रवृत्ति का प्रति समय निरीक्षण करता रहूँ कि (१) मन किसी अशुभ विचार की ओर तो उन्मुख नहीं हो रहा है, (२) गुणों की ओर मेरा जो आकर्षण बना है, वह अभिवृद्ध हो रहा है या नहीं, (३) दोषों के प्रति मेरी जो गर्दा बनी थी, वह गहरी हो रही है अथवा नहीं (४) गुणों के पोषक स्थान अहिंसा, सत्य, क्षमा आदि और वैसे निमित्तों का सेवन भी जारी है या नहीं और इन्हीं आधारों पर मैं अपने स्वाध्याय-तप का मूल्यांकन करूंगा तथा आत्म चिन्तन के अध्याय को सम्पन्न और सम्पूर्ण बनाऊंगा।
__ उच्चता ध्यान साधना की प्रायश्चित से पवित्र बना, विनय धर्म से मंडित, सेवा में तन्मय और आत्म चिन्तन का अध्येता होकर मेरा मन जब ध्यानावस्थित होगा तो निश्चय ही वह उसकी उच्चता को भी साध सकेगा। ध्यान तप की साधना से मेरी आत्म शक्तियां प्रकाशित भी होगी तथा प्रभावशाली भी। उनके सुप्रकटीकरण से मेरी आत्मा का परम प्रताप एवं सर्वशक्ति वैभव मुझे असीम आनन्द की अनुभूति देगा।
ध्यान तप की महत्ता का आकलन करने के लिये पहले ध्यान के प्रकारों को समझ लेना आवश्यक है। वैसे ध्यान को योग का सातवां अंग कहा गया है। बहुत देर तक चित्त को किसी एक ही तत्त्व या बात को सोचने में लगाये रखना भी एक तरह का ध्यान कहलाता है। इस प्रकार यदि बारह सेकिंड मात्र तक भी चित्त एक स्थान पर स्थिर रह जाय तो उसे धारणा भी कहते हैं। वस्तुतः बारह धारणाओं का एक ध्यान होता है। अशुभ एवं शुभ ध्यान रूप ध्यान के चार भेद एवं ४८ उपभेद निम्नानुसार कहे गये हैं :
(१) आर्तध्यान-दुःख के निमित्त अथवा दुःख में होने वाला ध्यान कहलाता है। यह आर्त याने दुःखी प्राणी का ध्यान होता है। मनोज्ञ वस्तु के वियोग एवं अमनोज्ञ वस्तु के संयोग आदि के कारणों से जब चित्त में आकुलता-व्याकुलता फैलती और बढ़ती है और आत्मा जब मोहवश राज्य या सत्ता के उपभोग, धन वैभव, शयन, आसन, वाहन, स्त्री, गंध, माला, मणि, रत्न, आभूषण आदि पदार्थों की जो अतिशय कामना करती है तब वह आर्तध्यान रूप अशुभ ध्यान में रत बनती है। इस ध्यान के चार प्रकार हैं-(अ) अमनोज्ञ वियोग चिन्ता-अमनोज्ञ, अप्रिय या अनिच्छित शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श, विषय एवं उनके साधन भूत पदार्थों का संयोग होने पर उनकी वियोग स्थिति की
३४५