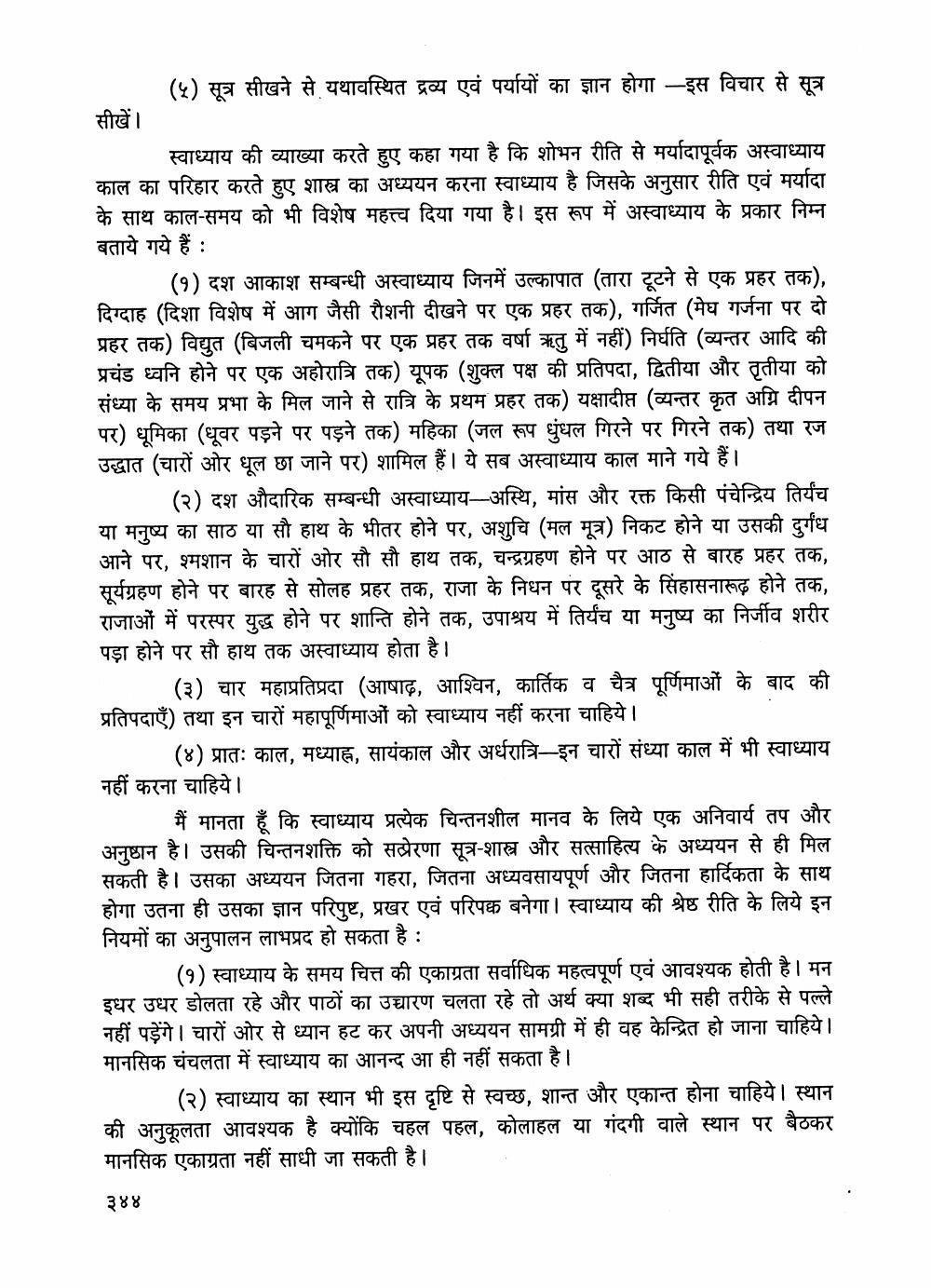________________
(५) सूत्र सीखने से यथावस्थित द्रव्य एवं पर्यायों का ज्ञान होगा - इस विचार से सूत्र
स्वाध्याय की व्याख्या करते हुए कहा गया है कि शोभन रीति से मर्यादापूर्वक अस्वाध्याय काल का परिहार करते हुए शास्त्र का अध्ययन करना स्वाध्याय है जिसके अनुसार रीति एवं मर्यादा के साथ काल - समय को भी विशेष महत्त्व दिया गया है। इस रूप में अस्वाध्याय के प्रकार निम्न बताये गये हैं:
सीखें।
(१) दश आकाश सम्बन्धी अस्वाध्याय जिनमें उल्कापात (तारा टूटने से एक प्रहर तक ), दिग्दाह (दिशा विशेष में आग जैसी रौशनी दीखने पर एक प्रहर तक ), गर्जित (मेघ गर्जना पर दो प्रहर तक) विद्युत ( बिजली चमकने पर एक प्रहर तक वर्षा ऋतु में नहीं) निर्धति (व्यन्तर आदि की प्रचंड ध्वनि होने पर एक अहोरात्र तक) यूपक ( शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया और तृतीया को संध्या के समय प्रभा के मिल जाने से रात्रि के प्रथम प्रहर तक ) यक्षादीप्त (व्यन्तर कृत अग्नि दीपन पर) धूमिका (धूवर पड़ने पर पड़ने तक) महिका (जल रूप धुंधल गिरने पर गिरने तक) तथा रज उद्धात (चारों ओर धूल छा जाने पर) शामिल हैं। ये सब अस्वाध्याय काल माने गये हैं ।
(२) दश औदारिक सम्बन्धी अस्वाध्याय – अस्थि, मांस और रक्त किसी पंचेन्द्रिय तिर्यंच या मनुष्य का साठ या सौ हाथ के भीतर होने पर, अशुचि (मल मूत्र) निकट होने या उसकी दुर्गंध आने पर, श्मशान के चारों ओर सौ सौ हाथ तक, चन्द्रग्रहण होने पर आठ से बारह प्रहर तक, सूर्यग्रहण होने पर बारह से सोलह प्रहर तक, राजा के निधन पर दूसरे के सिंहासनारूढ़ होने तक, राजाओं में परस्पर युद्ध होने पर शान्ति होने तक, उपाश्रय में तिर्यंच या मनुष्य का निर्जीव शरीर पड़ा होने पर सौ हाथ तक अस्वाध्याय होता है ।
(३) चार महाप्रतिप्रदा ( आषाढ़, आश्विन, कार्तिक व चैत्र पूर्णिमाओं के बाद की प्रतिपदाएँ) तथा इन चारों महापूर्णिमाओं को स्वाध्याय नहीं करना चाहिये ।
(४) प्रातः काल, मध्याह्न, सायंकाल और अर्धरात्रि - इन चारों संध्या काल में भी स्वाध्याय नहीं करना चाहिये ।
मैं मानता हूँ कि स्वाध्याय प्रत्येक चिन्तनशील मानव के लिये एक अनिवार्य तप और अनुष्ठान है। उसकी चिन्तनशक्ति को सत्प्रेरणा सूत्र - शास्त्र और सत्साहित्य के अध्ययन से ही मिल सकती है। उसका अध्ययन जितना गहरा, जितना अध्यवसायपूर्ण और जितना हार्दिकता के साथ होगा उतना ही उसका ज्ञान परिपुष्ट, प्रखर एवं परिपक्क बनेगा। स्वाध्याय की श्रेष्ठ रीति के लिये इन नियमों का अनुपालन लाभप्रद हो सकता है :
(१) स्वाध्याय के समय चित्त की एकाग्रता सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक होती है । मन इधर उधर डोलता रहे और पाठों का उच्चारण चलता रहे तो अर्थ क्या शब्द भी सही तरीके से पल्ले नहीं पड़ेंगे। चारों ओर से ध्यान हट कर अपनी अध्ययन सामग्री में ही वह केन्द्रित हो जाना चाहिये । मानसिक चंचलता में स्वाध्याय का आनन्द आ ही नहीं सकता है।
(२) स्वाध्याय का स्थान भी इस दृष्टि से स्वच्छ, शान्त और एकान्त होना चाहिये । स्थान की अनुकूलता आवश्यक है क्योंकि चहल पहल, कोलाहल या गंदगी वाले स्थान पर बैठकर मानसिक एकाग्रता नहीं साधी जा सकती है।
३४४