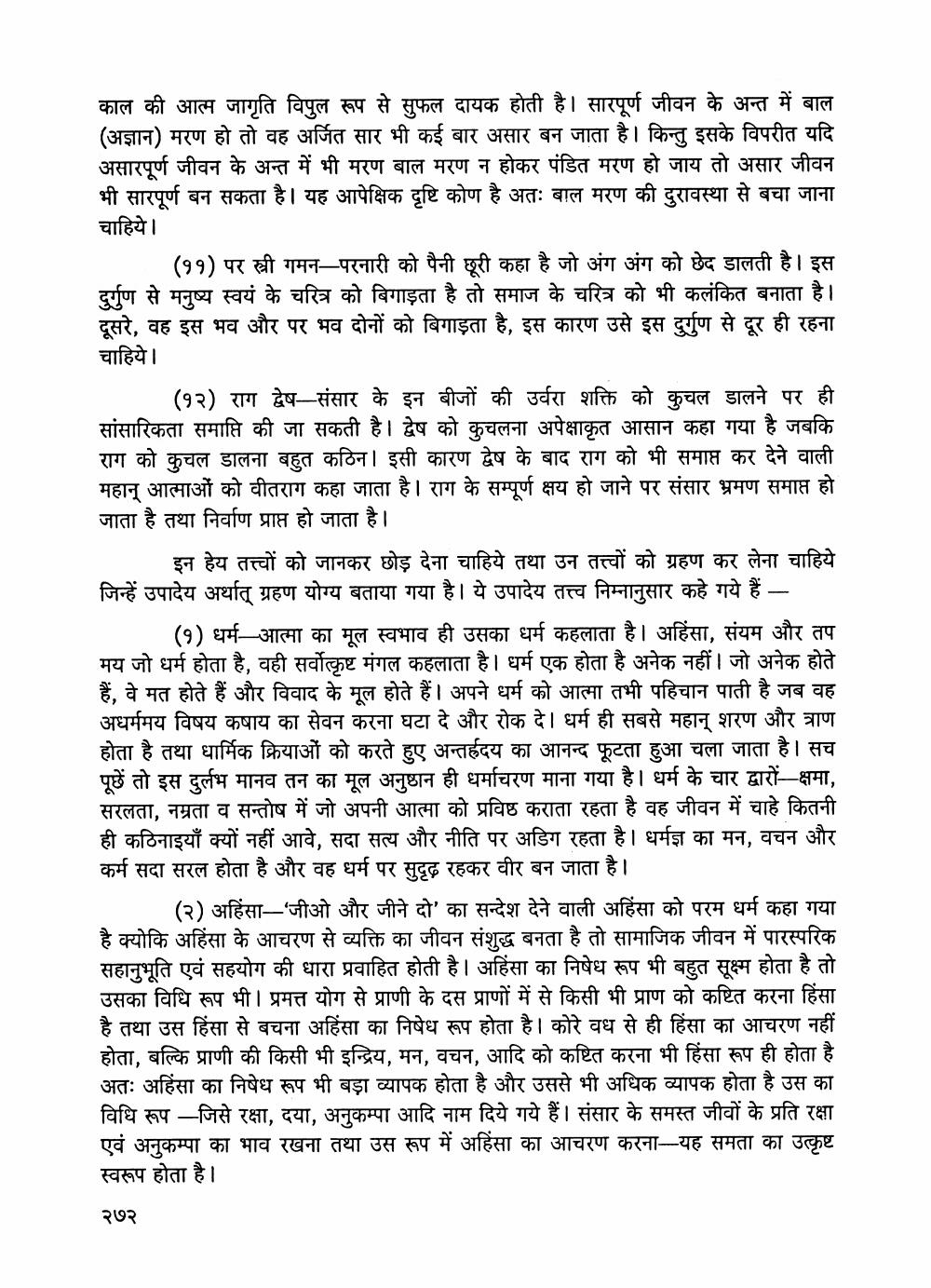________________
काल की आत्म जागृति विपुल रूप से सुफल दायक होती है। सारपूर्ण जीवन के अन्त में बाल (अज्ञान) मरण हो तो वह अर्जित सार भी कई बार असार बन जाता है। किन्तु इसके विपरीत यदि असारपूर्ण जीवन के अन्त में भी मरण बाल मरण न होकर पंडित मरण हो जाय तो असार जीवन भी सारपूर्ण बन सकता है। यह आपेक्षिक दृष्टि कोण है अतः बाल मरण की दुरावस्था से बचा जाना चाहिये।
(११) पर स्त्री गमन–परनारी को पैनी छूरी कहा है जो अंग अंग को छेद डालती है। इस दुर्गुण से मनुष्य स्वयं के चरित्र को बिगाड़ता है तो समाज के चरित्र को भी कलंकित बनाता है। दूसरे, वह इस भव और पर भव दोनों को बिगाड़ता है, इस कारण उसे इस दुर्गुण से दूर ही रहना चाहिये।
(१२) राग द्वेष—संसार के इन बीजों की उर्वरा शक्ति को कुचल डालने पर ही सांसारिकता समाप्ति की जा सकती है। द्वेष को कुचलना अपेक्षाकृत आसान कहा गया है जबकि राग को कुचल डालना बहुत कठिन। इसी कारण द्वेष के बाद राग को भी समाप्त कर देने वाली महान् आत्माओं को वीतराग कहा जाता है। राग के सम्पूर्ण क्षय हो जाने पर संसार भ्रमण समाप्त हो जाता है तथा निर्वाण प्राप्त हो जाता है।
इन हेय तत्त्वों को जानकर छोड़ देना चाहिये तथा उन तत्त्वों को ग्रहण कर लेना चाहिये जिन्हें उपादेय अर्थात् ग्रहण योग्य बताया गया है। ये उपादेय तत्त्व निम्नानुसार कहे गये हैं -
(१) धर्म आत्मा का मूल स्वभाव ही उसका धर्म कहलाता है। अहिंसा, संयम और तप जो धर्म होता है, वही सर्वोत्कष्ट मंगल कहलाता है। धर्म एक होता है अनेक नहीं। जो अनेक होते हैं, वे मत होते हैं और विवाद के मूल होते हैं। अपने धर्म को आत्मा तभी पहिचान पाती है जब वह अधर्ममय विषय कषाय का सेवन करना घटा दे और रोक दे। धर्म ही सबसे महान् शरण और त्राण होता है तथा धार्मिक क्रियाओं को करते हुए अन्तर्हृदय का आनन्द फूटता हुआ चला जाता है। सच पूछे तो इस दुर्लभ मानव तन का मूल अनुष्ठान ही धर्माचरण माना गया है। धर्म के चार द्वारों—क्षमा, सरलता, नम्रता व सन्तोष में जो अपनी आत्मा को प्रविष्ठ कराता रहता है वह जीवन में चाहे कितनी ही कठिनाइयाँ क्यों नहीं आवे, सदा सत्य और नीति पर अडिग रहता है। धर्मज्ञ का मन, वचन और कर्म सदा सरल होता है और वह धर्म पर सुदृढ़ रहकर वीर बन जाता है।
(२) अहिंसा-'जीओ और जीने दो' का सन्देश देने वाली अहिंसा को परम धर्म कहा गया है क्योकि अहिंसा के आचरण से व्यक्ति का जीवन संशुद्ध बनता है तो सामाजिक जीवन में पारस्परिक सहानुभूति एवं सहयोग की धारा प्रवाहित होती है। अहिंसा का निषेध रूप भी बहुत सूक्ष्म होता है तो उसका विधि रूप भी। प्रमत्त योग से प्राणी के दस प्राणों में से किसी भी प्राण को कष्टित करना हिंसा है तथा उस हिंसा से बचना अहिंसा का निषेध रूप होता है। कोरे वध से ही हिंसा का आचरण नहीं होता, बल्कि प्राणी की किसी भी इन्द्रिय, मन, वचन, आदि को कष्टित करना भी हिंसा रूप ही होता है अतः अहिंसा का निषेध रूप भी बड़ा व्यापक होता है और उससे भी अधिक व्यापक होता है उस का विधि रूप —जिसे रक्षा, दया, अनुकम्पा आदि नाम दिये गये हैं। संसार के समस्त जीवों के प्रति रक्षा एवं अनुकम्पा का भाव रखना तथा उस रूप में अहिंसा का आचरण करना—यह समता का उत्कृष्ट स्वरूप होता है।
२७२