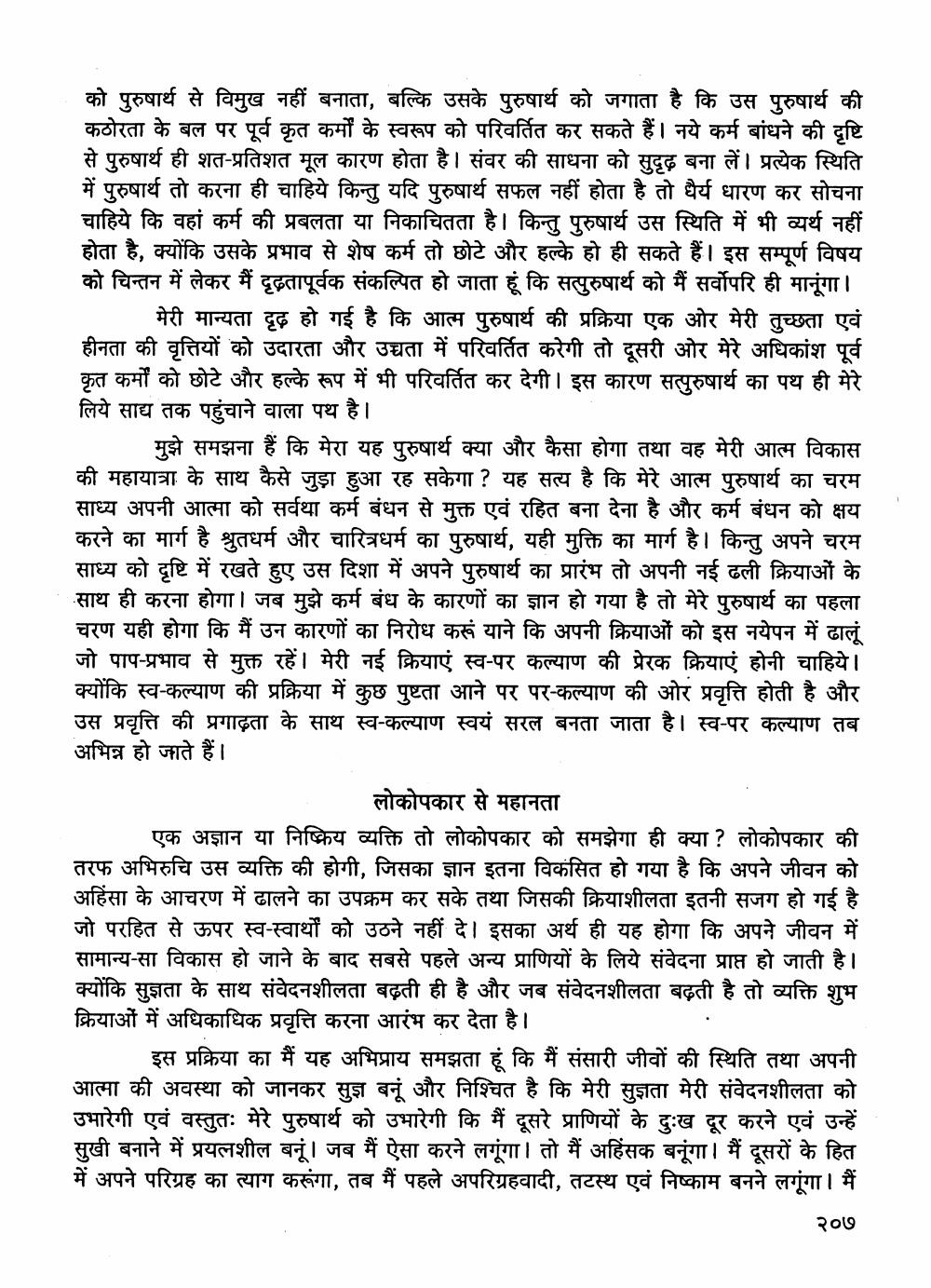________________
को पुरुषार्थ से विमुख नहीं बनाता, बल्कि उसके पुरुषार्थ को जगाता है कि उस पुरुषार्थ की कठोरता के बल पर पूर्व कृत कर्मों के स्वरूप को परिवर्तित कर सकते हैं। नये कर्म बांधने की दृष्टि से पुरुषार्थ ही शत-प्रतिशत मूल कारण होता है । संवर की साधना को सुदृढ़ बना लें। प्रत्येक स्थिति पुरुषार्थ तो करना ही चाहिये किन्तु यदि पुरुषार्थ सफल नहीं होता है तो धैर्य धारण कर सोचना चाहिये कि वहां कर्म की प्रबलता या निकाचितता है । किन्तु पुरुषार्थ उस स्थिति में भी व्यर्थ नहीं होता है, क्योंकि उसके प्रभाव से शेष कर्म तो छोटे और हल्के हो ही सकते हैं। इस सम्पूर्ण विषय को चिन्तन में लेकर मैं दृढ़तापूर्वक संकल्पित हो जाता हूं कि सत्पुरुषार्थ को मैं सर्वोपरि ही मानूंगा ।
मेरी मान्यता दृढ़ हो गई है कि आत्म पुरुषार्थ की प्रक्रिया एक ओर मेरी तुच्छता एवं हीनता की वृत्तियों को उदारता और उच्चता में परिवर्तित करेगी तो दूसरी ओर मेरे अधिकांश पूर्व कृत कर्मों को छोटे और हल्के रूप में भी परिवर्तित कर देगी। इस कारण सत्पुरुषार्थ का पथ ही मेरे लिये साद्य तक पहुंचाने वाला पथ है ।
मुझे समझना हैं कि मेरा यह पुरुषार्थ क्या और कैसा होगा तथा वह मेरी आत्म विकास की महायात्रा के साथ कैसे जुड़ा हुआ रह सकेगा ? यह सत्य है कि मेरे आत्म पुरुषार्थ का चरम साध्य अपनी आत्मा को सर्वथा कर्म बंधन से मुक्त एवं रहित बना देना है और कर्म बंधन को क्षय करने का मार्ग है श्रुतधर्म और चारित्रधर्म का पुरुषार्थ, यही मुक्ति का मार्ग है। किन्तु अपने चरम साध्य को दृष्टि में रखते हुए उस दिशा में अपने पुरुषार्थ का प्रारंभ तो अपनी नई ढली क्रियाओं के साथ ही करना होगा। जब मुझे कर्म बंध के कारणों का ज्ञान हो गया है तो मेरे पुरुषार्थ का पहला चरण यही होगा कि मैं उन कारणों का निरोध करूं याने कि अपनी क्रियाओं को इस नयेपन में ढालूं जो पाप प्रभाव से मुक्त रहें । मेरी नई क्रियाएं स्व-पर कल्याण की प्रेरक क्रियाएं होनी चाहिये । क्योंकि स्व-कल्याण की प्रक्रिया में कुछ पुष्टता आने पर पर- कल्याण की ओर प्रवृत्ति होती है और उस प्रवृत्ति की प्रगाढ़ता के साथ स्व-कल्याण स्वयं सरल बनता जाता है । स्व-पर कल्याण तब अभिन्न हो जाते हैं ।
लोकोपकार से महानता
एक अज्ञान या निष्क्रिय व्यक्ति तो लोकोपकार को समझेगा ही क्या ? लोकोपकार की तरफ अभिरुचि उस व्यक्ति की होगी, जिसका ज्ञान इतना विकसित हो गया है कि अपने जीवन को अहिंसा के आचरण में ढालने का उपक्रम कर सके तथा जिसकी क्रियाशीलता इतनी सजग हो गई है जो परहित से ऊपर स्व-स्वार्थों को उठने नहीं दे। इसका अर्थ ही यह होगा कि अपने जीवन में सामान्य-सा विकास हो जाने के बाद सबसे पहले अन्य प्राणियों के लिये संवेदना प्राप्त हो जाती है। क्योंकि सुज्ञता के साथ संवेदनशीलता बढ़ती ही है और जब संवेदनशीलता बढ़ती है तो व्यक्ति शुभ क्रियाओं में अधिकाधिक प्रवृत्ति करना आरंभ कर देता है।
इस प्रक्रिया का मैं यह अभिप्राय समझता हूं कि मैं संसारी जीवों की स्थिति तथा अपनी आत्मा की अवस्था को जानकर सुज्ञ बनूं और निश्चित है कि मेरी सुज्ञता मेरी संवेदनशीलता को उभारेगी एवं वस्तुतः मेरे पुरुषार्थ को उभारेगी कि मैं दूसरे प्राणियों के दुःख दूर करने एवं उन्हें सुखी बनाने में प्रयत्नशील बनूं। जब मैं ऐसा करने लगूंगा । तो मैं अहिंसक बनूंगा। मैं दूसरों के हित में अपने परिग्रह का त्याग करूंगा, तब मैं पहले अपरिग्रहवादी, तटस्थ एवं निष्काम बनने लगूंगा । मैं
२०७