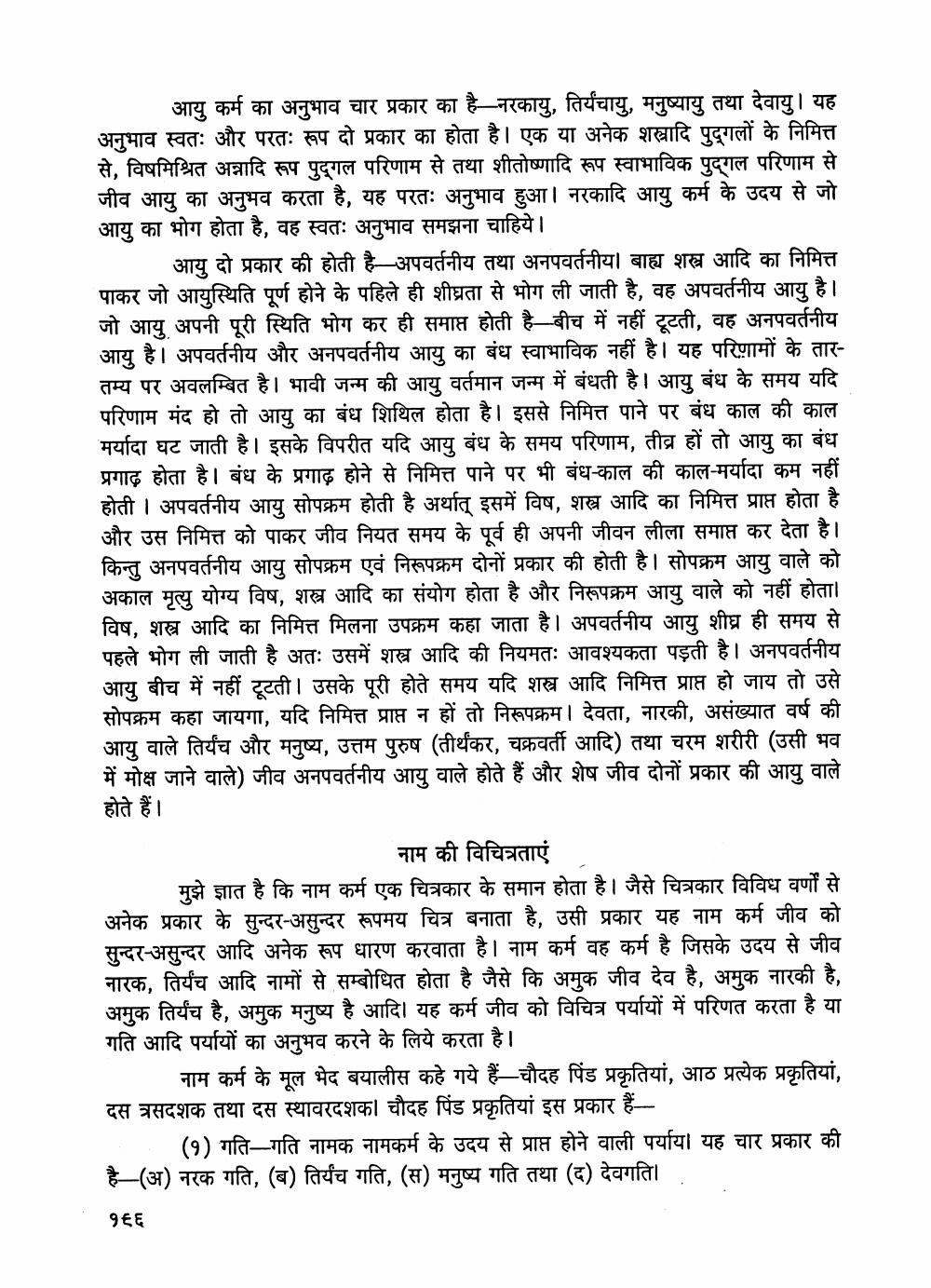________________
आयु कर्म का अनुभाव चार प्रकार का है—नरकायु, तिर्यंचायु, मनुष्यायु तथा देवायु। यह अनुभाव स्वतः और परतः रूप दो प्रकार का होता है। एक या अनेक शस्त्रादि पुद्गलों के निमित्त से, विषमिश्रित अन्नादि रूप पुद्गल परिणाम से तथा शीतोष्णादि रूप स्वाभाविक पुद्गल परिणाम से जीव आयु का अनुभव करता है, यह परतः अनुभाव हुआ। नरकादि आयु कर्म के उदय से जो आयु का भोग होता है, वह स्वतः अनुभाव समझना चाहिये।
आयु दो प्रकार की होती है—अपवर्तनीय तथा अनपवर्तनीय। बाह्य शस्त्र आदि का निमित्त पाकर जो आयुस्थिति पूर्ण होने के पहिले ही शीघ्रता से भोग ली जाती है, वह अपवर्तनीय आयु है। जो आयु अपनी पूरी स्थिति भोग कर ही समाप्त होती है—बीच में नहीं टूटती, वह अनपवर्तनीय आयु है। अपवर्तनीय और अनपवर्तनीय आयु का बंध स्वाभाविक नहीं है। यह परिणामों के तारतम्य पर अवलम्बित है। भावी जन्म की आयु वर्तमान जन्म में बंधती है। आयु बंध के समय यदि परिणाम मंद हो तो आयु का बंध शिथिल होता है। इससे निमित्त पाने पर बंध काल की काल मर्यादा घट जाती है। इसके विपरीत यदि आयु बंध के समय परिणाम, तीव्र हों तो आयु का बंध प्रगाढ़ होता है। बंध के प्रगाढ़ होने से निमित्त पाने पर भी बंध-काल की काल-मर्यादा कम नहीं होती । अपवर्तनीय आयु सोपक्रम होती है अर्थात् इसमें विष, शस्त्र आदि का निमित्त प्राप्त होता है
और उस निमित्त को पाकर जीव नियत समय के पूर्व ही अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। किन्तु अनपवर्तनीय आयु सोपक्रम एवं निरूपक्रम दोनों प्रकार की होती है। सोपक्रम आयु वाले को
अकाल मृत्यु योग्य विष, शस्त्र आदि का संयोग होता है और निरूपक्रम आयु वाले को नहीं होता। विष, शस्त्र आदि का निमित्त मिलना उपक्रम कहा जाता है। अपवर्तनीय आयु शीघ्र ही समय से पहले भोग ली जाती है अतः उसमें शस्त्र आदि की नियमतः आवश्यकता पड़ती है। अनपवर्तनीय आयु बीच में नहीं टूटती। उसके पूरी होते समय यदि शस्त्र आदि निमित्त प्राप्त हो जाय तो उसे सोपक्रम कहा जायगा, यदि निमित्त प्राप्त न हों तो निरूपक्रम । देवता, नारकी, असंख्यात वर्ष की आयु वाले तिर्यंच और मनुष्य, उत्तम पुरुष (तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि) तथा चरम शरीरी (उसी भव में मोक्ष जाने वाले) जीव अनपवर्तनीय आयु वाले होते हैं और शेष जीव दोनों प्रकार की आयु वाले होते हैं।
नाम की विचित्रताएं ___ मुझे ज्ञात है कि नाम कर्म एक चित्रकार के समान होता है। जैसे चित्रकार विविध वर्णों से अनेक प्रकार के सुन्दर-असुन्दर रूपमय चित्र बनाता है, उसी प्रकार यह नाम कर्म जीव को सुन्दर-असुन्दर आदि अनेक रूप धारण करवाता है। नाम कर्म वह कर्म है जिसके उदय से जीव नारक, तिर्यंच आदि नामों से सम्बोधित होता है जैसे कि अमुक जीव देव है, अमुक नारकी है, अमुक तिर्यंच है, अमुक मनुष्य है आदि। यह कर्म जीव को विचित्र पर्यायों में परिणत करता है या गति आदि पर्यायों का अनुभव करने के लिये करता है।
नाम कर्म के मूल भेद बयालीस कहे गये हैं चौदह पिंड प्रकृतियां, आठ प्रत्येक प्रकृतियां, दस त्रसदशक तथा दस स्थावरदशक| चौदह पिंड प्रकृतियां इस प्रकार हैं
(१) गति—गति नामक नामकर्म के उदय से प्राप्त होने वाली पर्याय। यह चार प्रकार की है—(अ) नरक गति, (ब) तिर्यंच गति, (स) मनुष्य गति तथा (द) देवगति। १६६