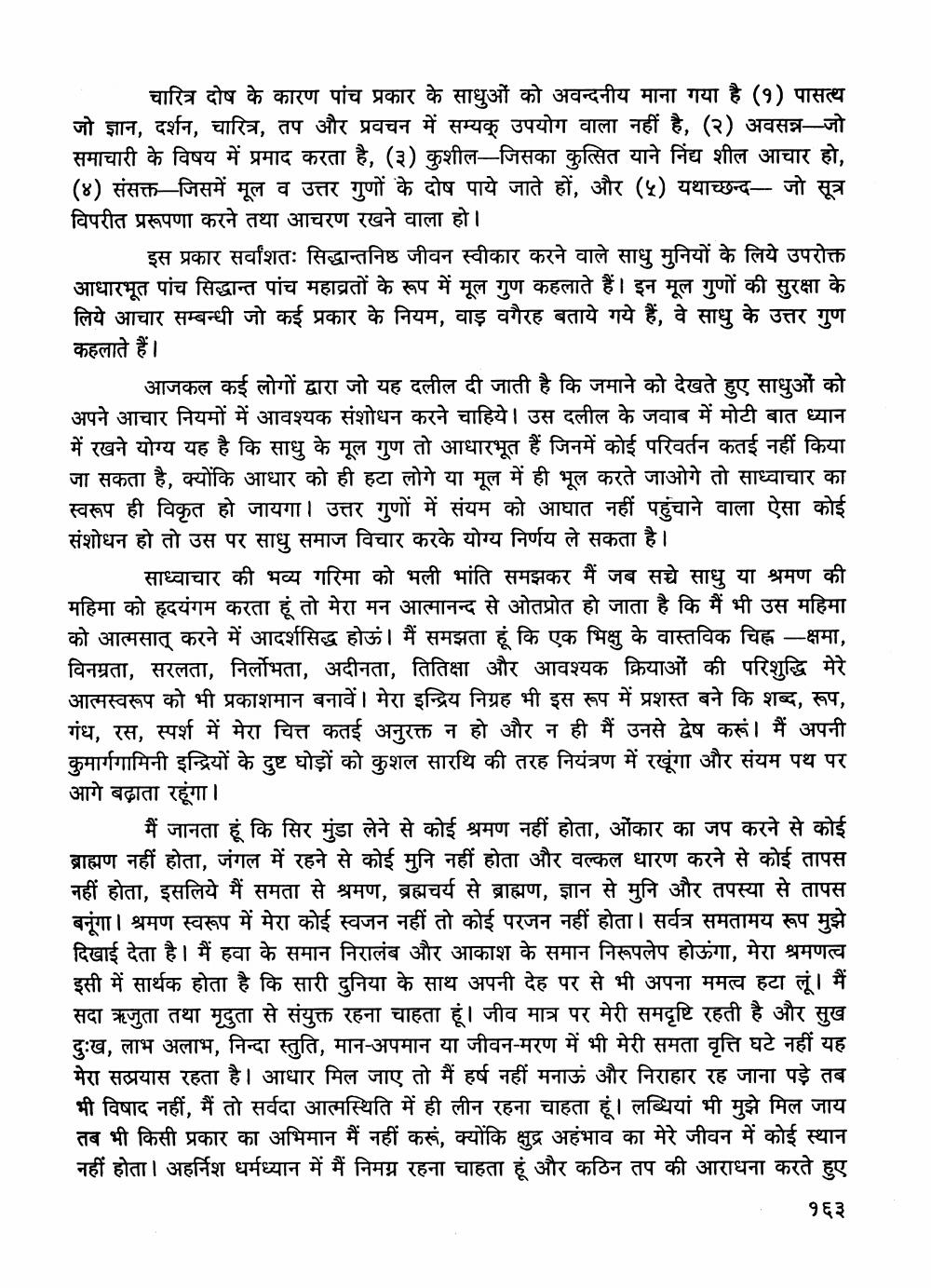________________
चारित्र दोष के कारण पांच प्रकार के साधुओं को अवन्दनीय माना गया है (१) पासत्थ जो ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और प्रवचन में सम्यक् उपयोग वाला नहीं है, (२) अवसन्न — जो समाचारी के विषय में प्रमाद करता है, (३) कुशील - जिसका कुत्सित याने निंद्य शील आचार हो, (४) संसक्त-— जिसमें मूल व उत्तर गुणों के दोष पाये जाते हों, और (५) यथाच्छन्द - जो सूत्र विपरीत प्ररूपणा करने तथा आचरण रखने वाला हो ।
इस प्रकार सर्वांशतः सिद्धान्तनिष्ठ जीवन स्वीकार करने वाले साधु मुनियों के लिये उपरोक्त आधारभूत पांच सिद्धान्त पांच महाव्रतों के रूप में मूल गुण कहलाते हैं। इन मूल गुणों की सुरक्षा के लिये आचार सम्बन्धी जो कई प्रकार के नियम, वाड़ वगैरह बताये गये हैं, वे साधु के उत्तर गुण कहलाते हैं ।
आजकल कई लोगों द्वारा जो यह दलील दी जाती है कि जमाने को देखते हुए साधुओं को अपने आचार नियमों में आवश्यक संशोधन करने चाहिये। उस दलील के जवाब में मोटी बात ध्यान में रखने योग्य यह है कि साधु के मूल गुण तो आधारभूत हैं जिनमें कोई परिवर्तन कतई नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आधार को ही हटा लोगे या मूल में ही भूल करते जाओगे तो साध्वाचार का स्वरूप ही विकृत हो जायगा । उत्तर गुणों में संयम को आघात नहीं पहुंचाने वाला ऐसा कोई संशोधन हो तो उस पर साधु समाज विचार करके योग्य निर्णय ले सकता है।
साध्वाचार की भव्य गरिमा को भली भांति समझकर मैं जब सच्चे साधु या श्रमण की महिमा को हृदयंगम करता हूं तो मेरा मन आत्मानन्द से ओतप्रोत हो जाता है कि मैं भी उस महिमा को आत्मसात् करने में आदर्शसिद्ध होऊं । मैं समझता हूं कि एक भिक्षु के वास्तविक चिह्न – क्षमा, विनम्रता, सरलता, निर्लोभता, अदीनता, तितिक्षा और आवश्यक क्रियाओं की परिशुद्धि मेरे आत्मस्वरूप को भी प्रकाशमान बनावें । मेरा इन्द्रिय निग्रह भी इस रूप में प्रशस्त बने कि शब्द, रूप, गंध, रस, स्पर्श में मेरा चित्त कतई अनुरक्त न हो और न ही मैं उनसे द्वेष करूं। मैं अपनी कुमार्गगामिनी इन्द्रियों के दुष्ट घोड़ों को कुशल सारथि की तरह नियंत्रण में रखूंगा और संयम पथ पर आगे बढ़ाता रहूंगा ।
मैं जानता हूं कि सिर मुंडा लेने से कोई श्रमण नहीं होता, ओंकार का जप करने से कोई ब्राह्मण नहीं होता, जंगल में रहने से कोई मुनि नहीं होता और वल्कल धारण करने से कोई तापस नहीं होता, इसलिये मैं समता से श्रमण, ब्रह्मचर्य से ब्राह्मण, ज्ञान से मुनि और तपस्या तापस बनूंगा । श्रमण स्वरूप में मेरा कोई स्वजन नहीं तो कोई परजन नहीं होता । सर्वत्र समतामय रूप मुझे दिखाई देता है। मैं हवा के समान निरालंब और आकाश के समान निरूपलेप होऊंगा, मेरा श्रमणत्व इसी में सार्थक होता है कि सारी दुनिया के साथ अपनी देह पर से भी अपना ममत्व हटा लूं। मैं सदा ऋजुता तथा मृदुता से संयुक्त रहना चाहता हूं। जीव मात्र पर मेरी समदृष्टि रहती है और सुख दुःख, लाभ अलाभ, निन्दा स्तुति, मान-अपमान या जीवन-मरण में भी मेरी समता वृत्ति घटे नहीं यह मेरा सत्प्रयास रहता है। आधार मिल जाए तो हर्ष नहीं मनाऊं और निराहार रह जाना पड़े तब भी विषाद नहीं, मैं तो सर्वदा आत्मस्थिति में ही लीन रहना चाहता हूं । लब्धियां भी मुझे मिल जाय तब भी किसी प्रकार का अभिमान मैं नहीं करूं, क्योंकि क्षुद्र अहंभाव का मेरे जीवन में कोई स्थान नहीं होता। अहर्निश धर्मध्यान में मैं निमग्न रहना चाहता हूं और कठिन तप की आराधना करते हुए
१६३