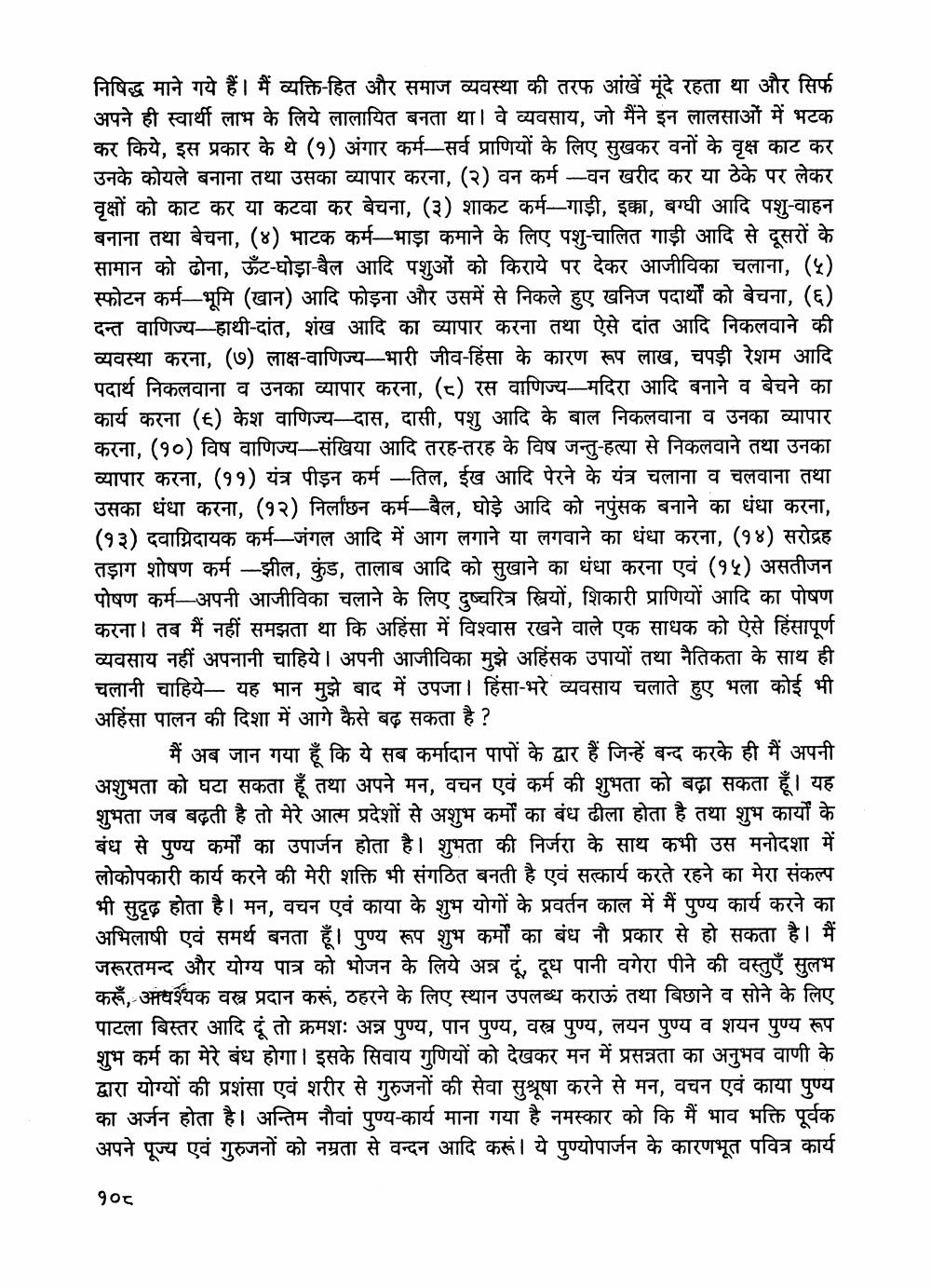________________
निषिद्ध माने गये हैं। मैं व्यक्ति-हित और समाज व्यवस्था की तरफ आंखें मूंदे रहता था और सिर्फ अपने ही स्वार्थी लाभ के लिये लालायित बनता था। वे व्यवसाय, जो मैंने इन लालसाओं में भटक कर किये, इस प्रकार के थे ( १ ) अंगार कर्म - सर्व प्राणियों के लिए सुखकर वनों के वृक्ष काट कर उनके कोयले बनाना तथा उसका व्यापार करना, (२) वन कर्म – वन खरीद कर या ठेके पर लेकर वृक्षों को काट कर या कटवा कर बेचना, (३) शाकट कर्म - गाड़ी, इक्का, बग्घी आदि पशु-वाहन बनाना तथा बेचना, (४) भाटक कर्म - भाड़ा कमाने के लिए पशु-चालित गाड़ी आदि से दूसरों के सामान को ढोना, ऊँट-घोड़ा-बैल आदि पशुओं को किराये पर देकर आजीविका चलाना, (५) स्फोटन कर्म - भूमि (खान) आदि फोड़ना और उसमें से निकले हुए खनिज पदार्थों को बेचना, (६) दन्त वाणिज्य - हाथी दांत, शंख आदि का व्यापार करना तथा ऐसे दांत आदि निकलवाने की व्यवस्था करना, (७) लाक्ष-वाणिज्य - भारी जीव-हिंसा के कारण रूप लाख, चपड़ी रेशम आदि पदार्थ निकलवाना व उनका व्यापार करना, (८) रस वाणिज्य – मदिरा आदि बनाने व बेचने का कार्य करना (६) केश वाणिज्य – दास, दासी, पशु आदि के बाल निकलवाना व उनका व्यापार करना, (१०) विष वाणिज्य - संखिया आदि तरह-तरह के विष जन्तु - हत्या से निकलवाने तथा उनका व्यापार करना, (११) यंत्र पीड़न कर्म – तिल, ईख आदि पेरने के यंत्र चलाना व चलवाना तथा उसका धंधा करना, (१२) निलछन कर्म - बैल, घोड़े आदि को नपुंसक बनाने का धंधा करना, (१३) दवाग्निदायक कर्म - जंगल आदि में आग लगाने या लगवाने का धंधा करना, (१४) सरोद्रह तड़ाग शोषण कर्म - झील, कुंड, तालाब आदि को सुखाने का धंधा करना एवं (१५) असतीजन पोषण कर्म – अपनी आजीविका चलाने के लिए दुष्चरित्र स्त्रियों, शिकारी प्राणियों आदि का पोषण करना । तब मैं नहीं समझता था कि अहिंसा में विश्वास रखने वाले एक साधक को ऐसे हिंसापूर्ण व्यवसाय नहीं अपनानी चाहिये। अपनी आजीविका मुझे अहिंसक उपायों तथा नैतिकता के साथ ही चलानी चाहिये— यह भान मुझे बाद में उपजा । हिंसा-भरे व्यवसाय चलाते हुए भला कोई भी अहिंसा पालन की दिशा में आगे कैसे बढ़ सकता है ?
मैं अब जान गया हूँ कि ये सब कर्मादान पापों के द्वार हैं जिन्हें बन्द करके ही मैं अपनी अशुभता को घटा सकता हूँ तथा अपने मन, वचन एवं कर्म की शुभता को बढ़ा सकता हूँ। यह शुभता जब बढ़ती है तो मेरे आत्म प्रदेशों से अशुभ कर्मों का बंध ढीला होता है तथा शुभ कार्यों के बंध से पुण्य कर्मों का उपार्जन होता है। शुभता की निर्जरा के साथ कभी उस मनोदशा में लोकोपकारी कार्य करने की मेरी शक्ति भी संगठित बनती है एवं सत्कार्य करते रहने का मेरा संकल्प भी सुदृढ़ होता है । मन, वचन एवं काया के शुभ योगों के प्रवर्तन काल मैं पुण्य कार्य करने का अभिलाषी एवं समर्थ बनता हूँ। पुण्य रूप शुभ कर्मों का बंध नौ प्रकार से हो सकता है। मैं जरूरतमन्द और योग्य पात्र को भोजन के लिये अन्न दूं, दूध पानी वगेरा पीने की वस्तुएँ सुलभ करूँ, आवश्यक वस्त्र प्रदान करूं, ठहरने के लिए स्थान उपलब्ध कराऊं तथा बिछाने व सोने के लिए पाटला बिस्तर आदि दूं तो क्रमशः अन्न पुण्य, पान पुण्य, वस्त्र पुण्य, लयन पुण्य व शयन पुण्य रूप शुभ कर्म का मेरे बंध होगा। इसके सिवाय गुणियों को देखकर मन में प्रसन्नता का अनुभव वाणी के द्वारा योग्यों की प्रशंसा एवं शरीर से गुरुजनों की सेवा सुश्रूषा करने मन, वचन एवं काया पुण्य का अर्जन होता है। अन्तिम नौवां पुण्य कार्य माना गया है नमस्कार को कि मैं भाव भक्ति पूर्वक अपने पूज्य एवं गुरुजनों को नम्रता से वन्दन आदि करूं । ये पुण्योपार्जन के कारणभूत पवित्र कार्य
१०८