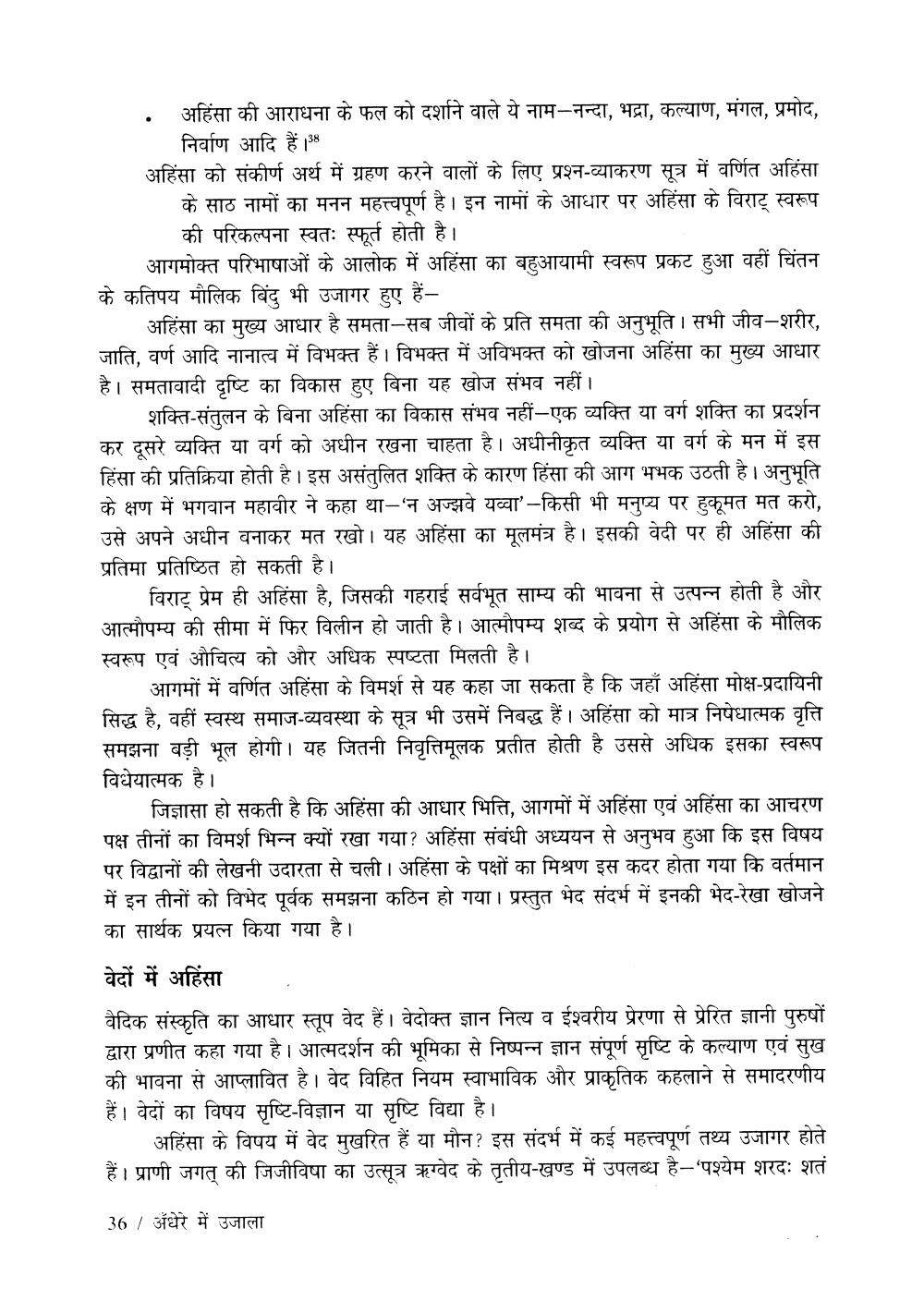________________
अहिंसा की आराधना के फल को दर्शाने वाले ये नाम - नन्दा, भद्रा, कल्याण, मंगल, प्रमोद, निर्वाण आदि हैं। 38
अहिंसा को संकीर्ण अर्थ में ग्रहण करने वालों के लिए प्रश्न- व्याकरण सूत्र में वर्णित अहिंसा
के साठ नामों का मनन महत्त्वपूर्ण है। इन नामों के आधार पर अहिंसा के विराट् स्वरूप की परिकल्पना स्वतः स्फूर्त होती है ।
आगमोक्त परिभाषाओं के आलोक में अहिंसा का बहुआयामी स्वरूप प्रकट हुआ वहीं चिंतन के कतिपय मौलिक बिंदु भी उजागर हुए हैं
अहिंसा का मुख्य आधार है समता - सब जीवों के प्रति समता की अनुभूति । सभी जीव- शरीर, जाति, वर्ण आदि नानात्व में विभक्त हैं । विभक्त में अविभक्त को खोजना अहिंसा का मुख्य आधार । समतावादी दृष्टि का विकास हुए बिना यह खोज संभव नहीं ।
शक्ति-संतुलन के बिना अहिंसा का विकास संभव नहीं - एक व्यक्ति या वर्ग शक्ति का प्रदर्शन कर दूसरे व्यक्ति या वर्ग को अधीन रखना चाहता है । अधीनीकृत व्यक्ति या वर्ग के मन में इस हिंसा की प्रतिक्रिया होती है। इस असंतुलित शक्ति के कारण हिंसा की आग भभक उठती है। अनुभूति केक्षण में भगवान महावीर ने कहा था- 'न अज्झवे यव्वा' - किसी भी मनुष्य पर हुकूमत मत करो, उसे अपने अधीन बनाकर मत रखो। यह अहिंसा का मूलमंत्र है। इसकी वेदी पर ही अहिंसा की प्रतिमा प्रतिष्ठित हो सकती है।
विराट् प्रेम ही अहिंसा है, जिसकी गहराई सर्वभूत साम्य की भावना से उत्पन्न होती है और आत्मौपम्य की सीमा में फिर विलीन हो जाती है । आत्मौपम्य शब्द के प्रयोग अहिंसा के मौलिक स्वरूप एवं औचित्य को और अधिक स्पष्टता मिलती है ।
आगमों में वर्णित अहिंसा के विमर्श से यह कहा जा सकता है कि जहाँ अहिंसा मोक्ष प्रदायिनी सिद्ध है, वहीं स्वस्थ समाज व्यवस्था के सूत्र भी उसमें निबद्ध हैं। अहिंसा को मात्र निषेधात्मक वृत्ति समझना बड़ी भूल होगी । यह जितनी निवृत्तिमूलक प्रतीत होती है उससे अधिक इसका स्वरूप विधेयात्मक है 1
जिज्ञासा हो सकती है कि अहिंसा की आधार भित्ति, आगमों में अहिंसा एवं अहिंसा का आचरण पक्ष तीनों का विमर्श भिन्न क्यों रखा गया ? अहिंसा संबंधी अध्ययन से अनुभव हुआ कि इस विषय पर विद्वानों की लेखनी उदारता से चली । अहिंसा के पक्षों का मिश्रण इस कदर होता गया कि वर्तमान में इन तीनों को विभेद पूर्वक समझना कठिन हो गया । प्रस्तुत भेद संदर्भ में इनकी भेद-रेखा खोजने का सार्थक प्रयत्न किया गया है।
वेदों में अहिंसा
वैदिक संस्कृति का आधार स्तूप वेद हैं। वेदोक्त ज्ञान नित्य व ईश्वरीय प्रेरणा से प्रेरित ज्ञानी पुरुषों द्वारा प्रणीत कहा गया है । आत्मदर्शन की भूमिका से निष्पन्न ज्ञान संपूर्ण सृष्टि के कल्याण एवं सुख की भावना से आप्लावित है । वेद विहित नियम स्वाभाविक और प्राकृतिक कहलाने से समादरणीय हैं। वेदों का विषय सृष्टि - विज्ञान या सृष्टि विद्या है।
अहिंसा के विषय में वेद मुखरित हैं या मौन ? इस संदर्भ में कई महत्त्वपूर्ण तथ्य उजागर होते हैं । प्राणी जगत् की जिजीविषा का उत्सूत्र ऋग्वेद के तृतीय खण्ड में उपलब्ध है - 'पश्येम शरदः शतं
36 / अँधेरे में उजाला