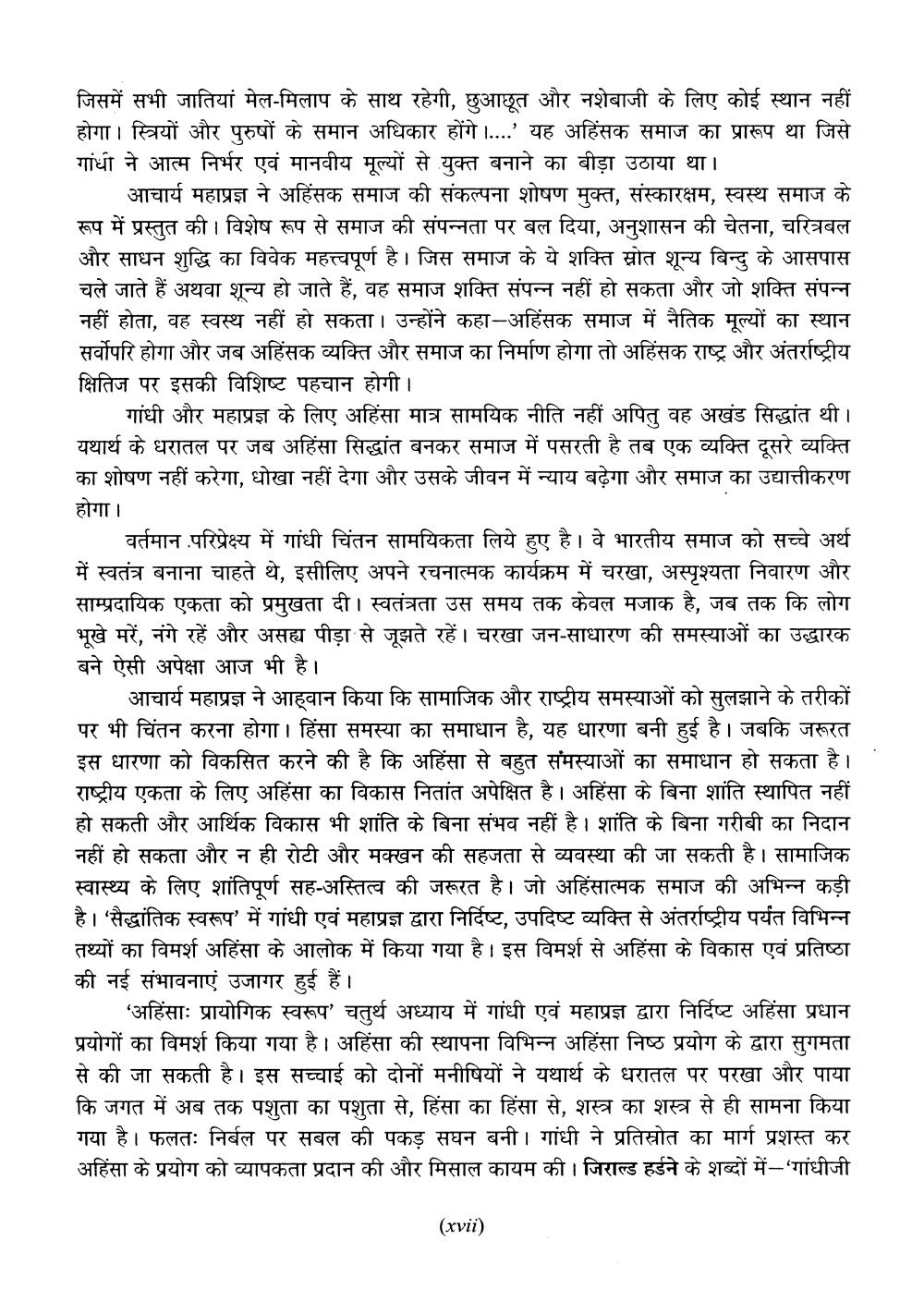________________
जिसमें सभी जातियां मेल-मिलाप के साथ रहेगी, छुआछूत और नशेबाजी के लिए कोई स्थान नहीं होगा। स्त्रियों और पुरुषों के समान अधिकार होंगे।....' यह अहिंसक समाज का प्रारूप था जिसे गांधी ने आत्म निर्भर एवं मानवीय मूल्यों से युक्त बनाने का बीड़ा उठाया था।
आचार्य महाप्रज्ञ ने अहिंसक समाज की संकल्पना शोषण मुक्त, संस्कारक्षम, स्वस्थ समाज के रूप में प्रस्तुत की। विशेष रूप से समाज की संपन्नता पर बल दिया, अनुशासन की चेतना, चरित्रबल और साधन शुद्धि का विवेक महत्त्वपूर्ण है। जिस समाज के ये शक्ति स्रोत शून्य बिन्दु के आसपास चले जाते हैं अथवा शून्य हो जाते हैं, वह समाज शक्ति संपन्न नहीं हो सकता और जो शक्ति संपन्न नहीं होता, वह स्वस्थ नहीं हो सकता। उन्होंने कहा-अहिंसक समाज में नैतिक मूल्यों का स्थान सर्वोपरि होगा और जब अहिंसक व्यक्ति और समाज का निर्माण होगा तो अहिंसक राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर इसकी विशिष्ट पहचान होगी।
गांधी और महाप्रज्ञ के लिए अहिंसा मात्र सामयिक नीति नहीं अपितु वह अखंड सिद्धांत थी। यथार्थ के धरातल पर जब अहिंसा सिद्धांत बनकर समाज में पसरती है तब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा, धोखा नहीं देगा और उसके जीवन में न्याय बढ़ेगा और समाज का उद्यात्तीकरण होगा।
__ वर्तमान परिप्रेक्ष्य में गांधी चिंतन सामयिकता लिये हुए है। वे भारतीय समाज को सच्चे अर्थ में स्वतंत्र बनाना चाहते थे, इसीलिए अपने रचनात्मक कार्यक्रम में चरखा, अस्पृश्यता निवारण और साम्प्रदायिक एकता को प्रमुखता दी। स्वतंत्रता उस समय तक केवल मजाक है, जब तक कि लोग भूखे मरें, नंगे रहें और असह्य पीड़ा से जूझते रहें। चरखा जन-साधारण की समस्याओं का उद्धारक बने ऐसी अपेक्षा आज भी है।
आचार्य महाप्रज्ञ ने आह्वान किया कि सामाजिक और राष्ट्रीय समस्याओं को सुलझाने के तरीकों पर भी चिंतन करना होगा। हिंसा समस्या का समाधान है, यह धारणा बनी हुई है। जबकि जरूरत इस धारणा को विकसित करने की है कि अहिंसा से बहुत समस्याओं का समाधान हो सकता है। राष्ट्रीय एकता के लिए अहिंसा का विकास नितांत अपेक्षित है। अहिंसा के बिना शांति स्थापित नहीं हो सकती और आर्थिक विकास भी शांति के बिना संभव नहीं है। शांति के बिना गरीबी का निदान नहीं हो सकता और न ही रोटी और मक्खन की सहजता से व्यवस्था की जा सकती है। सामाजिक स्वास्थ्य के लिए शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व की जरूरत है। जो अहिंसात्मक समाज की अभिन्न कड़ी है। ‘सैद्धांतिक स्वरूप' में गांधी एवं महाप्रज्ञ द्वारा निर्दिष्ट, उपदिष्ट व्यक्ति से अंतर्राष्ट्रीय पर्यंत विभिन्न तथ्यों का विमर्श अहिंसा के आलोक में किया गया है। इस विमर्श से अहिंसा के विकास एवं प्रतिष्ठा की नई संभावनाएं उजागर हुई हैं।
'अहिंसाः प्रायोगिक स्वरूप' चतुर्थ अध्याय में गांधी एवं महाप्रज्ञ द्वारा निर्दिष्ट अहिंसा प्रधान प्रयोगों का विमर्श किया गया है। अहिंसा की स्थापना विभिन्न अहिंसा निष्ठ प्रयोग के द्वारा सुगमता से की जा सकती है। इस सच्चाई को दोनों मनीषियों ने यथार्थ के धरातल पर परखा और पाया कि जगत में अब तक पशुता का पशुता से, हिंसा का हिंसा से, शस्त्र का शस्त्र से ही सामना किया गया है। फलतः निर्बल पर सबल की पकड़ सघन बनी। गांधी ने प्रतिस्रोत का मार्ग प्रशस्त कर अहिंसा के प्रयोग को व्यापकता प्रदान की और मिसाल कायम की। जिराल्ड हर्डने के शब्दों में-'गांधीजी
(xvii)