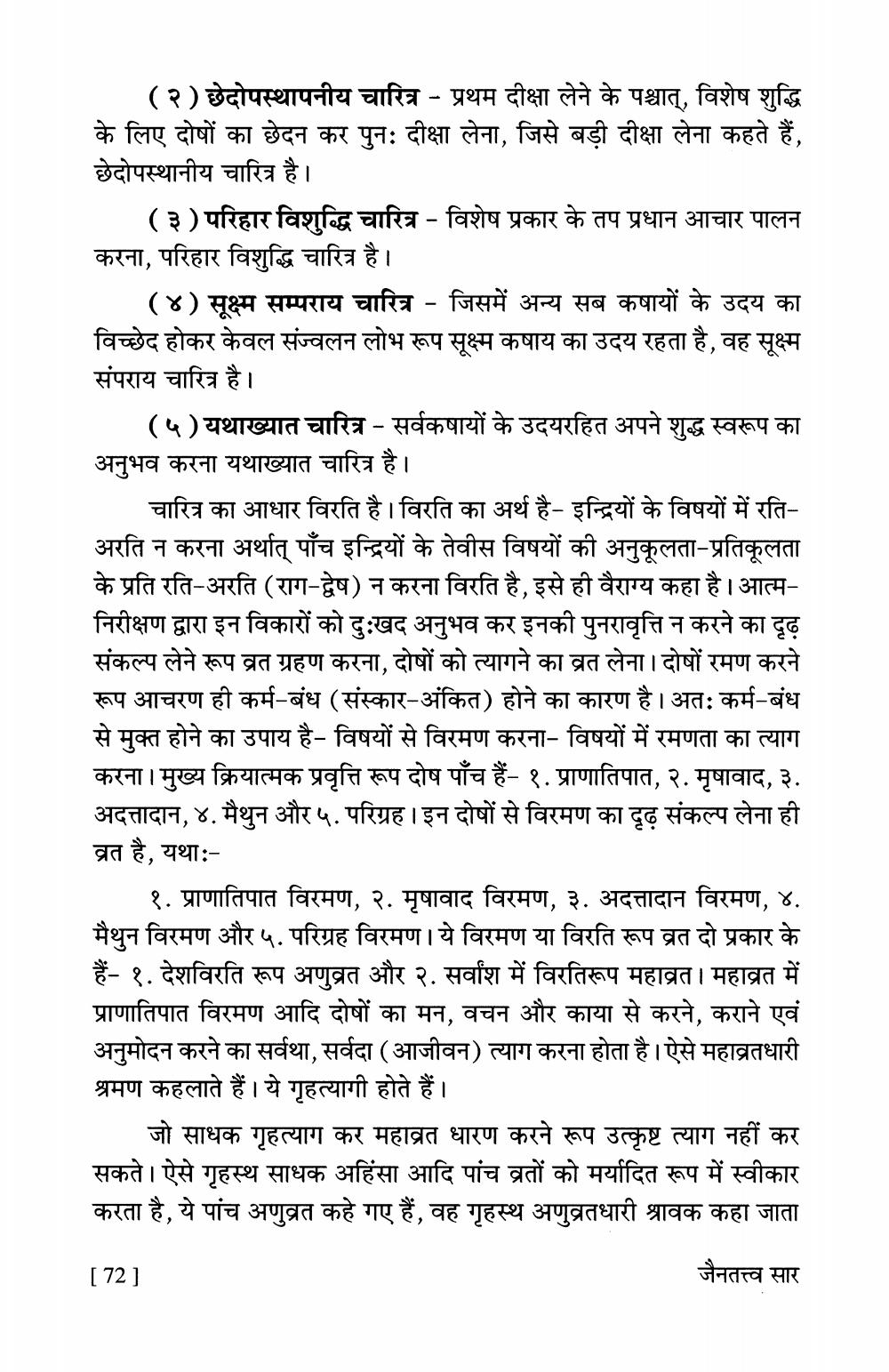________________
(२) छेदोपस्थापनीय चारित्र - प्रथम दीक्षा लेने के पश्चात्, विशेष शुद्धि के लिए दोषों का छेदन कर पुनः दीक्षा लेना, जिसे बड़ी दीक्षा लेना कहते हैं, छेदोपस्थानीय चारित्र है।
(३) परिहार विशुद्धि चारित्र - विशेष प्रकार के तप प्रधान आचार पालन करना, परिहार विशुद्धि चारित्र है।
(४) सूक्ष्म सम्पराय चारित्र - जिसमें अन्य सब कषायों के उदय का विच्छेद होकर केवल संज्वलन लोभ रूप सूक्ष्म कषाय का उदय रहता है, वह सूक्ष्म संपराय चारित्र है।
(५) यथाख्यात चारित्र - सर्वकषायों के उदयरहित अपने शुद्ध स्वरूप का अनुभव करना यथाख्यात चारित्र है।
चारित्र का आधार विरति है। विरति का अर्थ है- इन्द्रियों के विषयों में रतिअरति न करना अर्थात् पाँच इन्द्रियों के तेवीस विषयों की अनुकूलता-प्रतिकूलता के प्रति रति-अरति (राग-द्वेष) न करना विरति है, इसे ही वैराग्य कहा है। आत्मनिरीक्षण द्वारा इन विकारों को दुःखद अनुभव कर इनकी पुनरावृत्ति न करने का दृढ़ संकल्प लेने रूप व्रत ग्रहण करना, दोषों को त्यागने का व्रत लेना। दोषों रमण करने रूप आचरण ही कर्म-बंध (संस्कार-अंकित) होने का कारण है। अतः कर्म-बंध से मुक्त होने का उपाय है- विषयों से विरमण करना- विषयों में रमणता का त्याग करना। मुख्य क्रियात्मक प्रवृत्ति रूप दोष पाँच हैं- १. प्राणातिपात, २. मृषावाद, ३. अदत्तादान, ४. मैथुन और ५. परिग्रह । इन दोषों से विरमण का दृढ़ संकल्प लेना ही व्रत है, यथा:
१. प्राणातिपात विरमण, २. मृषावाद विरमण, ३. अदत्तादान विरमण, ४. मैथुन विरमण और ५. परिग्रह विरमण। ये विरमण या विरति रूप व्रत दो प्रकार के हैं- १. देशविरति रूप अणुव्रत और २. सर्वांश में विरतिरूप महाव्रत। महाव्रत में प्राणातिपात विरमण आदि दोषों का मन, वचन और काया से करने, कराने एवं अनुमोदन करने का सर्वथा, सर्वदा (आजीवन) त्याग करना होता है। ऐसे महाव्रतधारी श्रमण कहलाते हैं। ये गृहत्यागी होते हैं।
जो साधक गृहत्याग कर महाव्रत धारण करने रूप उत्कृष्ट त्याग नहीं कर सकते। ऐसे गृहस्थ साधक अहिंसा आदि पांच व्रतों को मर्यादित रूप में स्वीकार करता है, ये पांच अणुव्रत कहे गए हैं, वह गृहस्थ अणुव्रतधारी श्रावक कहा जाता
[72]
जैनतत्त्व सार