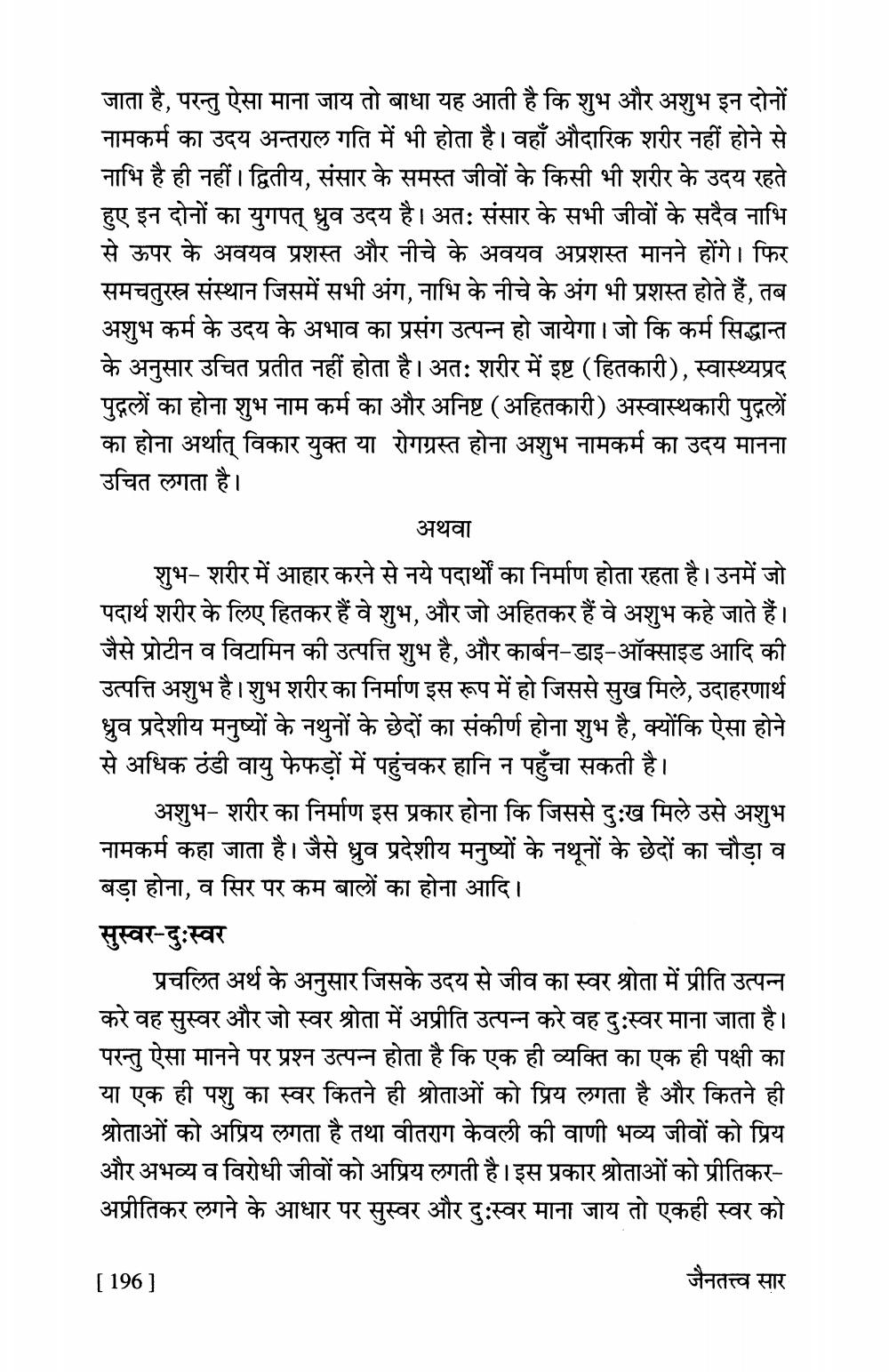________________
जाता है, परन्तु ऐसा माना जाय तो बाधा यह आती है कि शुभ और अशुभ इन दोनों नामकर्म का उदय अन्तराल गति में भी होता है। वहाँ औदारिक शरीर नहीं होने से नाभि है ही नहीं। द्वितीय, संसार के समस्त जीवों के किसी भी शरीर के उदय रहते हुए इन दोनों का युगपत् ध्रुव उदय है। अतः संसार के सभी जीवों के सदैव नाभि से ऊपर के अवयव प्रशस्त और नीचे के अवयव अप्रशस्त मानने होंगे। फिर समचतुरस्त्र संस्थान जिसमें सभी अंग, नाभि के नीचे के अंग भी प्रशस्त होते हैं, तब अशुभ कर्म के उदय के अभाव का प्रसंग उत्पन्न हो जायेगा। जो कि कर्म सिद्धान्त के अनुसार उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः शरीर में इष्ट (हितकारी), स्वास्थ्यप्रद पुद्गलों का होना शुभ नाम कर्म का और अनिष्ट (अहितकारी) अस्वास्थकारी पुद्गलों का होना अर्थात् विकार युक्त या रोगग्रस्त होना अशुभ नामकर्म का उदय मानना उचित लगता है।
अथवा
शुभ- शरीर में आहार करने से नये पदार्थों का निर्माण होता रहता है। उनमें जो पदार्थ शरीर के लिए हितकर हैं वे शुभ, और जो अहितकर हैं वे अशुभ कहे जाते हैं। जैसे प्रोटीन व विटामिन की उत्पत्ति शुभ है, और कार्बन-डाइ-ऑक्साइड आदि की उत्पत्ति अशुभ है। शुभ शरीर का निर्माण इस रूप में हो जिससे सुख मिले, उदाहरणार्थ ध्रुव प्रदेशीय मनुष्यों के नथुनों के छेदों का संकीर्ण होना शुभ है, क्योंकि ऐसा होने से अधिक ठंडी वायु फेफड़ों में पहुंचकर हानि न पहुँचा सकती है।
अशुभ- शरीर का निर्माण इस प्रकार होना कि जिससे दुःख मिले उसे अशुभ नामकर्म कहा जाता है। जैसे ध्रुव प्रदेशीय मनुष्यों के नथूनों के छेदों का चौड़ा व बड़ा होना, व सिर पर कम बालों का होना आदि। सुस्वर-दुःस्वर
प्रचलित अर्थ के अनुसार जिसके उदय से जीव का स्वर श्रोता में प्रीति उत्पन्न करे वह सुस्वर और जो स्वर श्रोता में अप्रीति उत्पन्न करे वह दुःस्वर माना जाता है। परन्तु ऐसा मानने पर प्रश्न उत्पन्न होता है कि एक ही व्यक्ति का एक ही पक्षी का या एक ही पशु का स्वर कितने ही श्रोताओं को प्रिय लगता है और कितने ही श्रोताओं को अप्रिय लगता है तथा वीतराग केवली की वाणी भव्य जीवों को प्रिय और अभव्य व विरोधी जीवों को अप्रिय लगती है। इस प्रकार श्रोताओं को प्रीतिकरअप्रीतिकर लगने के आधार पर सुस्वर और दुःस्वर माना जाय तो एकही स्वर को
[196]
जैनतत्त्व सार