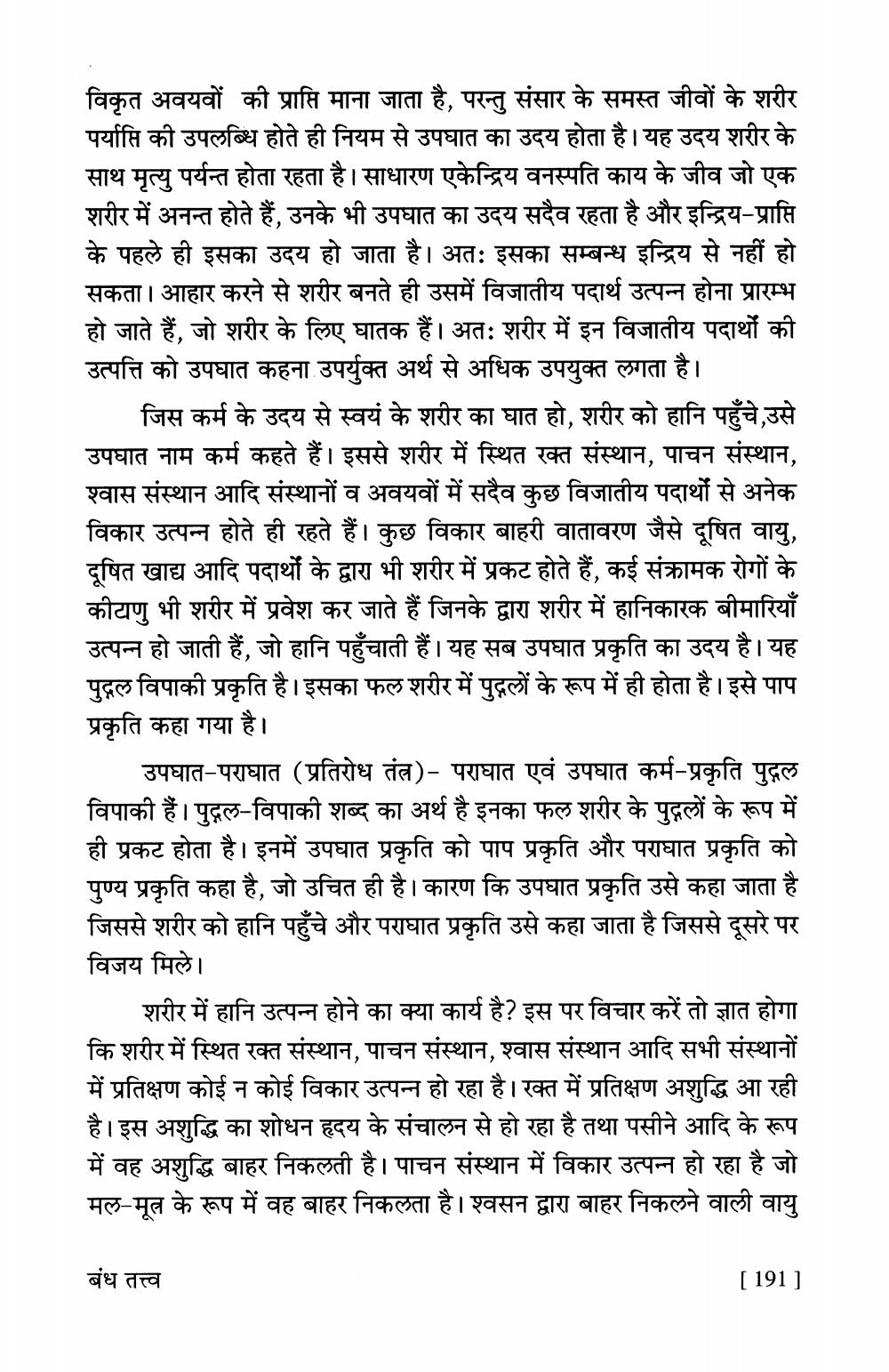________________
विकृत अवयवों की प्राप्ति माना जाता है, परन्तु संसार के समस्त जीवों के शरीर पर्याप्ति की उपलब्धि होते ही नियम से उपघात का उदय होता है। यह उदय शरीर के साथ मृत्यु पर्यन्त होता रहता है। साधारण एकेन्द्रिय वनस्पति काय के जीव जो एक शरीर में अनन्त होते हैं, उनके भी उपघात का उदय सदैव रहता है और इन्द्रिय-प्राप्ति के पहले ही इसका उदय हो जाता है। अतः इसका सम्बन्ध इन्द्रिय से नहीं हो सकता। आहार करने से शरीर बनते ही उसमें विजातीय पदार्थ उत्पन्न होना प्रारम्भ हो जाते हैं, जो शरीर के लिए घातक हैं। अतः शरीर में इन विजातीय पदार्थों की उत्पत्ति को उपघात कहना उपर्युक्त अर्थ से अधिक उपयुक्त लगता है।
_ जिस कर्म के उदय से स्वयं के शरीर का घात हो, शरीर को हानि पहुँचे,उसे उपघात नाम कर्म कहते हैं। इससे शरीर में स्थित रक्त संस्थान, पाचन संस्थान, श्वास संस्थान आदि संस्थानों व अवयवों में सदैव कुछ विजातीय पदार्थों से अनेक विकार उत्पन्न होते ही रहते हैं। कुछ विकार बाहरी वातावरण जैसे दूषित वायु, दूषित खाद्य आदि पदार्थों के द्वारा भी शरीर में प्रकट होते हैं, कई संक्रामक रोगों के कीटाणु भी शरीर में प्रवेश कर जाते हैं जिनके द्वारा शरीर में हानिकारक बीमारियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जो हानि पहुँचाती हैं। यह सब उपघात प्रकृति का उदय है। यह पुद्गल विपाकी प्रकृति है। इसका फल शरीर में पुद्गलों के रूप में ही होता है। इसे पाप प्रकृति कहा गया है।
उपघात-पराघात (प्रतिरोध तंत्र)- पराघात एवं उपघात कर्म-प्रकृति पुद्गल विपाकी हैं। पुद्गल-विपाकी शब्द का अर्थ है इनका फल शरीर के पुद्गलों के रूप में ही प्रकट होता है। इनमें उपघात प्रकृति को पाप प्रकृति और पराघात प्रकृति को पुण्य प्रकृति कहा है, जो उचित ही है। कारण कि उपघात प्रकृति उसे कहा जाता है जिससे शरीर को हानि पहुँचे और पराघात प्रकृति उसे कहा जाता है जिससे दूसरे पर विजय मिले।
शरीर में हानि उत्पन्न होने का क्या कार्य है? इस पर विचार करें तो ज्ञात होगा कि शरीर में स्थित रक्त संस्थान, पाचन संस्थान, श्वास संस्थान आदि सभी संस्थानों में प्रतिक्षण कोई न कोई विकार उत्पन्न हो रहा है। रक्त में प्रतिक्षण अशुद्धि आ रही है। इस अशुद्धि का शोधन हृदय के संचालन से हो रहा है तथा पसीने आदि के रूप में वह अशुद्धि बाहर निकलती है। पाचन संस्थान में विकार उत्पन्न हो रहा है जो मल-मूत्र के रूप में वह बाहर निकलता है। श्वसन द्वारा बाहर निकलने वाली वायु
बंध तत्त्व
[191]