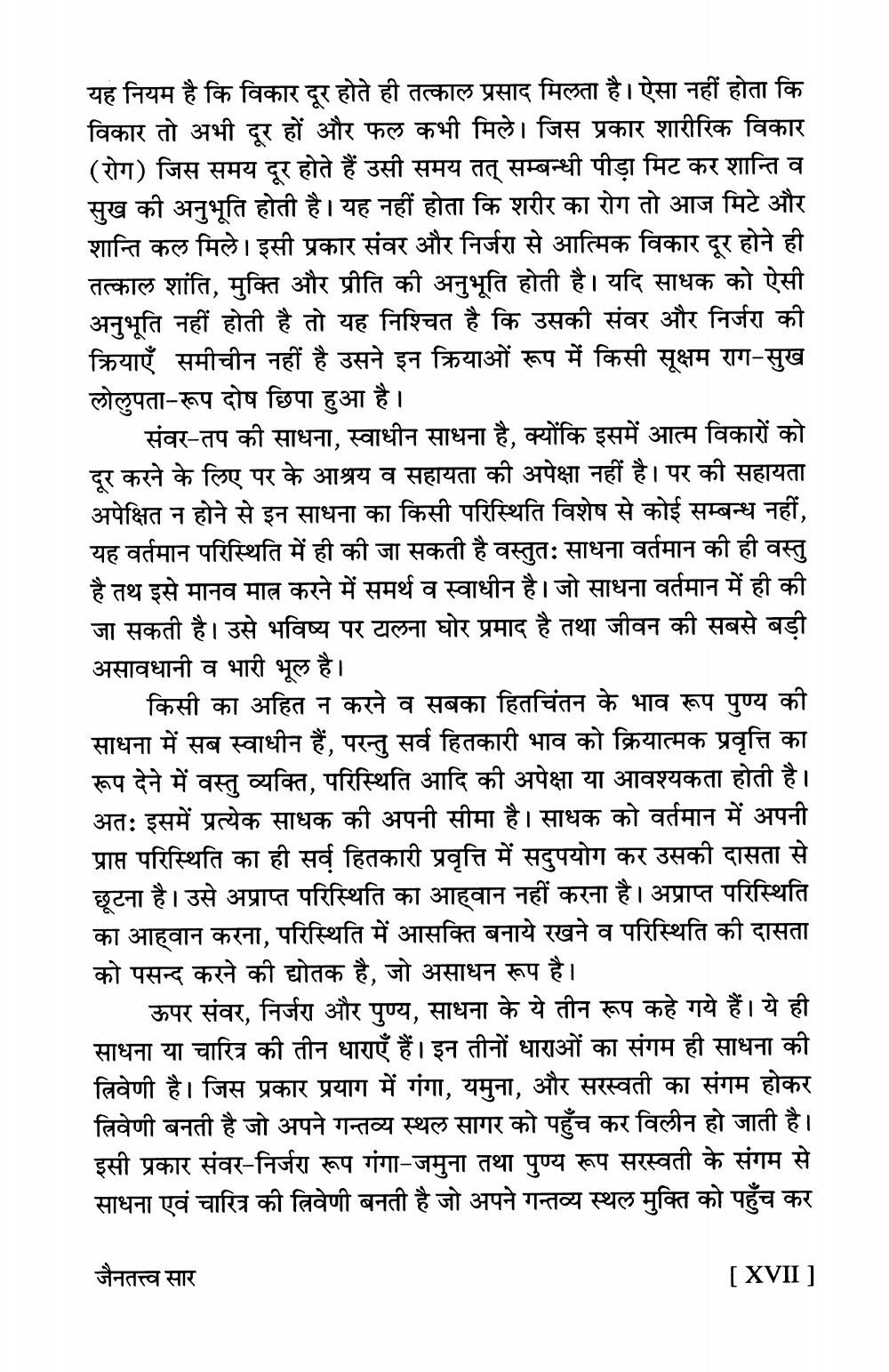________________
यह नियम है कि विकार दूर होते ही तत्काल प्रसाद मिलता है। ऐसा नहीं होता कि विकार तो अभी दूर हों और फल कभी मिले। जिस प्रकार शारीरिक विकार (रोग) जिस समय दूर होते हैं उसी समय तत् सम्बन्धी पीड़ा मिट कर शान्ति व सुख की अनुभूति होती है। यह नहीं होता कि शरीर का रोग तो आज मिटे और शान्ति कल मिले। इसी प्रकार संवर और निर्जरा से आत्मिक विकार दूर होने ही तत्काल शांति, मुक्ति और प्रीति की अनुभूति होती है। यदि साधक को ऐसी अनुभूति नहीं होती है तो यह निश्चित है कि उसकी संवर और निर्जरा की क्रियाएँ समीचीन नहीं है उसने इन क्रियाओं रूप में किसी सूक्षम राग-सुख लोलुपता-रूप दोष छिपा हुआ है।
संवर-तप की साधना, स्वाधीन साधना है, क्योंकि इसमें आत्म विकारों को दूर करने के लिए पर के आश्रय व सहायता की अपेक्षा नहीं है। पर की सहायता अपेक्षित न होने से इन साधना का किसी परिस्थिति विशेष से कोई सम्बन्ध नहीं, यह वर्तमान परिस्थिति में ही की जा सकती है वस्तुतः साधना वर्तमान की ही वस्तु है तथ इसे मानव मात्र करने में समर्थ व स्वाधीन है। जो साधना वर्तमान में ही की जा सकती है। उसे भविष्य पर टालना घोर प्रमाद है तथा जीवन की सबसे बड़ी असावधानी व भारी भूल है।
किसी का अहित न करने व सबका हितचिंतन के भाव रूप पुण्य की साधना में सब स्वाधीन हैं, परन्तु सर्व हितकारी भाव को क्रियात्मक प्रवृत्ति का रूप देने में वस्तु व्यक्ति, परिस्थिति आदि की अपेक्षा या आवश्यकता होती है। अतः इसमें प्रत्येक साधक की अपनी सीमा है। साधक को वर्तमान में अपनी प्राप्त परिस्थिति का ही सर्व हितकारी प्रवृत्ति में सदुपयोग कर उसकी दासता से छूटना है। उसे अप्राप्त परिस्थिति का आह्वान नहीं करना है। अप्राप्त परिस्थिति का आह्वान करना, परिस्थिति में आसक्ति बनाये रखने व परिस्थिति की दासता को पसन्द करने की द्योतक है, जो असाधन रूप है।
ऊपर संवर, निर्जरा और पुण्य, साधना के ये तीन रूप कहे गये हैं। ये ही साधना या चारित्र की तीन धाराएँ हैं। इन तीनों धाराओं का संगम ही साधना की त्रिवेणी है। जिस प्रकार प्रयाग में गंगा, यमुना, और सरस्वती का संगम होकर त्रिवेणी बनती है जो अपने गन्तव्य स्थल सागर को पहुँच कर विलीन हो जाती है। इसी प्रकार संवर-निर्जरा रूप गंगा-जमुना तथा पुण्य रूप सरस्वती के संगम से साधना एवं चारित्र की त्रिवेणी बनती है जो अपने गन्तव्य स्थल मुक्ति को पहुँच कर
जैनतत्त्व सार
[XVII]