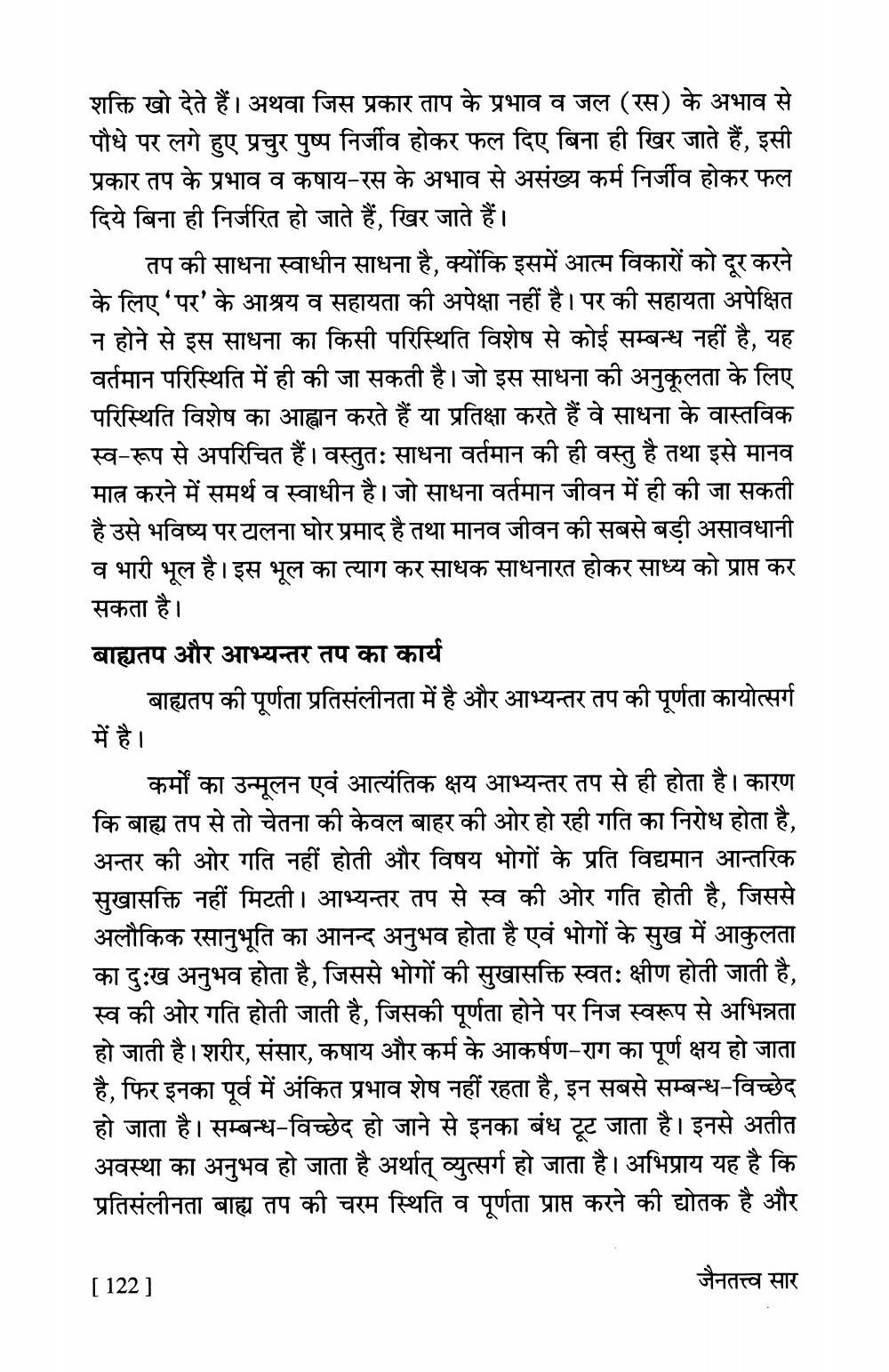________________
शक्ति खो देते हैं । अथवा जिस प्रकार ताप के प्रभाव व जल (रस) के अभाव से पौधे पर लगे हुए प्रचुर पुष्प निर्जीव होकर फल दिए बिना ही खिर जाते हैं, इसी प्रकार तप के प्रभाव व कषाय-रस के अभाव से असंख्य कर्म निर्जीव होकर फल दिये बिना ही निर्जरित हो जाते हैं, खिर जाते हैं ।
तप की साधना स्वाधीन साधना है, क्योंकि इसमें आत्म विकारों को दूर करने के लिए 'पर' के आश्रय व सहायता की अपेक्षा नहीं है । पर की सहायता अपेक्षित न होने से इस साधना का किसी परिस्थिति विशेष से कोई सम्बन्ध नहीं है, यह वर्तमान परिस्थिति में ही की जा सकती है। जो इस साधना की अनुकूलता के लिए परिस्थिति विशेष का आह्वान करते हैं या प्रतिक्षा करते हैं वे साधना के वास्तविक स्व-रूप से अपरिचित हैं । वस्तुतः साधना वर्तमान की ही वस्तु है तथा इसे मानव मात्र करने में समर्थ व स्वाधीन है। जो साधना वर्तमान जीवन में ही की जा सकती है उसे भविष्य पर टालना घोर प्रमाद है तथा मानव जीवन की सबसे बड़ी असावधानी भारी भूल है। इस भूल का त्याग कर साधक साधनारत होकर साध्य को प्राप्त कर सकता है।
बाह्यतप और आभ्यन्तर तप का कार्य
बाह्यतप की पूर्णता प्रतिसंलीनता में है और आभ्यन्तर तप की पूर्णता कायोत्सर्ग में है ।
कर्मों का उन्मूलन एवं आत्यंतिक क्षय आभ्यन्तर तप से ही होता है । कारण कि बाह्य तप से तो चेतना की केवल बाहर की ओर हो रही गति का निरोध होता है, अन्तर की ओर गति नहीं होती और विषय भोगों के प्रति विद्यमान आन्तरिक सुखासक्ति नहीं मिटती । आभ्यन्तर तप से स्व की ओर गति होती है, जिससे अलौकिक रसानुभूति का आनन्द अनुभव होता है एवं भोगों के सुख में आकुलता का दु:ख अनुभव होता है, जिससे भोगों की सुखासक्ति स्वत: क्षीण होती जाती है, स्व की ओर गति होती जाती है, जिसकी पूर्णता होने पर निज स्वरूप से अभिन्नता हो जाती है। शरीर, संसार, कषाय और कर्म के आकर्षण - राग का पूर्ण क्षय हो जाता है, फिर इनका पूर्व में अंकित प्रभाव शेष नहीं रहता है, इन सबसे सम्बन्ध-विच्छेद हो जाता है । सम्बन्ध-विच्छेद हो जाने से इनका बंध टूट जाता है। इनसे अतीत अवस्था का अनुभव हो जाता है अर्थात् व्युत्सर्ग हो जाता है। अभिप्राय यह है कि प्रतिसंलीनता बाह्य तप की चरम स्थिति व पूर्णता प्राप्त करने की द्योतक है और
[122]
जैनतत्त्व सा