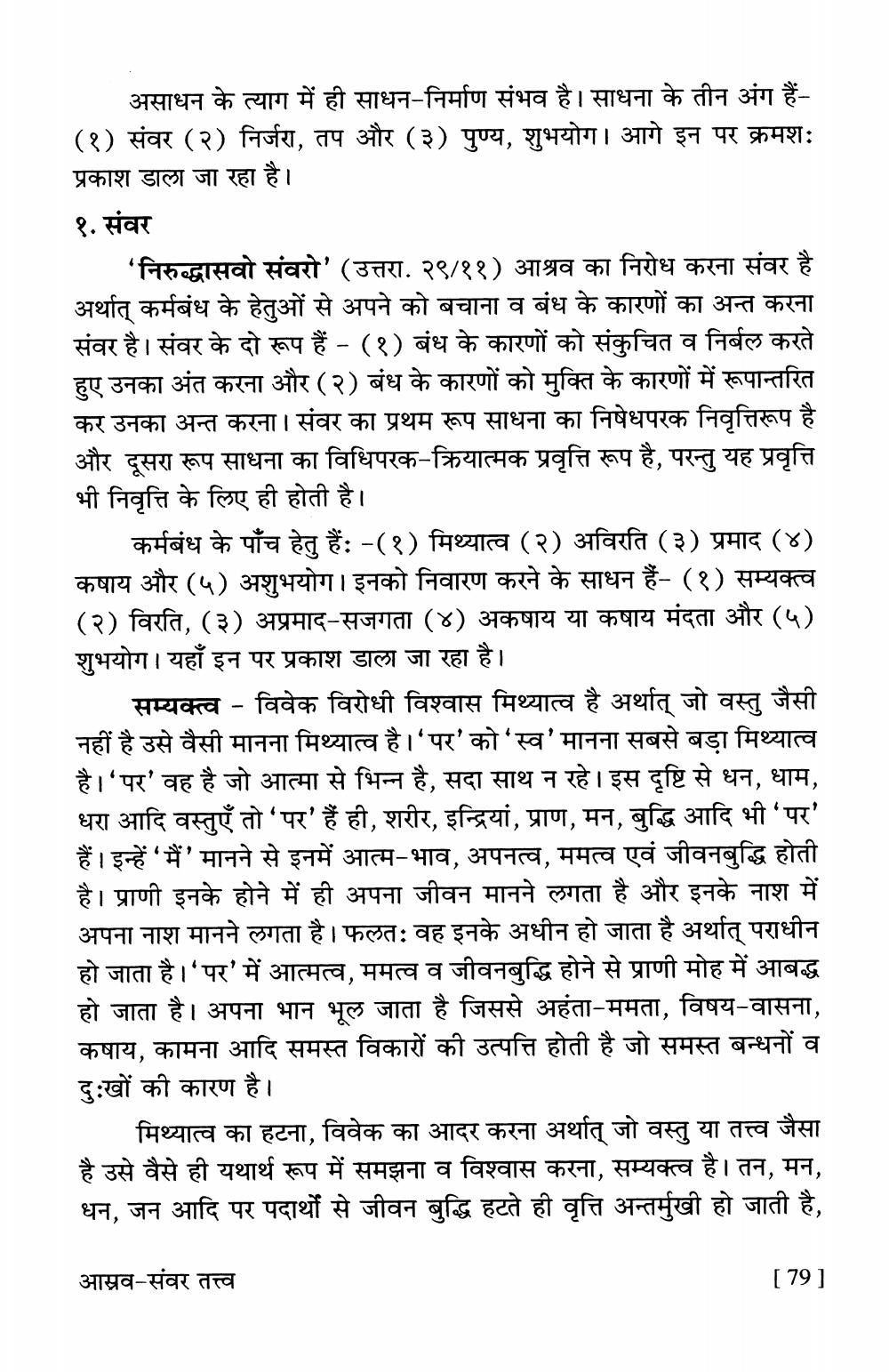________________
असाधन के त्याग में ही साधन-निर्माण संभव है। साधना के तीन अंग हैं(१) संवर (२) निर्जरा, तप और (३) पुण्य, शुभयोग। आगे इन पर क्रमशः प्रकाश डाला जा रहा है। १. संवर
"निरुद्धासवो संवरो' (उत्तरा. २९/११) आश्रव का निरोध करना संवर है अर्थात् कर्मबंध के हेतुओं से अपने को बचाना व बंध के कारणों का अन्त करना संवर है। संवर के दो रूप हैं - (१) बंध के कारणों को संकुचित व निर्बल करते हुए उनका अंत करना और (२) बंध के कारणों को मुक्ति के कारणों में रूपान्तरित कर उनका अन्त करना। संवर का प्रथम रूप साधना का निषेधपरक निवृत्तिरूप है और दूसरा रूप साधना का विधिपरक-क्रियात्मक प्रवृत्ति रूप है, परन्तु यह प्रवृत्ति भी निवृत्ति के लिए ही होती है।
कर्मबंध के पाँच हेतु हैं: -(१) मिथ्यात्व (२) अविरति (३) प्रमाद (४) कषाय और (५) अशुभयोग। इनको निवारण करने के साधन हैं- (१) सम्यक्त्व (२) विरति, (३) अप्रमाद-सजगता (४) अकषाय या कषाय मंदता और (५) शुभयोग। यहाँ इन पर प्रकाश डाला जा रहा है।
सम्यक्त्व - विवेक विरोधी विश्वास मिथ्यात्व है अर्थात् जो वस्तु जैसी नहीं है उसे वैसी मानना मिथ्यात्व है। 'पर' को 'स्व' मानना सबसे बड़ा मिथ्यात्व है। 'पर' वह है जो आत्मा से भिन्न है, सदा साथ न रहे। इस दृष्टि से धन, धाम, धरा आदि वस्तुएँ तो 'पर' हैं ही, शरीर, इन्द्रियां, प्राण, मन, बुद्धि आदि भी 'पर' हैं। इन्हें 'मैं' मानने से इनमें आत्म-भाव, अपनत्व, ममत्व एवं जीवनबुद्धि होती है। प्राणी इनके होने में ही अपना जीवन मानने लगता है और इनके नाश में अपना नाश मानने लगता है। फलतः वह इनके अधीन हो जाता है अर्थात् पराधीन हो जाता है। 'पर' में आत्मत्व, ममत्व व जीवनबुद्धि होने से प्राणी मोह में आबद्ध हो जाता है। अपना भान भूल जाता है जिससे अहंता-ममता, विषय-वासना, कषाय, कामना आदि समस्त विकारों की उत्पत्ति होती है जो समस्त बन्धनों व दु:खों की कारण है।
मिथ्यात्व का हटना, विवेक का आदर करना अर्थात् जो वस्तु या तत्त्व जैसा है उसे वैसे ही यथार्थ रूप में समझना व विश्वास करना, सम्यक्त्व है। तन, मन, धन, जन आदि पर पदार्थों से जीवन बुद्धि हटते ही वृत्ति अन्तर्मुखी हो जाती है,
आस्रव-संवर तत्त्व
[79]