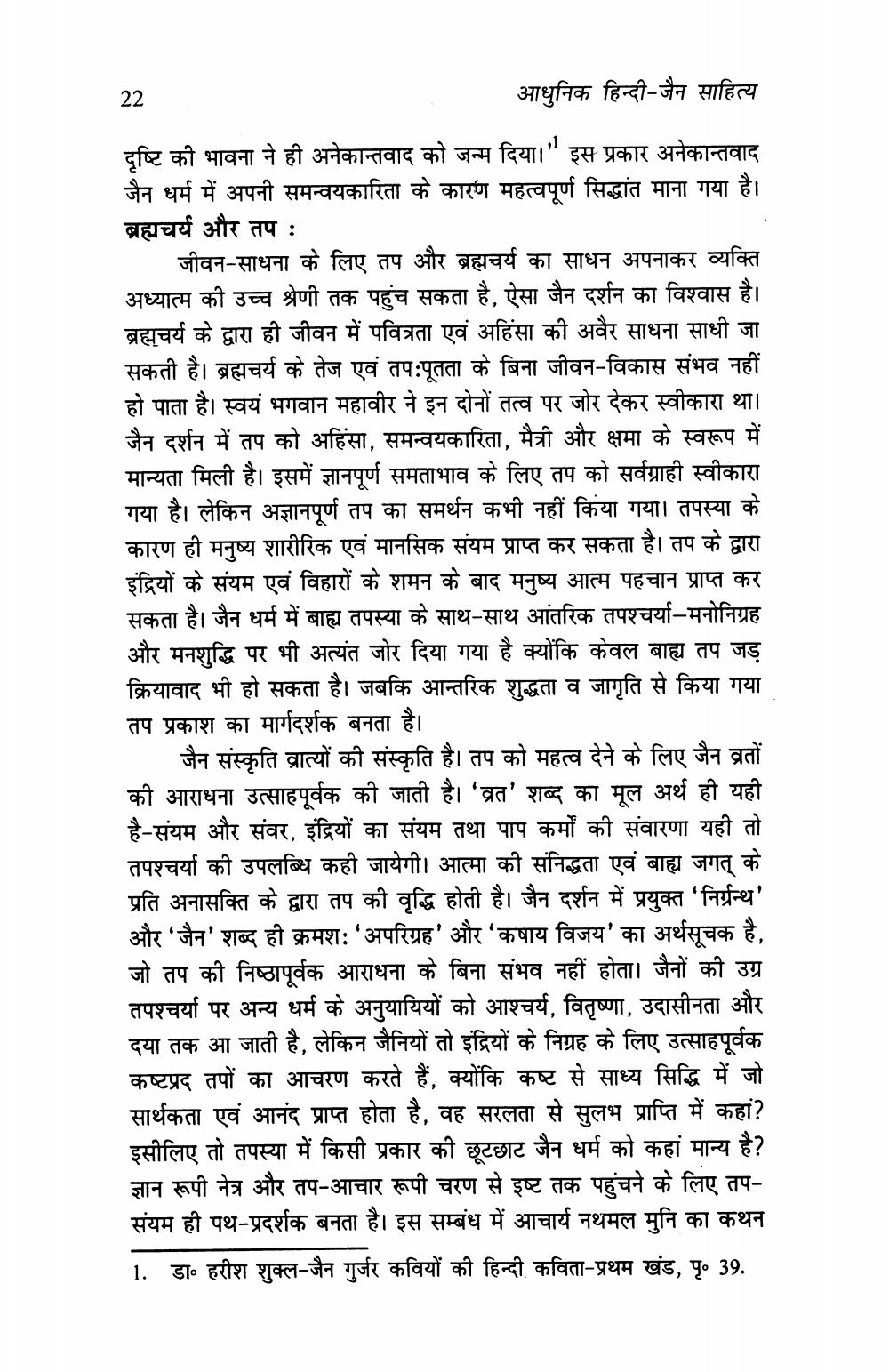________________
आधुनिक हिन्दी-जैन साहित्य
दृष्टि की भावना ने ही अनेकान्तवाद को जन्म दिया।" इस प्रकार अनेकान्तवाद जैन धर्म में अपनी समन्वयकारिता के कारण महत्वपूर्ण सिद्धांत माना गया है। ब्रह्मचर्य और तप :
जीवन-साधना के लिए तप और ब्रह्मचर्य का साधन अपनाकर व्यक्ति अध्यात्म की उच्च श्रेणी तक पहुंच सकता है, ऐसा जैन दर्शन का विश्वास है। ब्रह्मचर्य के द्वारा ही जीवन में पवित्रता एवं अहिंसा की अवैर साधना साधी जा सकती है। ब्रह्मचर्य के तेज एवं तपःपूतता के बिना जीवन-विकास संभव नहीं हो पाता है। स्वयं भगवान महावीर ने इन दोनों तत्व पर जोर देकर स्वीकारा था। जैन दर्शन में तप को अहिंसा, समन्वयकारिता, मैत्री और क्षमा के स्वरूप में मान्यता मिली है। इसमें ज्ञानपूर्ण समताभाव के लिए तप को सर्वग्राही स्वीकारा गया है। लेकिन अज्ञानपूर्ण तप का समर्थन कभी नहीं किया गया। तपस्या के कारण ही मनुष्य शारीरिक एवं मानसिक संयम प्राप्त कर सकता है। तप के द्वारा इंद्रियों के संयम एवं विहारों के शमन के बाद मनुष्य आत्म पहचान प्राप्त कर सकता है। जैन धर्म में बाह्य तपस्या के साथ-साथ आंतरिक तपश्चर्या-मनोनिग्रह
और मनशुद्धि पर भी अत्यंत जोर दिया गया है क्योंकि केवल बाह्य तप जड़ क्रियावाद भी हो सकता है। जबकि आन्तरिक शुद्धता व जागृति से किया गया तप प्रकाश का मार्गदर्शक बनता है।
जैन संस्कृति व्रात्यों की संस्कृति है। तप को महत्व देने के लिए जैन व्रतों की आराधना उत्साहपूर्वक की जाती है। 'व्रत' शब्द का मूल अर्थ ही यही है-संयम और संवर, इंद्रियों का संयम तथा पाप कर्मों की संवारणा यही तो तपश्चर्या की उपलब्धि कही जायेगी। आत्मा की संनिद्धता एवं बाह्य जगत् के प्रति अनासक्ति के द्वारा तप की वृद्धि होती है। जैन दर्शन में प्रयुक्त 'निर्ग्रन्थ'
और 'जैन' शब्द ही क्रमशः 'अपरिग्रह' और 'कषाय विजय' का अर्थसूचक है, जो तप की निष्ठापूर्वक आराधना के बिना संभव नहीं होता। जैनों की उग्र तपश्चर्या पर अन्य धर्म के अनुयायियों को आश्चर्य, वितृष्णा, उदासीनता और दया तक आ जाती है, लेकिन जैनियों तो इंद्रियों के निग्रह के लिए उत्साहपूर्वक कष्टप्रद तपों का आचरण करते हैं, क्योंकि कष्ट से साध्य सिद्धि में जो सार्थकता एवं आनंद प्राप्त होता है, वह सरलता से सुलभ प्राप्ति में कहां? इसीलिए तो तपस्या में किसी प्रकार की छूटछाट जैन धर्म को कहां मान्य है? ज्ञान रूपी नेत्र और तप-आचार रूपी चरण से इष्ट तक पहुंचने के लिए तपसंयम ही पथ-प्रदर्शक बनता है। इस सम्बंध में आचार्य नथमल मुनि का कथन 1. डा. हरीश शुक्ल-जैन गुर्जर कवियों की हिन्दी कविता-प्रथम खंड, पृ. 39.