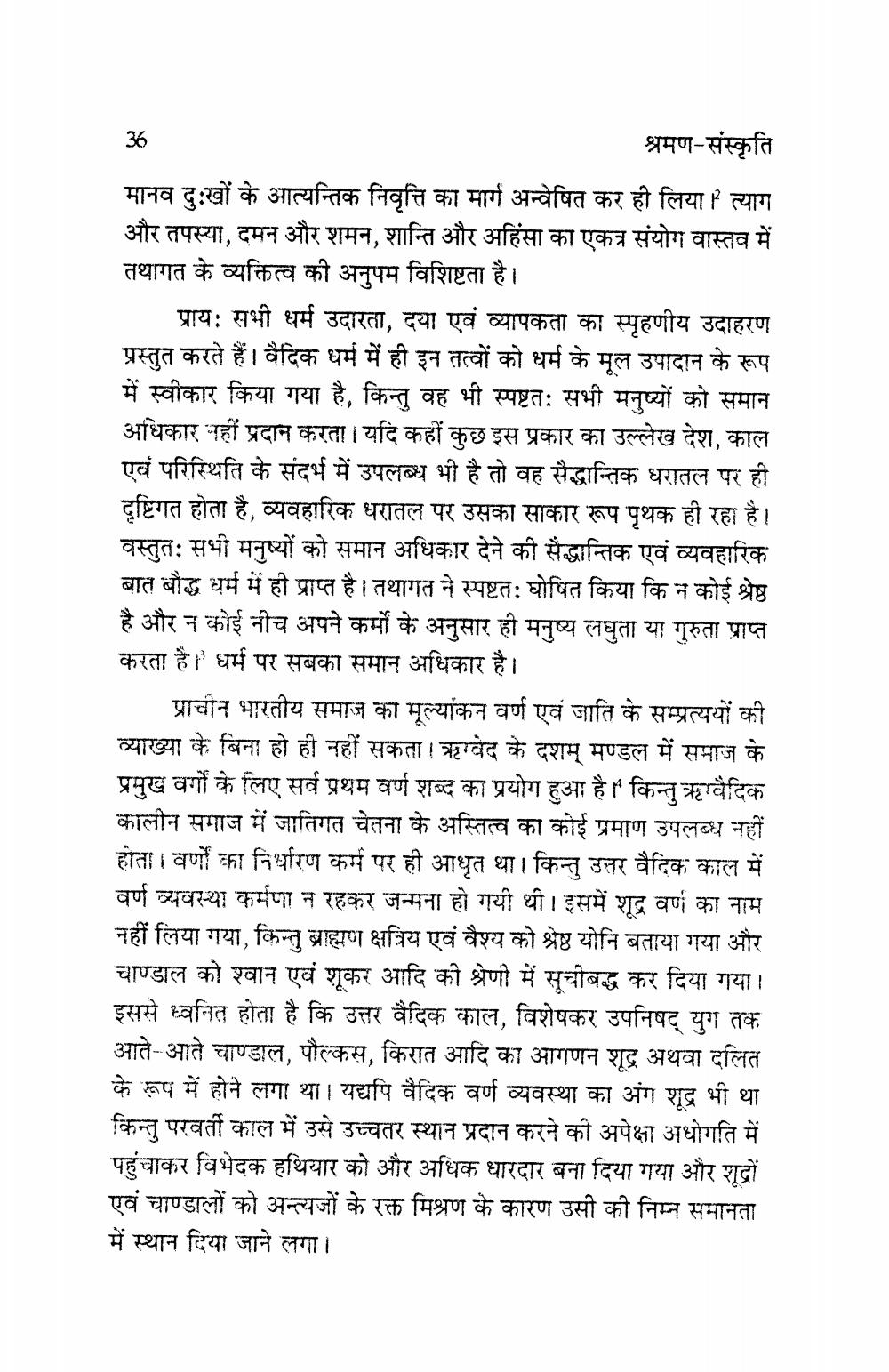________________
6
श्रमण-संस्कृति मानव दुःखों के आत्यन्तिक निवृत्ति का मार्ग अन्वेषित कर ही लिया। त्याग
और तपस्या, दमन और शमन, शान्ति और अहिंसा का एकत्र संयोग वास्तव में तथागत के व्यक्तित्व की अनुपम विशिष्टता है।
प्रायः सभी धर्म उदारता, दया एवं व्यापकता का स्पृहणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वैदिक धर्म में ही इन तत्वों को धर्म के मूल उपादान के रूप में स्वीकार किया गया है, किन्तु वह भी स्पष्टतः सभी मनुष्यों को समान अधिकार नहीं प्रदान करता। यदि कहीं कुछ इस प्रकार का उल्लेख देश, काल एवं परिस्थिति के संदर्भ में उपलब्ध भी है तो वह सैद्धान्तिक धरातल पर ही दृष्टिगत होता है, व्यवहारिक धरातल पर उसका साकार रूप पृथक ही रहा है। वस्तुतः सभी मनुष्यों को समान अधिकार देने की सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक बात बौद्ध धर्म में ही प्राप्त है। तथागत ने स्पष्टतः घोषित किया कि न कोई श्रेष्ठ है और न कोई नीच अपने कर्मों के अनुसार ही मनुष्य लघुता या गुरुता प्राप्त करता है। धर्म पर सबका समान अधिकार है।
प्राचीन भारतीय समाज का मूल्यांकन वर्ण एवं जाति के सम्प्रत्ययों की व्याख्या के बिना हो ही नहीं सकता। ऋग्वेद के दशम् मण्डल में समाज के प्रमुख वर्गों के लिए सर्व प्रथम वर्ण शब्द का प्रयोग हुआ है। किन्तु ऋावैदिक कालीन समाज में जातिगत चेतना के अस्तित्व का कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं होता। वर्गों का निर्धारण कर्म पर ही आधृत था। किन्तु उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्मणा न रहकर जन्मना हो गयी थी। इसमें शूद्र वर्ण का नाम नहीं लिया गया, किन्तु ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य को श्रेष्ठ योनि बताया गया और चाण्डाल को श्वान एवं शूकर आदि की श्रेणी में सूचीबद्ध कर दिया गया। इससे ध्वनित होता है कि उत्तर वैदिक काल, विशेषकर उपनिषद् युग तक आते-आते चाण्डाल, पौल्कस, किरात आदि का आगणन शूद्र अथवा दलित के रूप में होने लगा था। यद्यपि वैदिक वर्ण व्यवस्था का अंग शूद्र भी था किन्तु परवर्ती काल में उसे उच्चतर स्थान प्रदान करने की अपेक्षा अधोगति में पहुंचाकर विभेदक हथियार को और अधिक धारदार बना दिया गया और शूद्रों एवं चाण्डालों को अन्त्यजों के रक्त मिश्रण के कारण उसी की निम्न समानता में स्थान दिया जाने लगा।