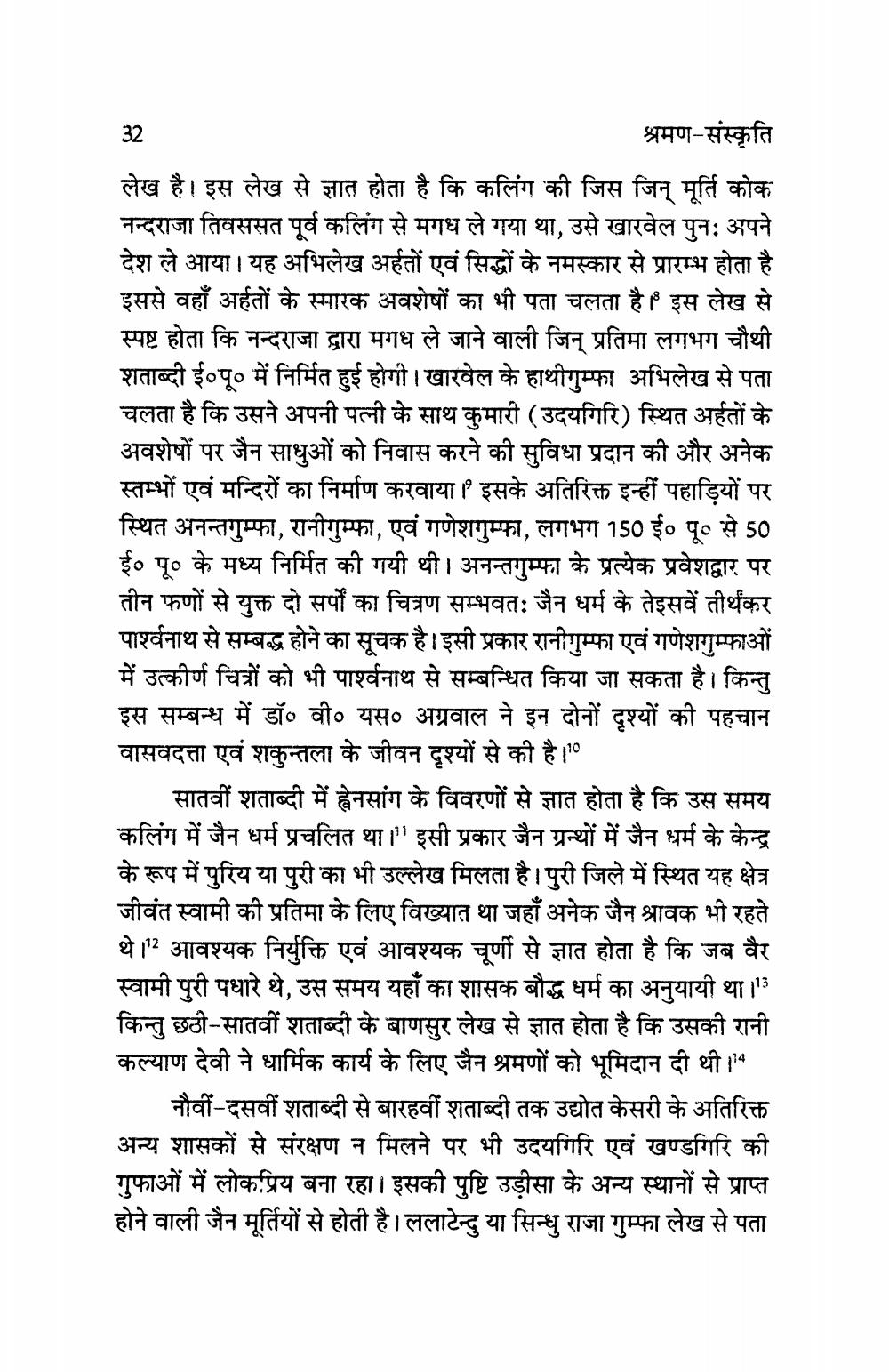________________
श्रमण-संस्कृति लेख है। इस लेख से ज्ञात होता है कि कलिंग की जिस जिन् मूर्ति कोक नन्दराजा तिवससत पूर्व कलिंग से मगध ले गया था, उसे खारवेल पुनः अपने देश ले आया। यह अभिलेख अर्हतों एवं सिद्धों के नमस्कार से प्रारम्भ होता है इससे वहाँ अर्हतों के स्मारक अवशेषों का भी पता चलता है। इस लेख से स्पष्ट होता कि नन्दराजा द्वारा मगध ले जाने वाली जिन प्रतिमा लगभग चौथी शताब्दी ई०पू० में निर्मित हुई होगी। खारवेल के हाथीगुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि उसने अपनी पत्नी के साथ कुमारी (उदयगिरि) स्थित अर्हतों के अवशेषों पर जैन साधुओं को निवास करने की सुविधा प्रदान की और अनेक स्तम्भों एवं मन्दिरों का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त इन्हीं पहाड़ियों पर स्थित अनन्तगुम्फा, रानीगुम्फा, एवं गणेशगुम्फा, लगभग 150 ई० पू० से 50 ई० पू० के मध्य निर्मित की गयी थी। अनन्तगुम्फा के प्रत्येक प्रवेशद्वार पर तीन फणों से युक्त दो सौ का चित्रण सम्भवतः जैन धर्म के तेइसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ से सम्बद्ध होने का सूचक है। इसी प्रकार रानीगुम्फा एवं गणेशगुम्फाओं में उत्कीर्ण चित्रों को भी पार्श्वनाथ से सम्बन्धित किया जा सकता है। किन्तु इस सम्बन्ध में डॉ० वी० यस० अग्रवाल ने इन दोनों दृश्यों की पहचान वासवदत्ता एवं शकुन्तला के जीवन दृश्यों से की है।"
सातवीं शताब्दी में ह्वेनसांग के विवरणों से ज्ञात होता है कि उस समय कलिंग में जैन धर्म प्रचलित था।" इसी प्रकार जैन ग्रन्थों में जैन धर्म के केन्द्र के रूप में पुरिय या पुरी का भी उल्लेख मिलता है। पुरी जिले में स्थित यह क्षेत्र जीवंत स्वामी की प्रतिमा के लिए विख्यात था जहाँ अनेक जैन श्रावक भी रहते थे। आवश्यक नियुक्ति एवं आवश्यक चूर्णी से ज्ञात होता है कि जब वैर स्वामी पुरी पधारे थे, उस समय यहाँ का शासक बौद्ध धर्म का अनुयायी था। किन्तु छठी-सातवीं शताब्दी के बाणसुर लेख से ज्ञात होता है कि उसकी रानी कल्याण देवी ने धार्मिक कार्य के लिए जैन श्रमणों को भूमिदान दी थी।
नौवीं-दसवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक उद्योत केसरी के अतिरिक्त अन्य शासकों से संरक्षण न मिलने पर भी उदयगिरि एवं खण्डगिरि की गुफाओं में लोकप्रिय बना रहा। इसकी पुष्टि उड़ीसा के अन्य स्थानों से प्राप्त होने वाली जैन मूर्तियों से होती है। ललाटेन्दु या सिन्धु राजा गुम्फा लेख से पता