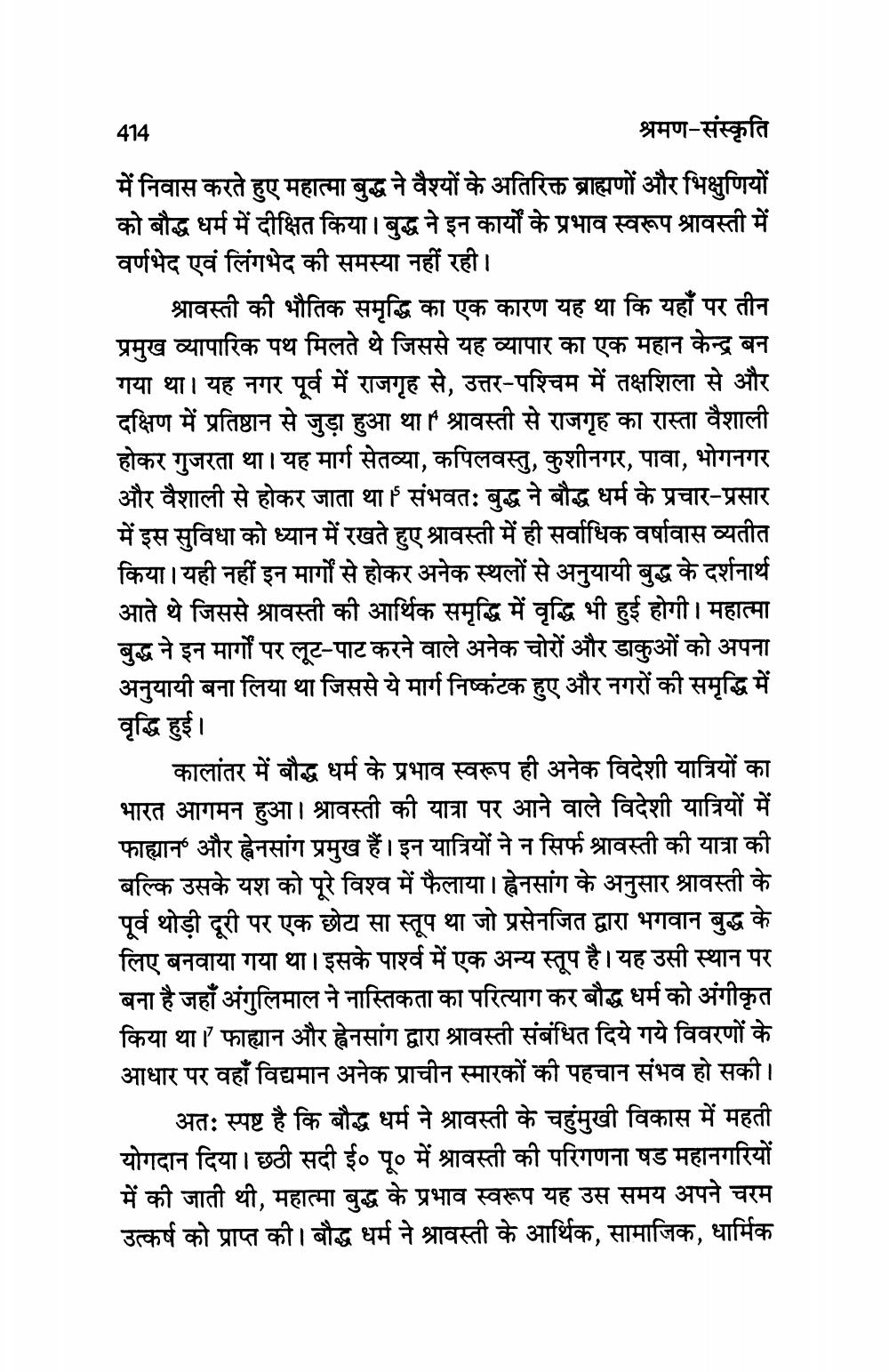________________
414
श्रमण-संस्कृति
में निवास करते हुए महात्मा बुद्ध ने वैश्यों के अतिरिक्त ब्राह्मणों और भिक्षुणियों को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया। बुद्ध ने इन कार्यों के प्रभाव स्वरूप श्रावस्ती में वर्णभेद एवं लिंगभेद की समस्या नहीं रही ।
श्रावस्ती की भौतिक समृद्धि का एक कारण यह था कि यहाँ पर तीन प्रमुख व्यापारिक पथ मिलते थे जिससे यह व्यापार का एक महान केन्द्र बन गया था। यह नगर पूर्व में राजगृह से, उत्तर-पश्चिम में तक्षशिला से और दक्षिण में प्रतिष्ठान से जुड़ा हुआ था । श्रावस्ती से राजगृह का रास्ता वैशाली होकर गुजरता था । यह मार्ग सेतव्या, कपिलवस्तु, कुशीनगर, पावा, भोगनगर और वैशाली से होकर जाता था । संभवतः बुद्ध ने बौद्ध धर्म के प्रचार-प्रसार
इस सुविधा को ध्यान में रखते हुए श्रावस्ती में ही सर्वाधिक वर्षावास व्यतीत किया। यही नहीं इन मार्गों से होकर अनेक स्थलों से अनुयायी बुद्ध के दर्शनार्थ आते थे जिससे श्रावस्ती की आर्थिक समृद्धि में वृद्धि भी हुई होगी। महात्मा बुद्ध ने इन मार्गों पर लूट-पाट करने वाले अनेक चोरों और डाकुओं को अपना अनुयायी बना लिया था जिससे ये मार्ग निष्कंटक हुए और नगरों की समृद्धि में वृद्धि हुई ।
कालांतर में बौद्ध धर्म के प्रभाव स्वरूप ही अनेक विदेशी यात्रियों का भारत आगमन हुआ । श्रावस्ती की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्रियों में फाह्यान' और ह्वेनसांग प्रमुख हैं। इन यात्रियों ने न सिर्फ श्रावस्ती की यात्रा की बल्कि उसके यश को पूरे विश्व में फैलाया । ह्वेनसांग के अनुसार श्रावस्ती के पूर्व थोड़ी दूरी पर एक छोटा सा स्तूप था जो प्रसेनजित द्वारा भगवान बुद्ध के लिए बनवाया गया था। इसके पार्श्व में एक अन्य स्तूप है। यह उसी स्थान पर बना है जहाँ अंगुलिमाल ने नास्तिकता का परित्याग कर बौद्ध धर्म को अंगीकृत किया था। फाह्यान और ह्वेनसांग द्वारा श्रावस्ती संबंधित दिये गये विवरणों के आधार पर वहाँ विद्यमान अनेक प्राचीन स्मारकों की पहचान संभव हो सकी।
अतः स्पष्ट है कि बौद्ध धर्म ने श्रावस्ती के चहुंमुखी विकास में महती योगदान दिया । छठी सदी ई० पू० में श्रावस्ती की परिगणना षड महानगरियों में की जाती थी, महात्मा बुद्ध के प्रभाव स्वरूप यह उस समय अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त की। बौद्ध धर्म ने श्रावस्ती के आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक