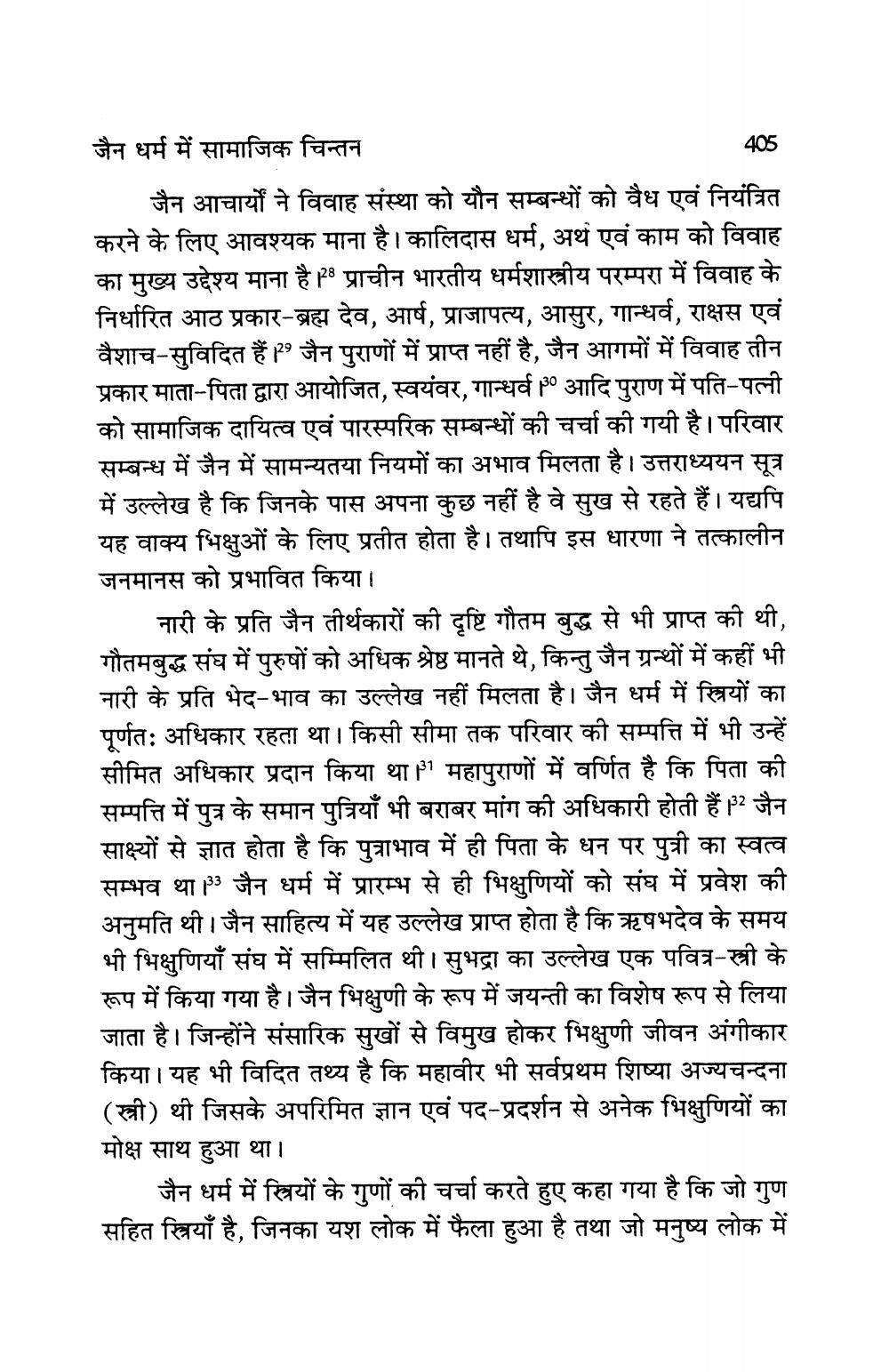________________
405
जैन धर्म में सामाजिक चिन्तन
जैन आचार्यों ने विवाह संस्था को यौन सम्बन्धों को वैध एवं नियंत्रित करने के लिए आवश्यक माना है। कालिदास धर्म, अर्थ एवं काम को विवाह का मुख्य उद्देश्य माना है। प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रीय परम्परा में विवाह के निर्धारित आठ प्रकार-ब्रह्म देव, आर्ष, प्राजापत्य, आसुर, गान्धर्व, राक्षस एवं वैशाच-सुविदित हैं। जैन पुराणों में प्राप्त नहीं है, जैन आगमों में विवाह तीन प्रकार माता-पिता द्वारा आयोजित, स्वयंवर, गान्धर्व आदि पुराण में पति-पत्नी को सामाजिक दायित्व एवं पारस्परिक सम्बन्धों की चर्चा की गयी है। परिवार सम्बन्ध में जैन में सामन्यतया नियमों का अभाव मिलता है। उत्तराध्ययन सूत्र में उल्लेख है कि जिनके पास अपना कुछ नहीं है वे सुख से रहते हैं। यद्यपि यह वाक्य भिक्षुओं के लिए प्रतीत होता है। तथापि इस धारणा ने तत्कालीन जनमानस को प्रभावित किया।
नारी के प्रति जैन तीर्थकारों की दृष्टि गौतम बुद्ध से भी प्राप्त की थी, गौतमबुद्ध संघ में पुरुषों को अधिक श्रेष्ठ मानते थे, किन्तु जैन ग्रन्थों में कहीं भी नारी के प्रति भेद-भाव का उल्लेख नहीं मिलता है। जैन धर्म में स्त्रियों का पूर्णतः अधिकार रहता था। किसी सीमा तक परिवार की सम्पत्ति में भी उन्हें सीमित अधिकार प्रदान किया था। महापुराणों में वर्णित है कि पिता की सम्पत्ति में पुत्र के समान पुत्रियाँ भी बराबर मांग की अधिकारी होती हैं। जैन साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि पुत्राभाव में ही पिता के धन पर पुत्री का स्वत्व सम्भव था। जैन धर्म में प्रारम्भ से ही भिक्षुणियों को संघ में प्रवेश की अनुमति थी। जैन साहित्य में यह उल्लेख प्राप्त होता है कि ऋषभदेव के समय भी भिक्षुणियाँ संघ में सम्मिलित थी। सुभद्रा का उल्लेख एक पवित्र-स्त्री के रूप में किया गया है। जैन भिक्षुणी के रूप में जयन्ती का विशेष रूप से लिया जाता है। जिन्होंने संसारिक सुखों से विमुख होकर भिक्षुणी जीवन अंगीकार किया। यह भी विदित तथ्य है कि महावीर भी सर्वप्रथम शिष्या अज्यचन्दना (स्त्री) थी जिसके अपरिमित ज्ञान एवं पद-प्रदर्शन से अनेक भिक्षुणियों का मोक्ष साथ हुआ था।
जैन धर्म में स्त्रियों के गुणों की चर्चा करते हुए कहा गया है कि जो गुण सहित स्त्रियाँ है, जिनका यश लोक में फैला हुआ है तथा जो मनुष्य लोक में