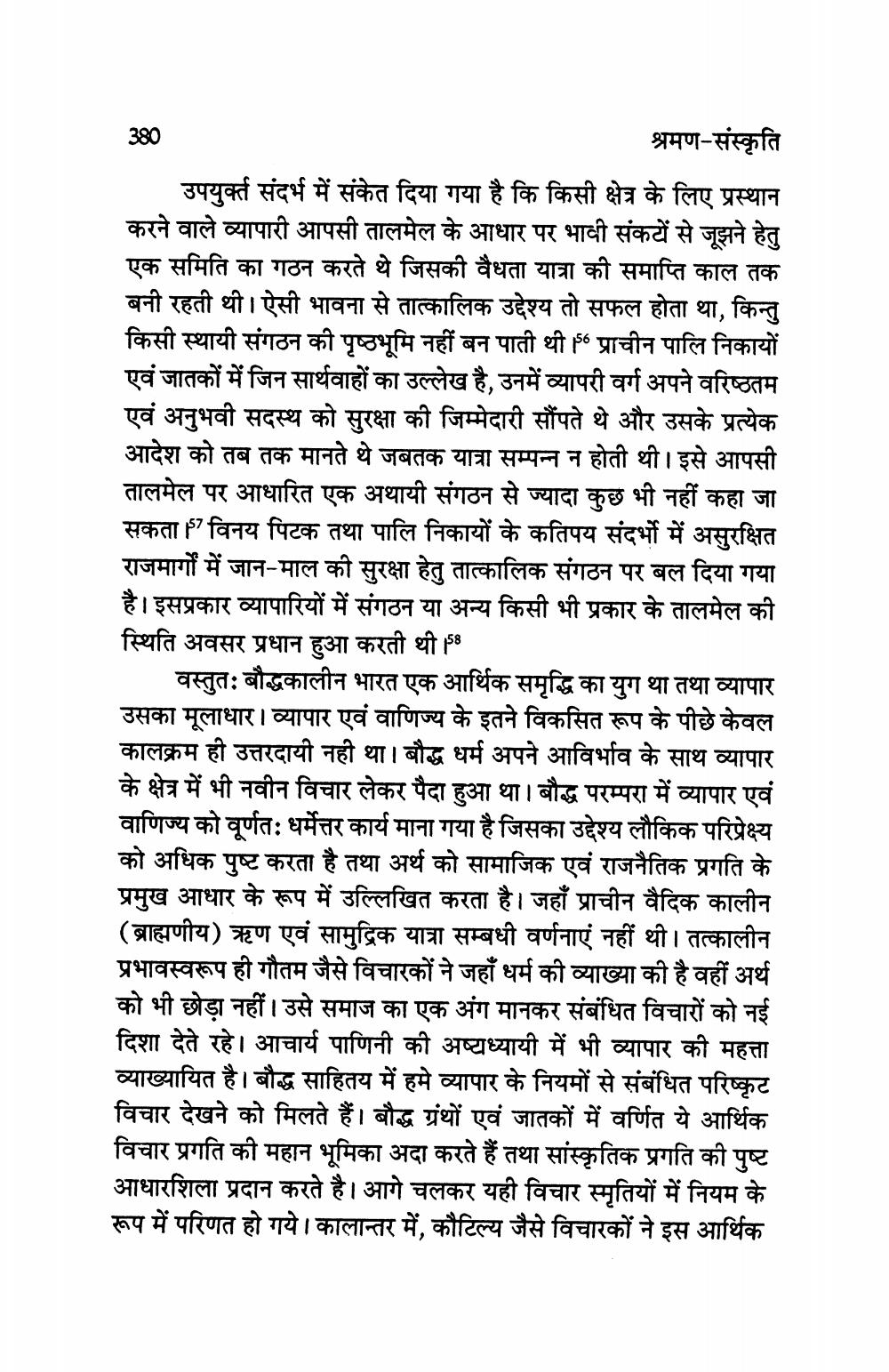________________
380
श्रमण-संस्कृति उपयुक्त संदर्भ में संकेत दिया गया है कि किसी क्षेत्र के लिए प्रस्थान करने वाले व्यापारी आपसी तालमेल के आधार पर भावी संकट से जूझने हेतु एक समिति का गठन करते थे जिसकी वैधता यात्रा की समाप्ति काल तक बनी रहती थी। ऐसी भावना से तात्कालिक उद्देश्य तो सफल होता था, किन्तु किसी स्थायी संगठन की पृष्ठभूमि नहीं बन पाती थी। प्राचीन पालि निकायों एवं जातकों में जिन सार्थवाहों का उल्लेख है, उनमें व्यापरी वर्ग अपने वरिष्ठतम एवं अनुभवी सदस्थ को सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपते थे और उसके प्रत्येक आदेश को तब तक मानते थे जबतक यात्रा सम्पन्न न होती थी। इसे आपसी तालमेल पर आधारित एक अथायी संगठन से ज्यादा कुछ भी नहीं कहा जा सकता विनय पिटक तथा पालि निकायों के कतिपय संदर्भो में असुरक्षित राजमार्गों में जान-माल की सुरक्षा हेतु तात्कालिक संगठन पर बल दिया गया है। इसप्रकार व्यापारियों में संगठन या अन्य किसी भी प्रकार के तालमेल की स्थिति अवसर प्रधान हुआ करती थी।
वस्तुतः बौद्धकालीन भारत एक आर्थिक समृद्धि का युग था तथा व्यापार उसका मूलाधार । व्यापार एवं वाणिज्य के इतने विकसित रूप के पीछे केवल कालक्रम ही उत्तरदायी नही था। बौद्ध धर्म अपने आविर्भाव के साथ व्यापार के क्षेत्र में भी नवीन विचार लेकर पैदा हुआ था। बौद्ध परम्परा में व्यापार एवं वाणिज्य को पूर्णतः धर्मेत्तर कार्य माना गया है जिसका उद्देश्य लौकिक परिप्रेक्ष्य को अधिक पुष्ट करता है तथा अर्थ को सामाजिक एवं राजनैतिक प्रगति के प्रमुख आधार के रूप में उल्लिखित करता है। जहाँ प्राचीन वैदिक कालीन (ब्राह्मणीय) ऋण एवं सामुद्रिक यात्रा सम्बधी वर्णनाएं नहीं थी। तत्कालीन प्रभावस्वरूप ही गौतम जैसे विचारकों ने जहाँ धर्म की व्याख्या की है वहीं अर्थ को भी छोड़ा नहीं। उसे समाज का एक अंग मानकर संबंधित विचारों को नई दिशा देते रहे। आचार्य पाणिनी की अष्टाध्यायी में भी व्यापार की महत्ता व्याख्यायित है। बौद्ध साहितय में हमे व्यापार के नियमों से संबंधित परिष्कृट विचार देखने को मिलते हैं। बौद्ध ग्रंथों एवं जातकों में वर्णित ये आर्थिक विचार प्रगति की महान भूमिका अदा करते हैं तथा सांस्कृतिक प्रगति की पुष्ट आधारशिला प्रदान करते है। आगे चलकर यही विचार स्मृतियों में नियम के रूप में परिणत हो गये। कालान्तर में, कौटिल्य जैसे विचारकों ने इस आर्थिक