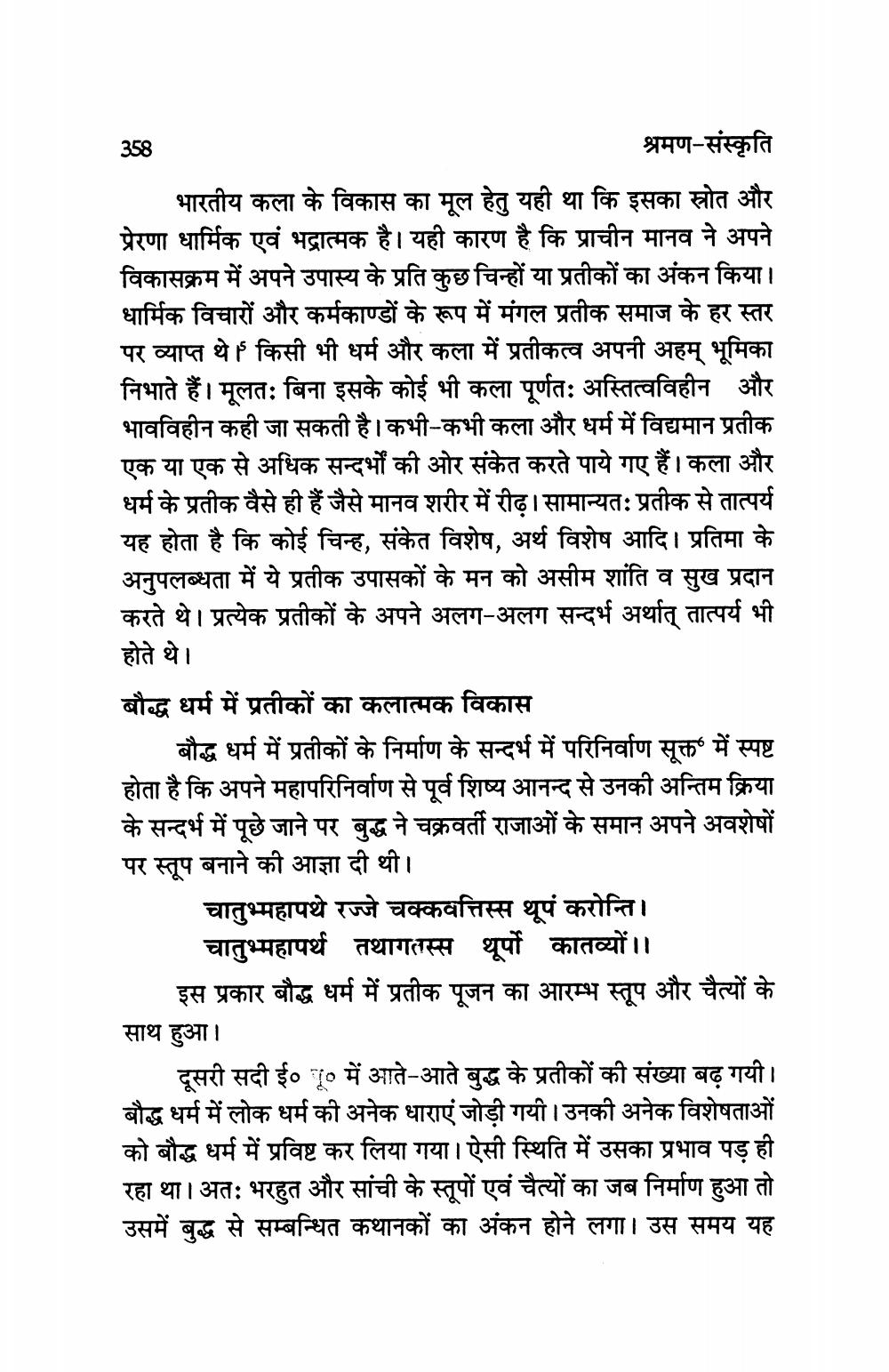________________
श्रमण-संस्कृति
भारतीय कला के विकास का मूल हेतु यही था कि इसका स्रोत और प्रेरणा धार्मिक एवं भद्रात्मक है । यही कारण है कि प्राचीन मानव ने अपने विकासक्रम में अपने उपास्य के प्रति कुछ चिन्हों या प्रतीकों का अंकन किया। धार्मिक विचारों और कर्मकाण्डों के रूप में मंगल प्रतीक समाज के हर स्तर पर व्याप्त थे। किसी भी धर्म और कला में प्रतीकत्व अपनी अहम् भूमिका निभाते हैं। मूलतः बिना इसके कोई भी कला पूर्णत: अस्तित्वविहीन और भावविहीन कही जा सकती है। कभी-कभी कला और धर्म में विद्यमान प्रतीक एक या एक से अधिक सन्दर्भों की ओर संकेत करते पाये गए हैं। कला और धर्म के प्रतीक वैसे ही हैं जैसे मानव शरीर में रीढ़ । सामान्यतः प्रतीक से तात्पर्य यह होता है कि कोई चिन्ह, संकेत विशेष, अर्थ विशेष आदि । प्रतिमा के अनुपलब्धता में ये प्रतीक उपासकों के मन को असीम शांति व सुख प्रदान करते थे। प्रत्येक प्रतीकों के अपने अलग-अलग सन्दर्भ अर्थात् तात्पर्य भी होते थे ।
358
बौद्ध धर्म में प्रतीकों का कलात्मक विकास
बौद्ध धर्म में प्रतीकों के निर्माण के सन्दर्भ में परिनिर्वाण सूक्त' में स्पष्ट होता है कि अपने महापरिनिर्वाण से पूर्व शिष्य आनन्द से उनकी अन्तिम क्रिया सन्दर्भ में पूछे जाने पर बुद्ध ने चक्रवर्ती राजाओं के समान अपने अवशेषों पर स्तूप बनाने की आज्ञा दी थी।
चातुभ्महापथे रज्जे चक्कवत्तिस्स थूपं करोन्ति । चातुभ्महापर्थ तथागतस्स थूप कातव्यों ।।
इस प्रकार बौद्ध धर्म में प्रतीक पूजन का आरम्भ स्तूप और चैत्यों के साथ हुआ।
दूसरी सदी ई० पू० में आते-आते बुद्ध के प्रतीकों की संख्या बढ़ गयी । बौद्ध धर्म में लोक धर्म की अनेक धाराएं जोड़ी गयी। उनकी अनेक विशेषताओं को बौद्ध धर्म में प्रविष्ट कर लिया गया। ऐसी स्थिति में उसका प्रभाव पड़ ही रहा था। अतः भरहुत और सांची के स्तूपों एवं चैत्यों का जब निर्माण हुआ तो उसमें बुद्ध से सम्बन्धित कथानकों का अंकन होने लगा। उस समय यह