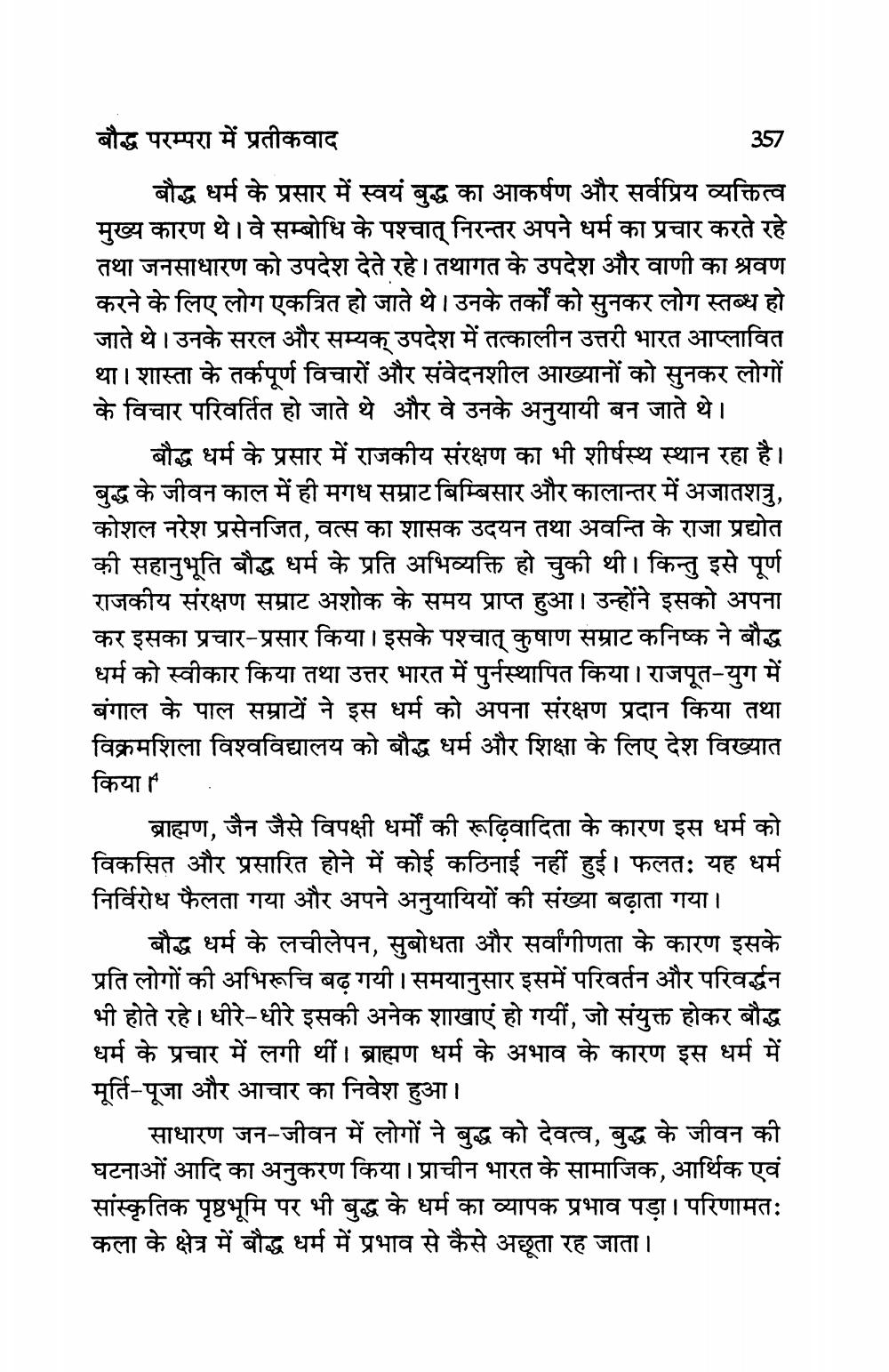________________
बौद्ध परम्परा में प्रतीकवाद
357 बौद्ध धर्म के प्रसार में स्वयं बुद्ध का आकर्षण और सर्वप्रिय व्यक्तित्व मुख्य कारण थे। वे सम्बोधि के पश्चात् निरन्तर अपने धर्म का प्रचार करते रहे तथा जनसाधारण को उपदेश देते रहे। तथागत के उपदेश और वाणी का श्रवण करने के लिए लोग एकत्रित हो जाते थे। उनके तर्कों को सुनकर लोग स्तब्ध हो जाते थे। उनके सरल और सम्यक् उपदेश में तत्कालीन उत्तरी भारत आप्लावित था। शास्ता के तर्कपूर्ण विचारों और संवेदनशील आख्यानों को सुनकर लोगों के विचार परिवर्तित हो जाते थे और वे उनके अनुयायी बन जाते थे। ___बौद्ध धर्म के प्रसार में राजकीय संरक्षण का भी शीर्षस्थ स्थान रहा है। बद्ध के जीवन काल में ही मगध सम्राट बिम्बिसार और कालान्तर में अजातशत्र, कोशल नरेश प्रसेनजित, वत्स का शासक उदयन तथा अवन्ति के राजा प्रद्योत की सहानुभूति बौद्ध धर्म के प्रति अभिव्यक्ति हो चुकी थी। किन्तु इसे पूर्ण राजकीय संरक्षण सम्राट अशोक के समय प्राप्त हुआ। उन्होंने इसको अपना कर इसका प्रचार-प्रसार किया। इसके पश्चात् कुषाण सम्राट कनिष्क ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तथा उत्तर भारत में पुर्नस्थापित किया। राजपूत-युग में बंगाल के पाल सम्राटों ने इस धर्म को अपना संरक्षण प्रदान किया तथा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को बौद्ध धर्म और शिक्षा के लिए देश विख्यात किया।
ब्राह्मण, जैन जैसे विपक्षी धर्मों की रूढ़िवादिता के कारण इस धर्म को विकसित और प्रसारित होने में कोई कठिनाई नहीं हुई। फलतः यह धर्म निर्विरोध फैलता गया और अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाता गया।
बौद्ध धर्म के लचीलेपन, सुबोधता और सर्वांगीणता के कारण इसके प्रति लोगों की अभिरूचि बढ़ गयी। समयानुसार इसमें परिवर्तन और परिवर्द्धन भी होते रहे। धीरे-धीरे इसकी अनेक शाखाएं हो गयीं, जो संयुक्त होकर बौद्ध धर्म के प्रचार में लगी थीं। ब्राह्मण धर्म के अभाव के कारण इस धर्म में मूर्ति-पूजा और आचार का निवेश हुआ।
साधारण जन-जीवन में लोगों ने बुद्ध को देवत्व, बुद्ध के जीवन की घटनाओं आदि का अनुकरण किया। प्राचीन भारत के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर भी बुद्ध के धर्म का व्यापक प्रभाव पड़ा। परिणामतः कला के क्षेत्र में बौद्ध धर्म में प्रभाव से कैसे अछूता रह जाता।