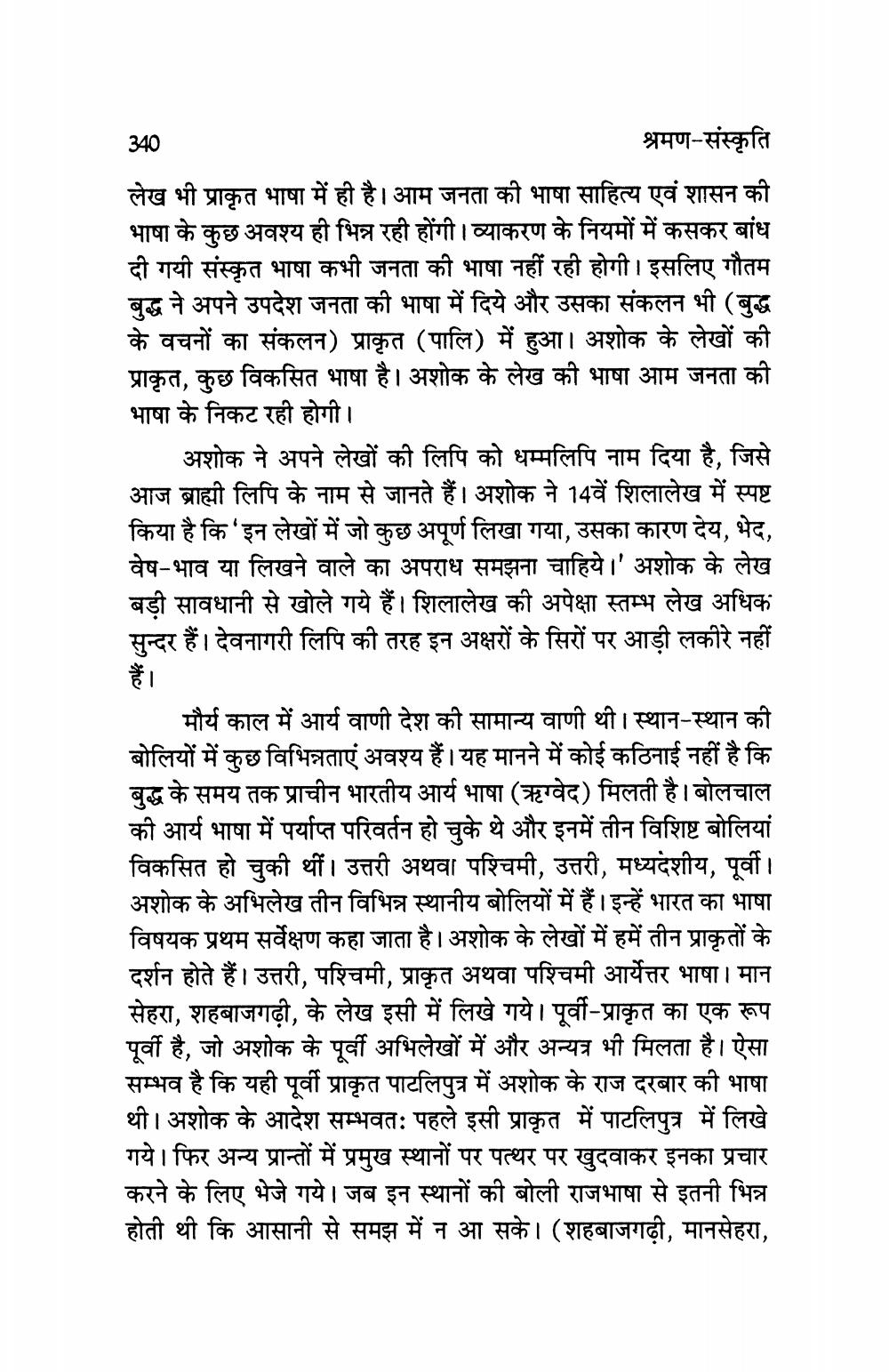________________
340
श्रमण-संस्कृति लेख भी प्राकृत भाषा में ही है। आम जनता की भाषा साहित्य एवं शासन की भाषा के कुछ अवश्य ही भिन्न रही होंगी। व्याकरण के नियमों में कसकर बांध दी गयी संस्कृत भाषा कभी जनता की भाषा नहीं रही होगी। इसलिए गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश जनता की भाषा में दिये और उसका संकलन भी (बुद्ध के वचनों का संकलन) प्राकृत (पालि) में हुआ। अशोक के लेखों की प्राकृत, कुछ विकसित भाषा है। अशोक के लेख की भाषा आम जनता की भाषा के निकट रही होगी।
अशोक ने अपने लेखों की लिपि को धम्मलिपि नाम दिया है, जिसे आज ब्राह्मी लिपि के नाम से जानते हैं। अशोक ने 14वें शिलालेख में स्पष्ट किया है कि इन लेखों में जो कुछ अपूर्ण लिखा गया, उसका कारण देय, भेद, वेष-भाव या लिखने वाले का अपराध समझना चाहिये।' अशोक के लेख बड़ी सावधानी से खोले गये हैं। शिलालेख की अपेक्षा स्तम्भ लेख अधिक सुन्दर हैं। देवनागरी लिपि की तरह इन अक्षरों के सिरों पर आड़ी लकीरे नहीं
__ मौर्य काल में आर्य वाणी देश की सामान्य वाणी थी। स्थान-स्थान की बोलियों में कुछ विभिन्नताएं अवश्य हैं। यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि बुद्ध के समय तक प्राचीन भारतीय आर्य भाषा (ऋग्वेद) मिलती है। बोलचाल की आर्य भाषा में पर्याप्त परिवर्तन हो चुके थे और इनमें तीन विशिष्ट बोलियां विकसित हो चुकी थीं। उत्तरी अथवा पश्चिमी, उत्तरी, मध्यदेशीय, पूर्वी। अशोक के अभिलेख तीन विभिन्न स्थानीय बोलियों में हैं। इन्हें भारत का भाषा विषयक प्रथम सर्वेक्षण कहा जाता है। अशोक के लेखों में हमें तीन प्राकृतों के दर्शन होते हैं। उत्तरी, पश्चिमी, प्राकृत अथवा पश्चिमी आर्येत्तर भाषा। मान सेहरा, शहबाजगढ़ी, के लेख इसी में लिखे गये। पूर्वी-प्राकृत का एक रूप पूर्वी है, जो अशोक के पूर्वी अभिलेखों में और अन्यत्र भी मिलता है। ऐसा सम्भव है कि यही पूर्वी प्राकृत पाटलिपुत्र में अशोक के राज दरबार की भाषा थी। अशोक के आदेश सम्भवतः पहले इसी प्राकृत में पाटलिपुत्र में लिखे गये। फिर अन्य प्रान्तों में प्रमुख स्थानों पर पत्थर पर खुदवाकर इनका प्रचार करने के लिए भेजे गये। जब इन स्थानों की बोली राजभाषा से इतनी भिन्न होती थी कि आसानी से समझ में न आ सके। (शहबाजगढ़ी, मानसेहरा,