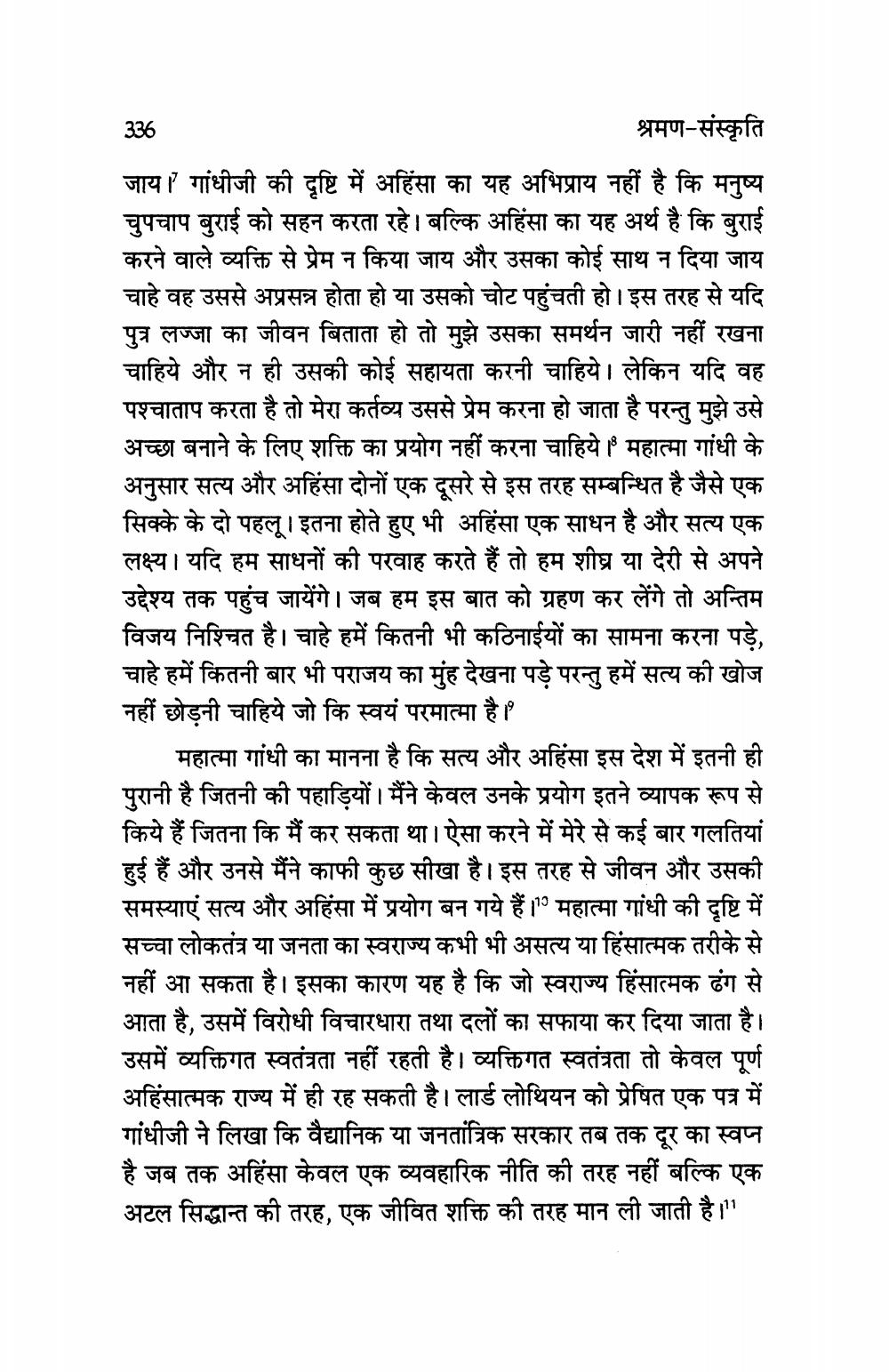________________
336
श्रमण-संस्कृति जाय।' गांधीजी की दृष्टि में अहिंसा का यह अभिप्राय नहीं है कि मनुष्य चुपचाप बुराई को सहन करता रहे। बल्कि अहिंसा का यह अर्थ है कि बुराई करने वाले व्यक्ति से प्रेम न किया जाय और उसका कोई साथ न दिया जाय चाहे वह उससे अप्रसन्न होता हो या उसको चोट पहुंचती हो। इस तरह से यदि पुत्र लज्जा का जीवन बिताता हो तो मुझे उसका समर्थन जारी नहीं रखना चाहिये और न ही उसकी कोई सहायता करनी चाहिये। लेकिन यदि वह पश्चाताप करता है तो मेरा कर्तव्य उससे प्रेम करना हो जाता है परन्तु मुझे उसे अच्छा बनाने के लिए शक्ति का प्रयोग नहीं करना चाहिये। महात्मा गांधी के अनुसार सत्य और अहिंसा दोनों एक दूसरे से इस तरह सम्बन्धित है जैसे एक सिक्के के दो पहलू । इतना होते हुए भी अहिंसा एक साधन है और सत्य एक लक्ष्य। यदि हम साधनों की परवाह करते हैं तो हम शीघ्र या देरी से अपने उद्देश्य तक पहुंच जायेंगे। जब हम इस बात को ग्रहण कर लेंगे तो अन्तिम विजय निश्चित है। चाहे हमें कितनी भी कठिनाईयों का सामना करना पड़े, चाहे हमें कितनी बार भी पराजय का मुंह देखना पड़े परन्तु हमें सत्य की खोज नहीं छोड़नी चाहिये जो कि स्वयं परमात्मा है।'
महात्मा गांधी का मानना है कि सत्य और अहिंसा इस देश में इतनी ही पुरानी है जितनी की पहाड़ियों। मैंने केवल उनके प्रयोग इतने व्यापक रूप से किये हैं जितना कि मैं कर सकता था। ऐसा करने में मेरे से कई बार गलतियां हुई हैं और उनसे मैंने काफी कुछ सीखा है। इस तरह से जीवन और उसकी समस्याएं सत्य और अहिंसा में प्रयोग बन गये हैं। महात्मा गांधी की दृष्टि में सच्चा लोकतंत्र या जनता का स्वराज्य कभी भी असत्य या हिंसात्मक तरीके से नहीं आ सकता है। इसका कारण यह है कि जो स्वराज्य हिंसात्मक ढंग से आता है, उसमें विरोधी विचारधारा तथा दलों का सफाया कर दिया जाता है। उसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं रहती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो केवल पूर्ण अहिंसात्मक राज्य में ही रह सकती है। लार्ड लोथियन को प्रेषित एक पत्र में गांधीजी ने लिखा कि वैद्यानिक या जनतांत्रिक सरकार तब तक दूर का स्वप्न है जब तक अहिंसा केवल एक व्यवहारिक नीति की तरह नहीं बल्कि एक अटल सिद्धान्त की तरह, एक जीवित शक्ति की तरह मान ली जाती है।"