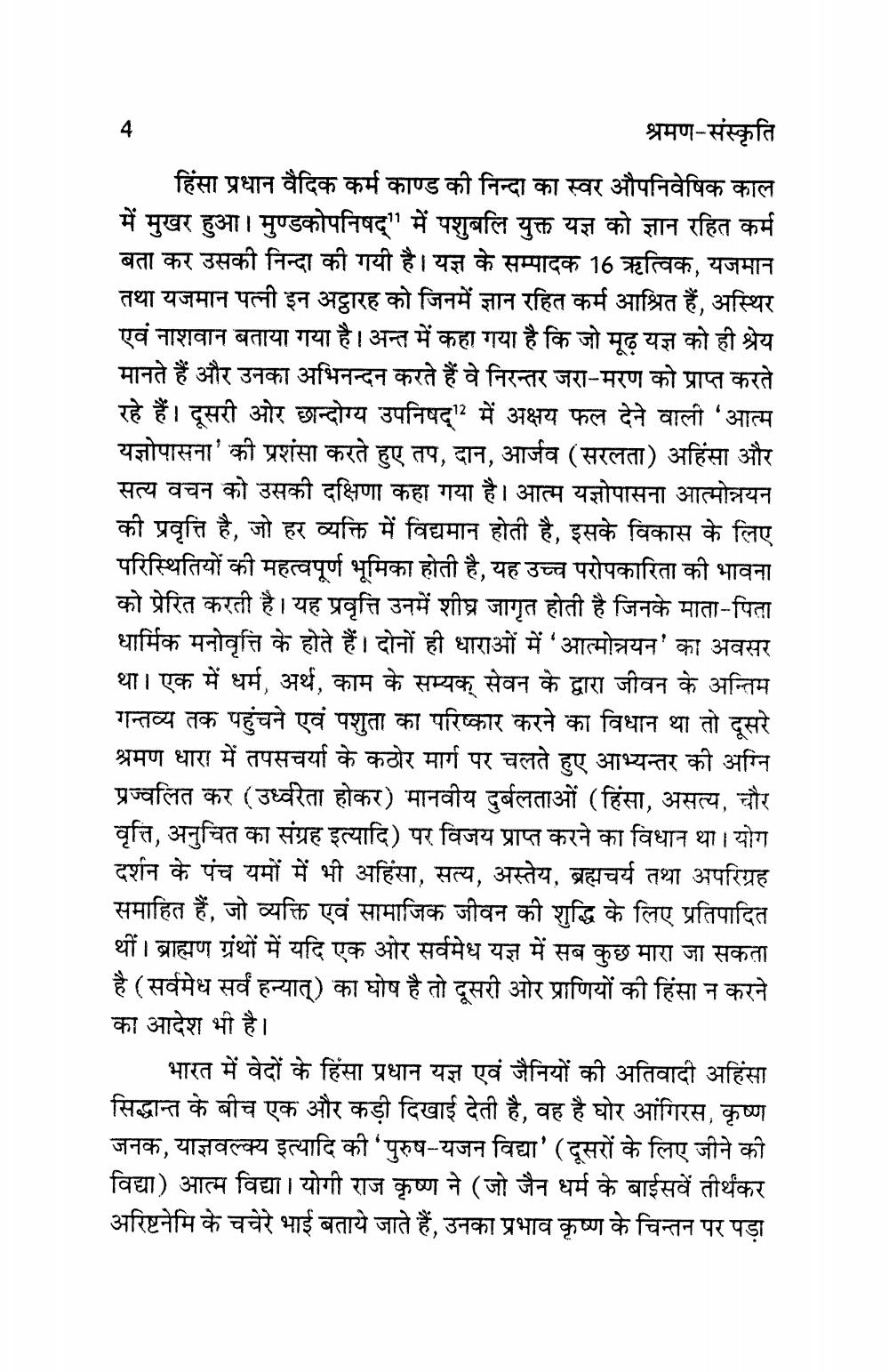________________
श्रमण-संस्कृति हिंसा प्रधान वैदिक कर्म काण्ड की निन्दा का स्वर औपनिवेषिक काल में मुखर हुआ। मुण्डकोपनिषद् में पशुबलि युक्त यज्ञ को ज्ञान रहित कर्म बता कर उसकी निन्दा की गयी है। यज्ञ के सम्पादक 16 ऋत्विक, यजमान तथा यजमान पत्नी इन अट्ठारह को जिनमें ज्ञान रहित कर्म आश्रित हैं, अस्थिर एवं नाशवान बताया गया है। अन्त में कहा गया है कि जो मूढ यज्ञ को ही श्रेय मानते हैं और उनका अभिनन्दन करते हैं वे निरन्तर जरा-मरण को प्राप्त करते रहे हैं। दूसरी ओर छान्दोग्य उपनिषद् में अक्षय फल देने वाली 'आत्म यज्ञोपासना' की प्रशंसा करते हुए तप, दान, आर्जव (सरलता) अहिंसा और सत्य वचन को उसकी दक्षिणा कहा गया है। आत्म यज्ञोपासना आत्मोन्नयन की प्रवृत्ति है, जो हर व्यक्ति में विद्यमान होती है, इसके विकास के लिए परिस्थितियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यह उच्च परोपकारिता की भावना को प्रेरित करती है। यह प्रवृत्ति उनमें शीघ्र जागृत होती है जिनके माता-पिता धार्मिक मनोवृत्ति के होते हैं। दोनों ही धाराओं में 'आत्मोन्नयन' का अवसर था। एक में धर्म, अर्थ, काम के सम्यक् सेवन के द्वारा जीवन के अन्तिम गन्तव्य तक पहुंचने एवं पशुता का परिष्कार करने का विधान था तो दूसरे श्रमण धारा में तपसचर्या के कठोर मार्ग पर चलते हुए आभ्यन्तर की अग्नि प्रज्वलित कर (उर्ध्वरेता होकर) मानवीय दुर्बलताओं (हिंसा, असत्य, चौर वृत्ति, अनुचित का संग्रह इत्यादि) पर विजय प्राप्त करने का विधान था। योग दर्शन के पंच यमों में भी अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह समाहित हैं, जो व्यक्ति एवं सामाजिक जीवन की शद्धि के लिए प्रतिपादित थीं। ब्राह्मण ग्रंथों में यदि एक ओर सर्वमेध यज्ञ में सब कुछ मारा जा सकता है (सर्वमेध सर्वं हन्यात्) का घोष है तो दूसरी ओर प्राणियों की हिंसा न करने का आदेश भी है।
भारत में वेदों के हिंसा प्रधान यज्ञ एवं जैनियों की अतिवादी अहिंसा सिद्धान्त के बीच एक और कड़ी दिखाई देती है, वह है घोर आंगिरस, कृष्ण जनक, याज्ञवल्क्य इत्यादि की 'पुरुष-यजन विद्या' (दूसरों के लिए जीने की विद्या) आत्म विद्या । योगी राज कृष्ण ने (जो जैन धर्म के बाईसवें तीर्थंकर अरिष्टनेमि के चचेरे भाई बताये जाते हैं, उनका प्रभाव कृष्ण के चिन्तन पर पड़ा