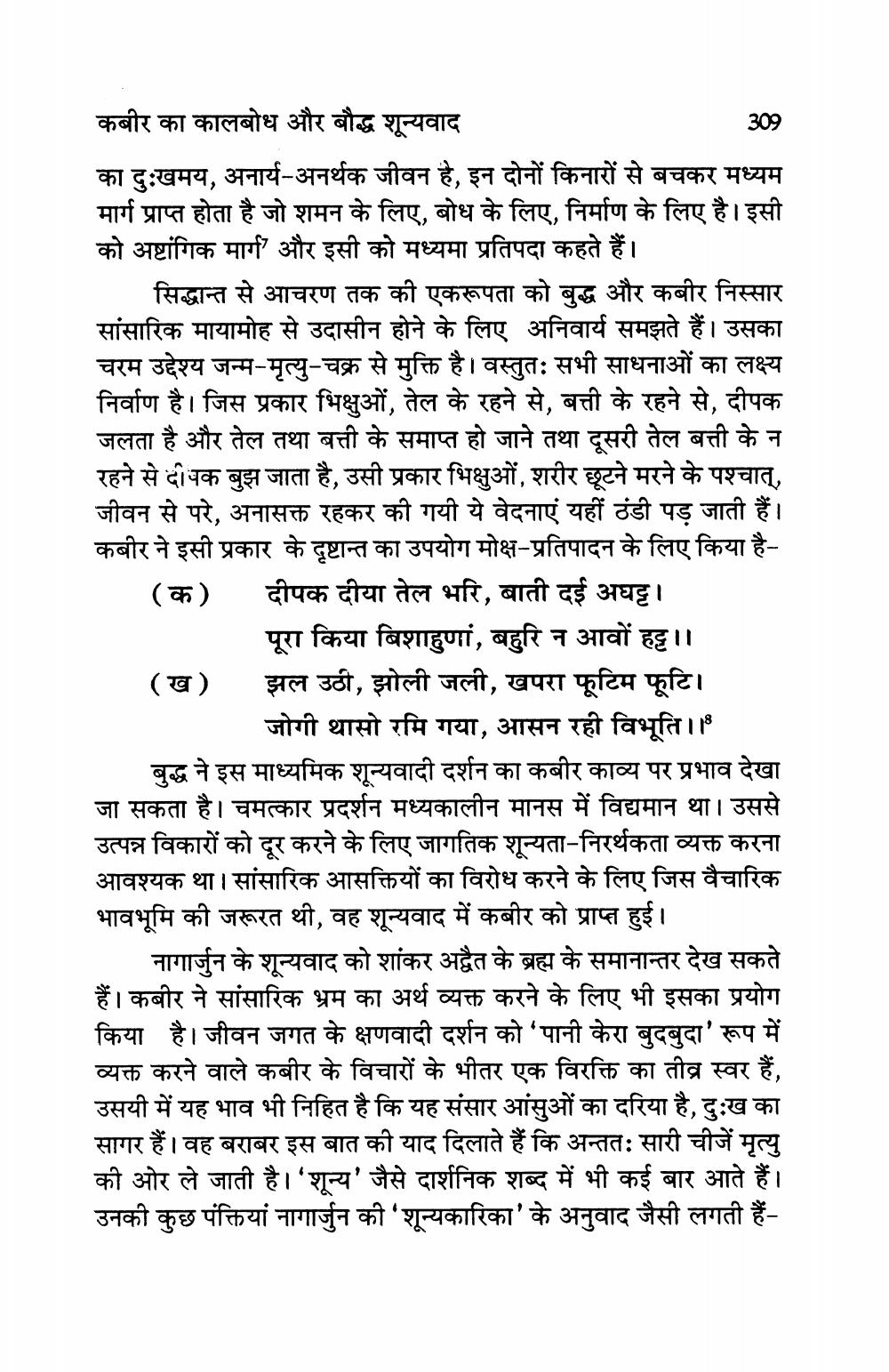________________
कबीर का कालबोध और बौद्ध शून्यवाद
309
का दुःखमय, अनार्य-अनर्थक जीवन है, इन दोनों किनारों से बचकर मध्यम मार्ग प्राप्त होता है जो शमन के लिए, बोध के लिए, निर्माण के लिए है। इसी को अष्टांगिक मार्ग' और इसी को मध्यमा प्रतिपदा कहते हैं ।
सिद्धान्त से आचरण तक की एकरूपता को बुद्ध और कबीर निस्सार सांसारिक मायामोह से उदासीन होने के लिए अनिवार्य समझते हैं । उसका चरम उद्देश्य जन्म-मृत्यु-चक्र से मुक्ति है। वस्तुतः सभी साधनाओं का लक्ष्य निर्वाण है । जिस प्रकार भिक्षुओं, तेल के रहने से, बत्ती के रहने से, दीपक जलता है और तेल तथा बत्ती के समाप्त हो जाने तथा दूसरी तेल बत्ती के न रहने से दीपक बुझ जाता है, उसी प्रकार भिक्षुओं, शरीर छूटने मरने के पश्चात्, जीवन से परे, अनासक्त रहकर की गयी ये वेदनाएं यहीं ठंडी पड़ जाती हैं। कबीर ने इसी प्रकार के दृष्टान्त का उपयोग मोक्ष-प्रतिपादन के लिए किया हैदीपक दीया तेल भरि, बाती दई अघट्ट | पूरा किया बिशाहुणां, बहुरि न आवों हट्ट | | झल उठी, झोली जली, खपरा फूटिम फूटि । जोगी थासो रम गया, आसन रही विभूति । । "
(क)
(ख)
बुद्ध ने इस माध्यमिक शून्यवादी दर्शन का कबीर काव्य पर प्रभाव देखा जा सकता है। चमत्कार प्रदर्शन मध्यकालीन मानस में विद्यमान था । उससे उत्पन्न विकारों को दूर करने के लिए जागतिक शून्यता- निरर्थकता व्यक्त करना आवश्यक था। सांसारिक आसक्तियों का विरोध करने के लिए जिस वैचारिक भावभूमि की जरूरत थी, वह शून्यवाद में कबीर को प्राप्त हुई ।
नागार्जुन के शून्यवाद को शांकर अद्वैत के ब्रह्म के समानान्तर देख सकते हैं। कबीर ने सांसारिक भ्रम का अर्थ व्यक्त करने के लिए भी इसका प्रयोग किया है। जीवन जगत के क्षणवादी दर्शन को 'पानी केरा बुदबुदा' रूप में व्यक्त करने वाले कबीर के विचारों के भीतर एक विरक्ति का तीव्र स्वर हैं, उसयी में यह भाव भी निहित है कि यह संसार आंसुओं का दरिया है, दुःख का सागर हैं। वह बराबर इस बात की याद दिलाते हैं कि अन्ततः सारी चीजें मृत्यु की ओर ले जाती है। 'शून्य' जैसे दार्शनिक शब्द में भी कई बार आते हैं । उनकी कुछ पंक्तियां नागार्जुन की 'शून्यकारिका' के अनुवाद जैसी लगती हैं