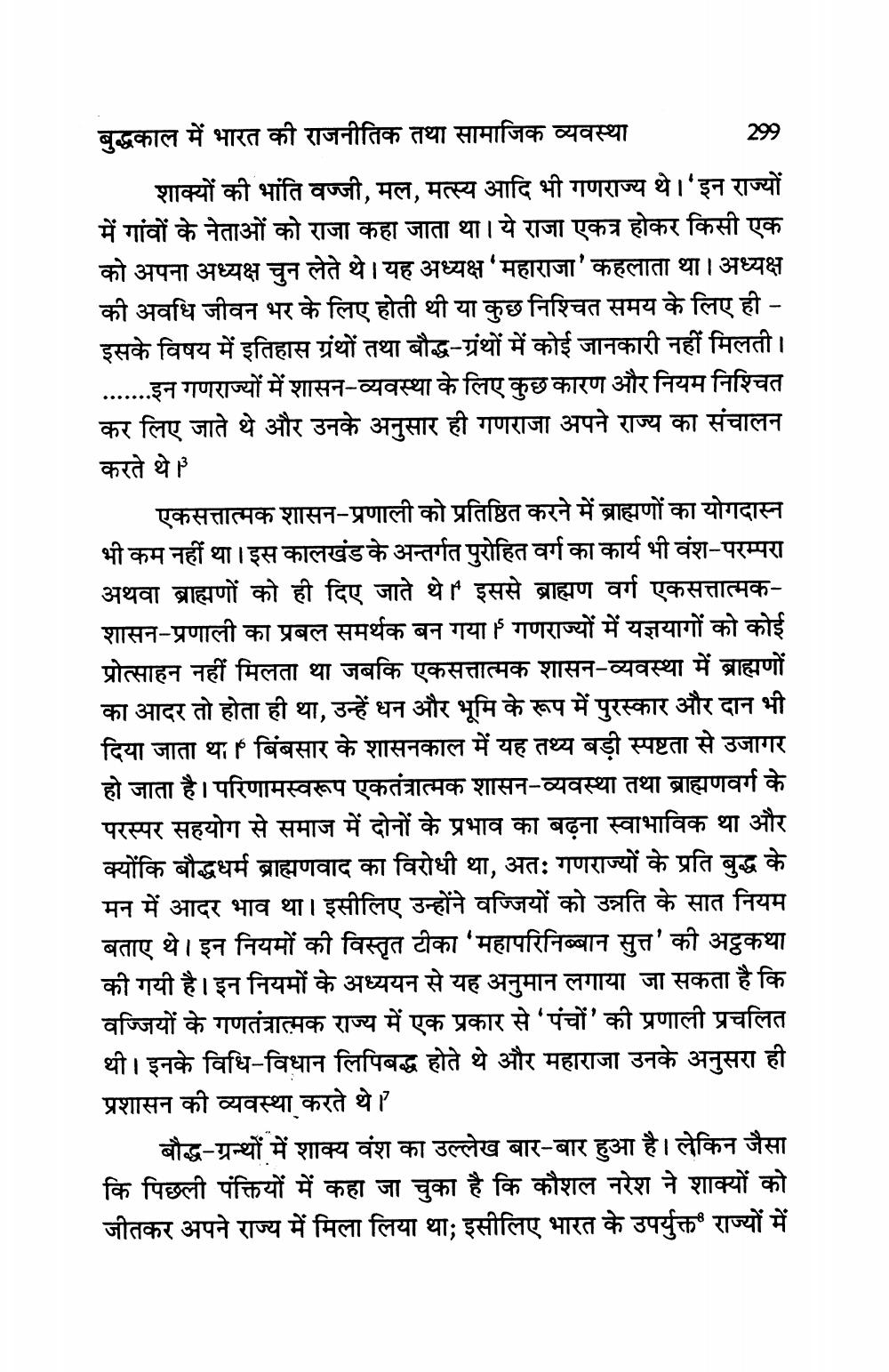________________
बुद्धकाल में भारत की राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्था
शाक्यों की भांति वज्जी, मल, मत्स्य आदि भी गणराज्य थे । ' इन राज्यों में गांवों के नेताओं को राजा कहा जाता था । ये राजा एकत्र होकर किसी एक को अपना अध्यक्ष चुन लेते थे । यह अध्यक्ष 'महाराजा' कहलाता था । अध्यक्ष की अवधि जीवन भर के लिए होती थी या कुछ निश्चित समय के लिए ही इसके विषय में इतिहास ग्रंथों तथा बौद्ध-ग्रंथों में कोई जानकारी नहीं मिलती ।
299
.. इन गणराज्यों में शासन-व्यवस्था के लिए कुछ कारण और नियम निश्चित कर लिए जाते थे और उनके अनुसार ही गणराजा अपने राज्य का संचालन करते थे।
एकसत्तात्मक शासन-प्रणाली को प्रतिष्ठित करने में ब्राह्मणों का योगदान भी कम नहीं था । इस कालखंड के अन्तर्गत पुरोहित वर्ग का कार्य भी वंश-परम्परा अथवा ब्राह्मणों को ही दिए जाते थे। इससे ब्राह्मण वर्ग एकसत्तात्मकशासन-प्रणाली का प्रबल समर्थक बन गया । गणराज्यों में यज्ञयागों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता था जबकि एकसत्तात्मक शासन व्यवस्था में ब्राह्मणों का आदर तो होता ही था, उन्हें धन और भूमि के रूप में पुरस्कार और दान भी दिया जाता था । बिंबसार के शासनकाल में यह तथ्य बड़ी स्पष्टता से उजागर हो जाता है। परिणामस्वरूप एकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था तथा ब्राह्मणवर्ग के परस्पर सहयोग से समाज में दोनों के प्रभाव का बढ़ना स्वाभाविक था और क्योंकि बौद्धधर्म ब्राह्मणवाद का विरोधी था, अतः गणराज्यों के प्रति बुद्ध के मन में आदर भाव था । इसीलिए उन्होंने वज्जियों को उन्नति के सात नियम बताए थे। इन नियमों की विस्तृत टीका 'महापरिनिब्बान सुत्त' की अट्ठकथा की गयी है। इन नियमों के अध्ययन से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि वज्जियों के गणतंत्रात्मक राज्य में एक प्रकार से 'पंचों' की प्रणाली प्रचलित थी। इनके विधि-विधान लिपिबद्ध होते थे और महाराजा उनके अनुसरा ही प्रशासन की व्यवस्था करते थे ।
बौद्ध-ग्रन्थों में शाक्य वंश का उल्लेख बार-बार हुआ है। लेकिन जैसा कि पिछली पंक्तियों में कहा जा चुका है कि कौशल नरेश ने शाक्यों को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था; इसीलिए भारत के उपर्युक्त राज्यों में