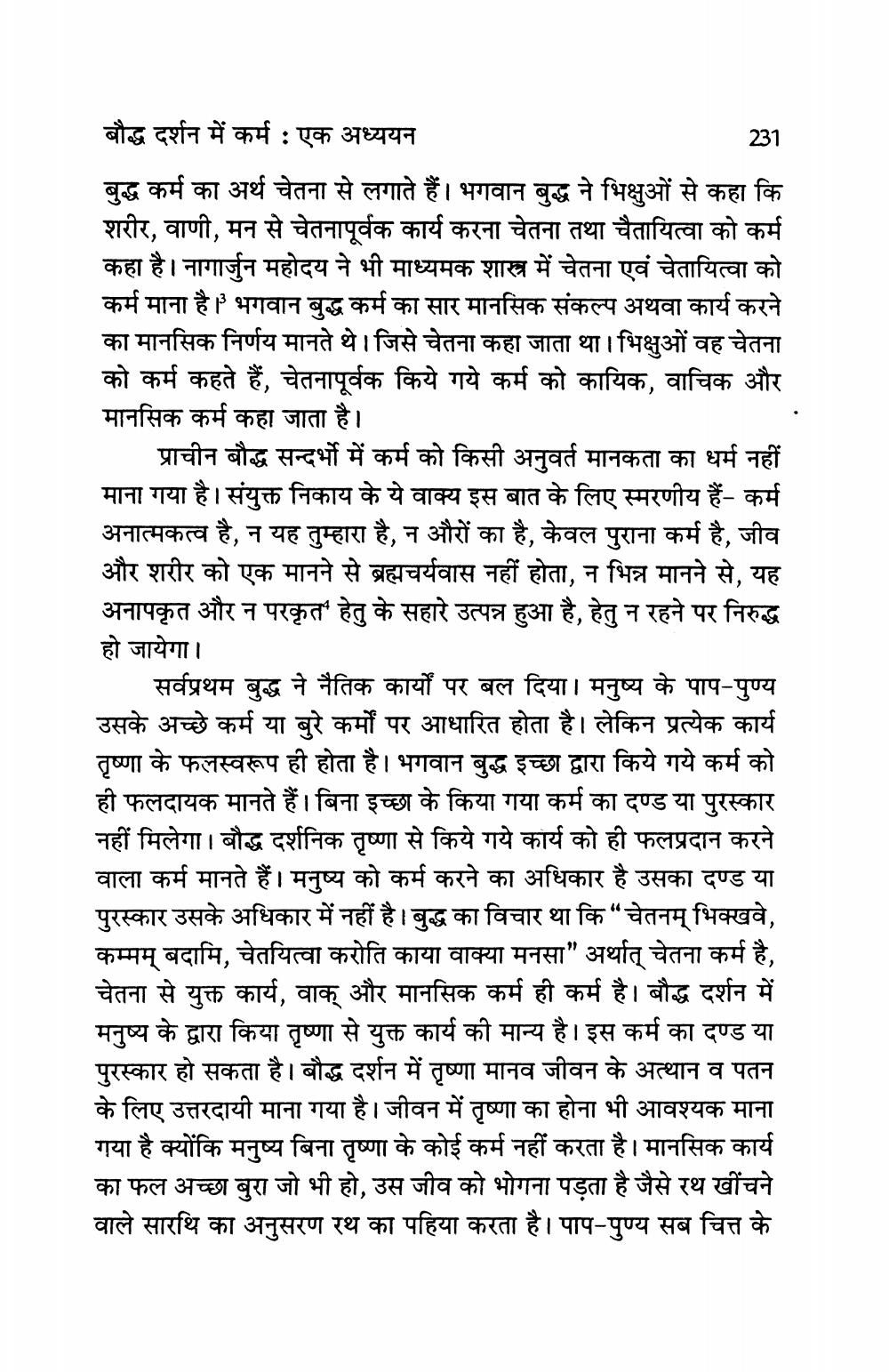________________
बौद्ध दर्शन में कर्म : एक अध्ययन
231 बुद्ध कर्म का अर्थ चेतना से लगाते हैं। भगवान बुद्ध ने भिक्षुओं से कहा कि शरीर, वाणी, मन से चेतनापूर्वक कार्य करना चेतना तथा चैतायित्वा को कर्म कहा है। नागार्जुन महोदय ने भी माध्यमक शास्त्र में चेतना एवं चेतायित्वा को कर्म माना है। भगवान बुद्ध कर्म का सार मानसिक संकल्प अथवा कार्य करने का मानसिक निर्णय मानते थे। जिसे चेतना कहा जाता था। भिक्षुओं वह चेतना को कर्म कहते हैं, चेतनापूर्वक किये गये कर्म को कायिक, वाचिक और मानसिक कर्म कहा जाता है। __ प्राचीन बौद्ध सन्दर्भो में कर्म को किसी अनुवर्त मानकता का धर्म नहीं माना गया है। संयुक्त निकाय के ये वाक्य इस बात के लिए स्मरणीय हैं- कर्म अनात्मकत्व है, न यह तुम्हारा है, न औरों का है, केवल पुराना कर्म है, जीव और शरीर को एक मानने से ब्रह्मचर्यवास नहीं होता, न भिन्न मानने से, यह अनापकृत और न परकृत' हेतु के सहारे उत्पन्न हुआ है, हेतु न रहने पर निरुद्ध हो जायेगा।
सर्वप्रथम बुद्ध ने नैतिक कार्यों पर बल दिया। मनुष्य के पाप-पुण्य उसके अच्छे कर्म या बुरे कर्मों पर आधारित होता है। लेकिन प्रत्येक कार्य तृष्णा के फलस्वरूप ही होता है। भगवान बुद्ध इच्छा द्वारा किये गये कर्म को ही फलदायक मानते हैं। बिना इच्छा के किया गया कर्म का दण्ड या पुरस्कार नहीं मिलेगा। बौद्ध दर्शनिक तृष्णा से किये गये कार्य को ही फलप्रदान करने वाला कर्म मानते हैं। मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है उसका दण्ड या पुरस्कार उसके अधिकार में नहीं है। बुद्ध का विचार था कि “चेतनम् भिक्खवे, कम्मम् बदामि, चेतयित्वा करोति काया वाक्या मनसा" अर्थात् चेतना कर्म है, चेतना से युक्त कार्य, वाक् और मानसिक कर्म ही कर्म है। बौद्ध दर्शन में मनुष्य के द्वारा किया तृष्णा से युक्त कार्य की मान्य है। इस कर्म का दण्ड या पुरस्कार हो सकता है। बौद्ध दर्शन में तृष्णा मानव जीवन के अत्थान व पतन के लिए उत्तरदायी माना गया है। जीवन में तृष्णा का होना भी आवश्यक माना गया है क्योंकि मनुष्य बिना तृष्णा के कोई कर्म नहीं करता है। मानसिक कार्य का फल अच्छा बुरा जो भी हो, उस जीव को भोगना पड़ता है जैसे रथ खींचने वाले सारथि का अनुसरण रथ का पहिया करता है। पाप-पुण्य सब चित्त के