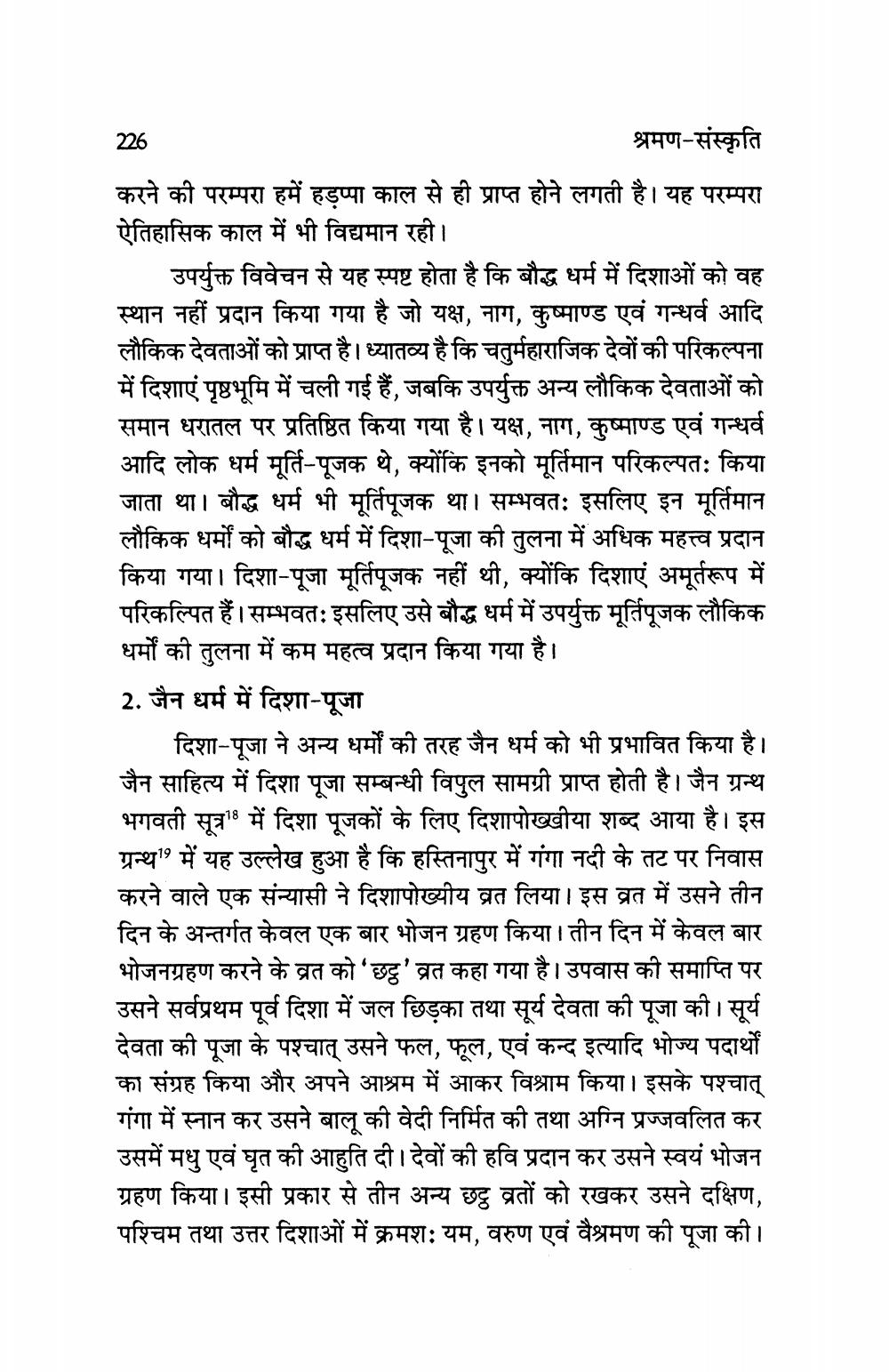________________
26
श्रमण-संस्कृति करने की परम्परा हमें हड़प्पा काल से ही प्राप्त होने लगती है। यह परम्परा ऐतिहासिक काल में भी विद्यमान रही।
उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट होता है कि बौद्ध धर्म में दिशाओं को वह स्थान नहीं प्रदान किया गया है जो यक्ष, नाग, कुष्माण्ड एवं गन्धर्व आदि लौकिक देवताओं को प्राप्त है। ध्यातव्य है कि चतुर्महाराजिक देवों की परिकल्पना में दिशाएं पृष्ठभूमि में चली गई हैं, जबकि उपर्युक्त अन्य लौकिक देवताओं को समान धरातल पर प्रतिष्ठित किया गया है। यक्ष, नाग, कुष्माण्ड एवं गन्धर्व आदि लोक धर्म मूर्ति-पूजक थे, क्योंकि इनको मूर्तिमान परिकल्पतः किया जाता था। बौद्ध धर्म भी मूर्तिपूजक था। सम्भवतः इसलिए इन मूर्तिमान लौकिक धर्मों को बौद्ध धर्म में दिशा-पूजा की तुलना में अधिक महत्त्व प्रदान किया गया। दिशा-पूजा मूर्तिपूजक नहीं थी, क्योंकि दिशाएं अमूर्तरूप में परिकल्पित हैं। सम्भवतः इसलिए उसे बौद्ध धर्म में उपर्युक्त मूर्तिपूजक लौकिक धर्मों की तुलना में कम महत्व प्रदान किया गया है। 2. जैन धर्म में दिशा-पूजा
दिशा-पूजा ने अन्य धर्मों की तरह जैन धर्म को भी प्रभावित किया है। जैन साहित्य में दिशा पूजा सम्बन्धी विपुल सामग्री प्राप्त होती है। जैन ग्रन्थ भगवती सूत्र में दिशा पूजकों के लिए दिशापोख्खीया शब्द आया है। इस ग्रन्था में यह उल्लेख हुआ है कि हस्तिनापुर में गंगा नदी के तट पर निवास करने वाले एक संन्यासी ने दिशापोख्यीय व्रत लिया। इस व्रत में उसने तीन दिन के अन्तर्गत केवल एक बार भोजन ग्रहण किया। तीन दिन में केवल बार भोजनग्रहण करने के व्रत को 'छ?' व्रत कहा गया है। उपवास की समाप्ति पर उसने सर्वप्रथम पूर्व दिशा में जल छिड़का तथा सूर्य देवता की पूजा की। सूर्य देवता की पूजा के पश्चात् उसने फल, फूल, एवं कन्द इत्यादि भोज्य पदार्थों का संग्रह किया और अपने आश्रम में आकर विश्राम किया। इसके पश्चात् गंगा में स्नान कर उसने बालू की वेदी निर्मित की तथा अग्नि प्रज्जवलित कर उसमें मधु एवं घृत की आहुति दी। देवों की हवि प्रदान कर उसने स्वयं भोजन ग्रहण किया। इसी प्रकार से तीन अन्य छट्ठ व्रतों को रखकर उसने दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिशाओं में क्रमशः यम, वरुण एवं वैश्रमण की पूजा की।