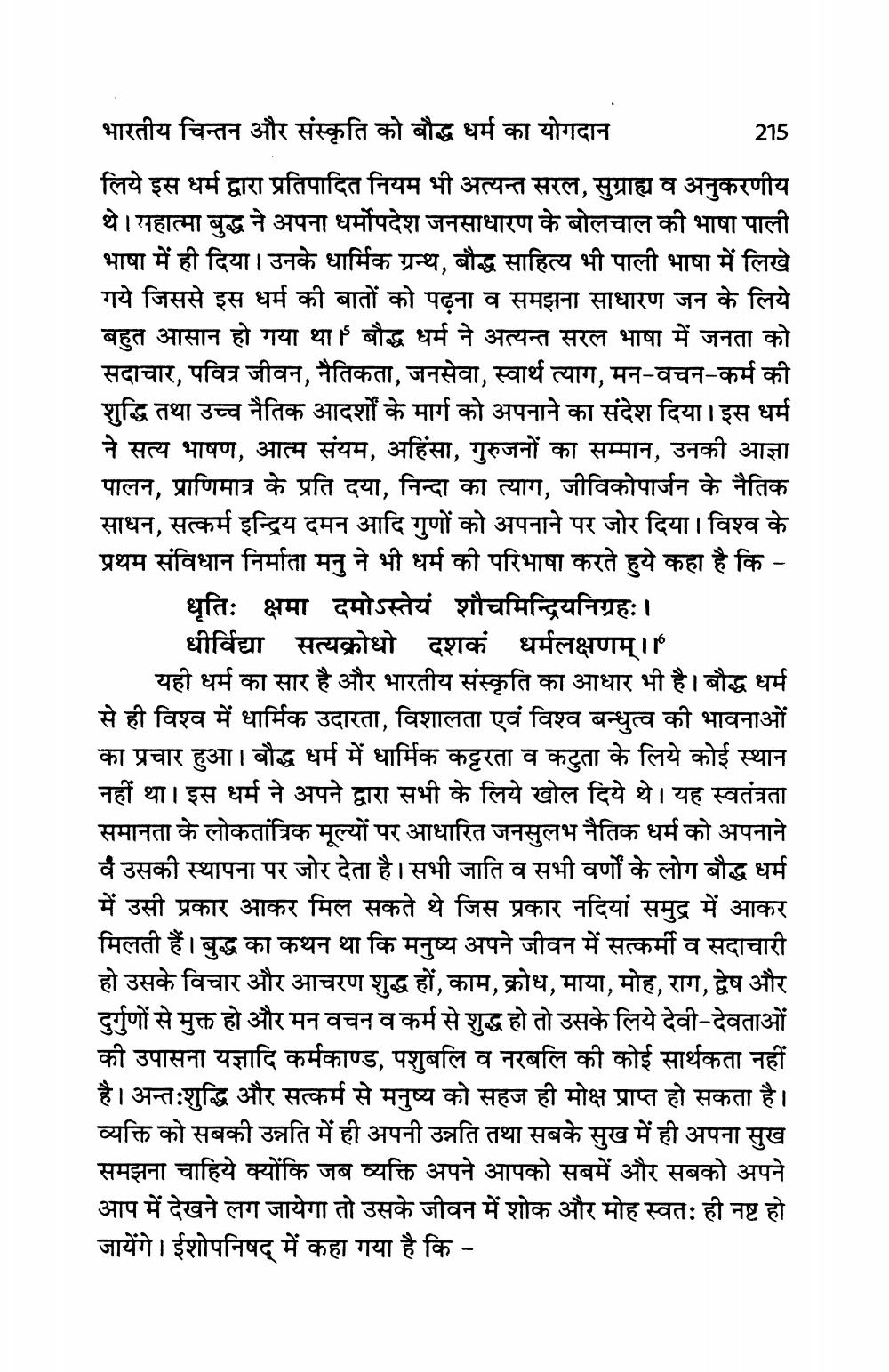________________
भारतीय चिन्तन और संस्कृति को बौद्ध धर्म का योगदान
लिये इस धर्म द्वारा प्रतिपादित नियम भी अत्यन्त सरल, सुग्राह्य व अनुकरणीय थे। यहात्मा बुद्ध ने अपना धर्मोपदेश जनसाधारण के बोलचाल की भाषा पाली भाषा में ही दिया । उनके धार्मिक ग्रन्थ, बौद्ध साहित्य भी पाली भाषा में लिखे गये जिससे इस धर्म की बातों को पढ़ना व समझना साधारण जन के लिये बहुत आसान हो गया था। बौद्ध धर्म ने अत्यन्त सरल भाषा में जनता को सदाचार, पवित्र जीवन, नैतिकता, जनसेवा, स्वार्थ त्याग, मन-वचन-कर्म की शुद्धि तथा उच्च नैतिक आदर्शों के मार्ग को अपनाने का संदेश दिया। इस धर्म ने सत्य भाषण, आत्म संयम, अहिंसा, गुरुजनों का सम्मान, उनकी आज्ञा पालन, प्राणिमात्र के प्रति दया, निन्दा का त्याग, जीविकोपार्जन के नैतिक साधन, सत्कर्म इन्द्रिय दमन आदि गुणों को अपनाने पर जोर दिया। विश्व के प्रथम संविधान निर्माता मनु ने भी धर्म की परिभाषा करते हुये कहा है कि धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः । धीर्विद्या सत्यक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥'
यही धर्म का सार है और भारतीय संस्कृति का आधार भी है । बौद्ध धर्म से ही विश्व में धार्मिक उदारता, विशालता एवं विश्व बन्धुत्व की भावनाओं का प्रचार हुआ। बौद्ध धर्म में धार्मिक कट्टरता व कटुता के लिये कोई स्थान नहीं था । इस धर्म ने अपने द्वारा सभी के लिये खोल दिये थे । यह स्वतंत्रता समानता के लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित जनसुलभ नैतिक धर्म को अपनाने व उसकी स्थापना पर जोर देता है। सभी जाति व सभी वर्गों के लोग बौद्ध धर्म में उसी प्रकार आकर मिल सकते थे जिस प्रकार नदियां समुद्र में आकर मिलती हैं । बुद्ध का कथन था कि मनुष्य अपने जीवन में सत्कर्मी व सदाचारी हो उसके विचार और आचरण शुद्ध हों, काम, क्रोध, माया, मोह, राग, द्वेष और दुर्गुणों से मुक्त हो और मन वचन व कर्म से शुद्ध हो तो उसके लिये देवी-देवताओं की उपासना यज्ञादि कर्मकाण्ड, पशुबलि व नरबलि की कोई सार्थकता नहीं है । अन्तःशुद्धि और सत्कर्म से मनुष्य को सहज ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है। व्यक्ति को सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति तथा सबके सुख में ही अपना सुख समझना चाहिये क्योंकि जब व्यक्ति अपने आपको सबमें और सबको अपने आप में देखने लग जायेगा तो उसके जीवन में शोक और मोह स्वतः ही नष्ट हो जायेंगे। ईशोपनिषद् में कहा गया है कि
215