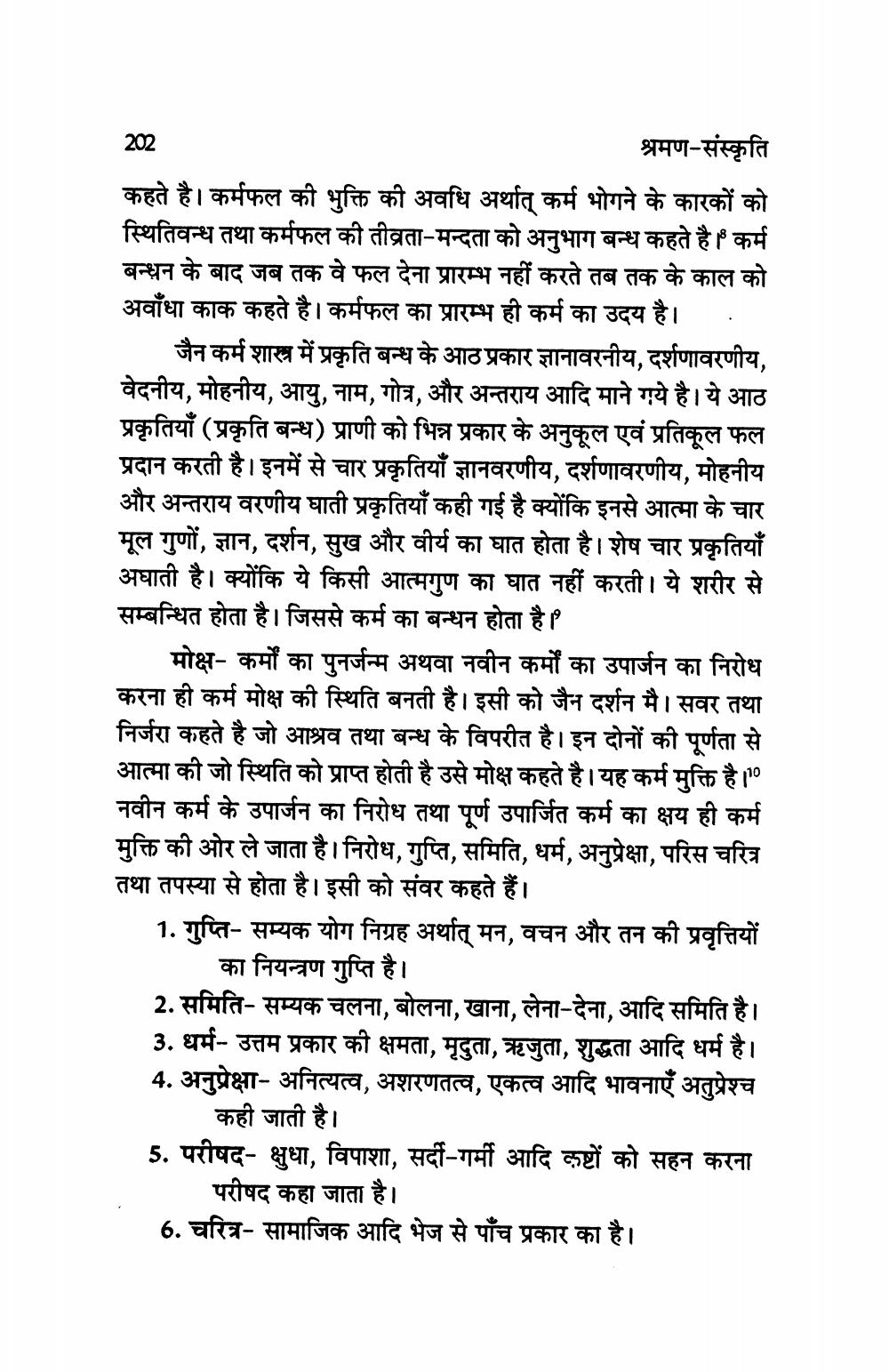________________
श्रमण-संस्कृति कहते है। कर्मफल की भुक्ति की अवधि अर्थात् कर्म भोगने के कारकों को स्थितिवन्ध तथा कर्मफल की तीव्रता-मन्दता को अनुभाग बन्ध कहते है। कर्म बन्धन के बाद जब तक वे फल देना प्रारम्भ नहीं करते तब तक के काल को अवाँधा काक कहते है। कर्मफल का प्रारम्भ ही कर्म का उदय है। .
जैन कर्म शास्त्र में प्रकृति बन्ध के आठ प्रकार ज्ञानावरनीय, दर्शणावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, और अन्तराय आदि माने गये है। ये आठ प्रकृतियाँ (प्रकृति बन्ध) प्राणी को भिन्न प्रकार के अनुकूल एवं प्रतिकूल फल प्रदान करती है। इनमें से चार प्रकृतियाँ ज्ञानवरणीय, दर्शणावरणीय, मोहनीय
और अन्तराय वरणीय घाती प्रकृतियाँ कही गई है क्योंकि इनसे आत्मा के चार मूल गुणों, ज्ञान, दर्शन, सुख और वीर्य का घात होता है। शेष चार प्रकृतियाँ अघाती है। क्योंकि ये किसी आत्मगुण का घात नहीं करती। ये शरीर से सम्बन्धित होता है। जिससे कर्म का बन्धन होता है।
मोक्ष- कर्मों का पुनर्जन्म अथवा नवीन कर्मों का उपार्जन का निरोध करना ही कर्म मोक्ष की स्थिति बनती है। इसी को जैन दर्शन मै। सवर तथा निर्जरा कहते है जो आश्रव तथा बन्ध के विपरीत है। इन दोनों की पूर्णता से आत्मा की जो स्थिति को प्राप्त होती है उसे मोक्ष कहते है। यह कर्म मुक्ति है।" नवीन कर्म के उपार्जन का निरोध तथा पूर्ण उपार्जित कर्म का क्षय ही कर्म मुक्ति की ओर ले जाता है। निरोध, गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिस चरित्र तथा तपस्या से होता है। इसी को संवर कहते हैं। 1. गुप्ति- सम्यक योग निग्रह अर्थात् मन, वचन और तन की प्रवृत्तियों
का नियन्त्रण गुप्ति है। 2. समिति- सम्यक चलना, बोलना, खाना, लेना-देना, आदि समिति है। 3. धर्म- उत्तम प्रकार की क्षमता, मृदुता, ऋजुता, शुद्धता आदि धर्म है। 4. अनुप्रेक्षा- अनित्यत्व, अशरणतत्व, एकत्व आदि भावनाएँ अतुप्रेश्च
कही जाती है। 5. परीषद- क्षुधा, विपाशा, सर्दी-गर्मी आदि कष्टों को सहन करना
परीषद कहा जाता है। 6. चरित्र- सामाजिक आदि भेज से पाँच प्रकार का है।