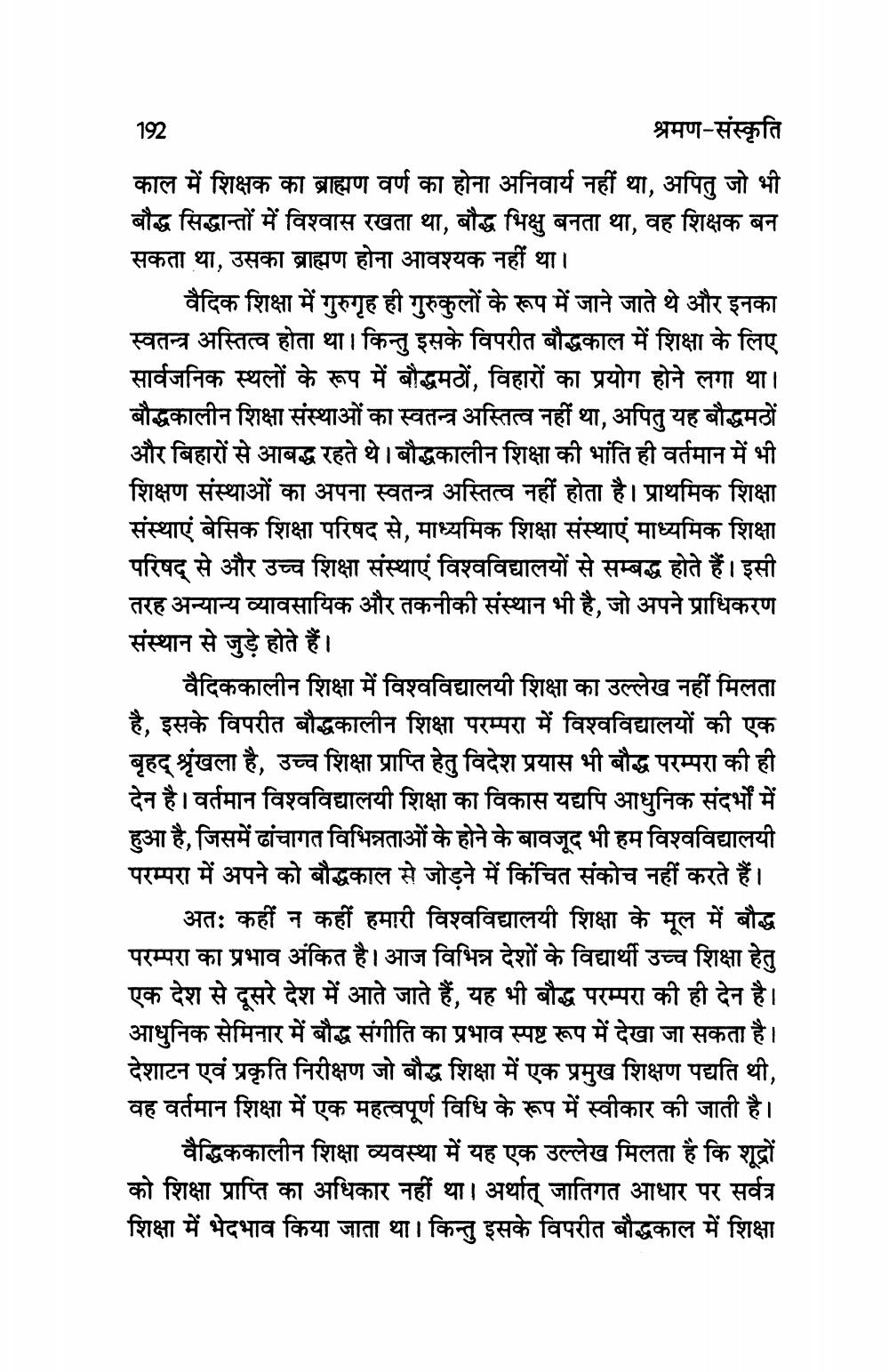________________
192
श्रमण-संस्कृति काल में शिक्षक का ब्राह्मण वर्ण का होना अनिवार्य नहीं था, अपितु जो भी बौद्ध सिद्धान्तों में विश्वास रखता था, बौद्ध भिक्षु बनता था, वह शिक्षक बन सकता था, उसका ब्राह्मण होना आवश्यक नहीं था।
वैदिक शिक्षा में गुरुगृह ही गुरुकुलों के रूप में जाने जाते थे और इनका स्वतन्त्र अस्तित्व होता था। किन्तु इसके विपरीत बौद्धकाल में शिक्षा के लिए सार्वजनिक स्थलों के रूप में बौद्धमठों, विहारों का प्रयोग होने लगा था। बौद्धकालीन शिक्षा संस्थाओं का स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं था, अपितु यह बौद्धमठों
और बिहारों से आबद्ध रहते थे। बौद्धकालीन शिक्षा की भांति ही वर्तमान में भी शिक्षण संस्थाओं का अपना स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं होता है। प्राथमिक शिक्षा संस्थाएं बेसिक शिक्षा परिषद से, माध्यमिक शिक्षा संस्थाएं माध्यमिक शिक्षा परिषद् से और उच्च शिक्षा संस्थाएं विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध होते हैं। इसी तरह अन्यान्य व्यावसायिक और तकनीकी संस्थान भी है, जो अपने प्राधिकरण संस्थान से जुड़े होते हैं।
वैदिककालीन शिक्षा में विश्वविद्यालयी शिक्षा का उल्लेख नहीं मिलता है, इसके विपरीत बौद्धकालीन शिक्षा परम्परा में विश्वविद्यालयों की एक बृहद् श्रृंखला है, उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु विदेश प्रयास भी बौद्ध परम्परा की ही देन है। वर्तमान विश्वविद्यालयी शिक्षा का विकास यद्यपि आधुनिक संदर्भो में हुआ है, जिसमें ढांचागत विभिन्नताओं के होने के बावजूद भी हम विश्वविद्यालयी परम्परा में अपने को बौद्धकाल से जोड़ने में किंचित संकोच नहीं करते हैं। ___ अतः कहीं न कहीं हमारी विश्वविद्यालयी शिक्षा के मूल में बौद्ध परम्परा का प्रभाव अंकित है। आज विभिन्न देशों के विद्यार्थी उच्च शिक्षा हेतु एक देश से दूसरे देश में आते जाते हैं, यह भी बौद्ध परम्परा की ही देन है। आधुनिक सेमिनार में बौद्ध संगीति का प्रभाव स्पष्ट रूप में देखा जा सकता है। देशाटन एवं प्रकृति निरीक्षण जो बौद्ध शिक्षा में एक प्रमुख शिक्षण पद्यति थी, वह वर्तमान शिक्षा में एक महत्वपूर्ण विधि के रूप में स्वीकार की जाती है।
वैद्धिककालीन शिक्षा व्यवस्था में यह एक उल्लेख मिलता है कि शूद्रों को शिक्षा प्राप्ति का अधिकार नहीं था। अर्थात् जातिगत आधार पर सर्वत्र शिक्षा में भेदभाव किया जाता था। किन्तु इसके विपरीत बौद्धकाल में शिक्षा