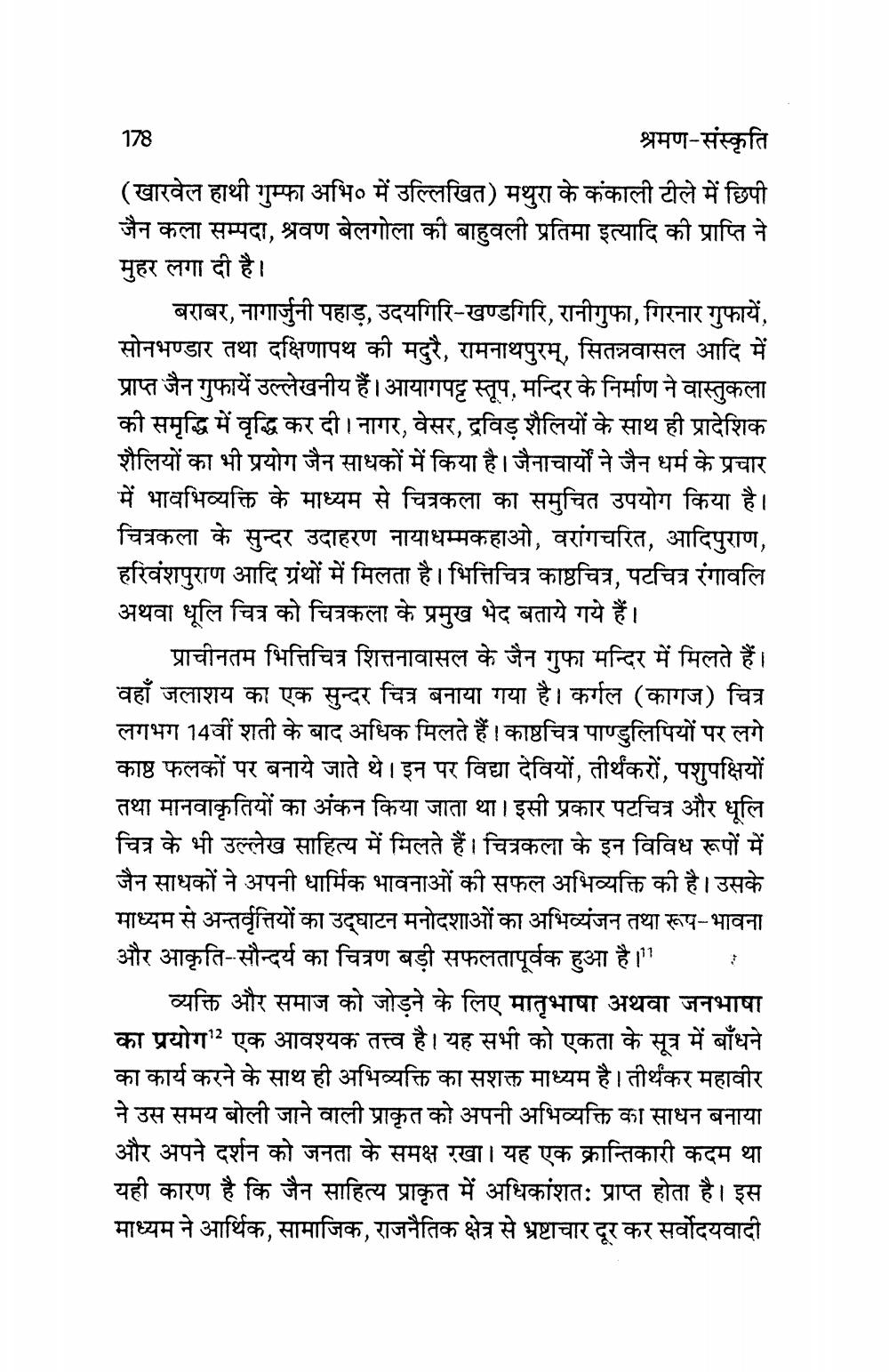________________
178
श्रमण-संस्कृति (खारवेल हाथी गुम्फा अभि० में उल्लिखित) मथुरा के कंकाली टीले में छिपी जैन कला सम्पदा, श्रवण बेलगोला की बाहुवली प्रतिमा इत्यादि की प्राप्ति ने मुहर लगा दी है।
बराबर, नागार्जुनी पहाड़, उदयगिरि-खण्डगिरि, रानीगुफा, गिरनार गुफायें, सोनभण्डार तथा दक्षिणापथ की मदुरै, रामनाथपुरम्, सितन्नवासल आदि में प्राप्त जैन गुफायें उल्लेखनीय हैं। आयागपट्ट स्तूप, मन्दिर के निर्माण ने वास्तुकला की समृद्धि में वृद्धि कर दी। नागर, वेसर, द्रविड़ शैलियों के साथ ही प्रादेशिक शैलियों का भी प्रयोग जैन साधकों में किया है। जैनाचार्यों ने जैन धर्म के प्रचार में भावभिव्यक्ति के माध्यम से चित्रकला का समुचित उपयोग किया है। चित्रकला के सुन्दर उदाहरण नायाधम्मकहाओ, वरांगचरित, आदिपुराण, हरिवंशपुराण आदि ग्रंथों में मिलता है। भित्तिचित्र काष्ठचित्र, पटचित्र रंगावलि अथवा धूलि चित्र को चित्रकला के प्रमुख भेद बताये गये हैं।
प्राचीनतम भित्तिचित्र शित्तनावासल के जैन गुफा मन्दिर में मिलते हैं। वहाँ जलाशय का एक सुन्दर चित्र बनाया गया है। कर्गल (कागज) चित्र लगभग 14वीं शती के बाद अधिक मिलते हैं। काष्ठचित्र पाण्डुलिपियों पर लगे काष्ठ फलकों पर बनाये जाते थे। इन पर विद्या देवियों, तीर्थंकरों, पशुपक्षियों तथा मानवाकृतियों का अंकन किया जाता था। इसी प्रकार पटचित्र और धूलि चित्र के भी उल्लेख साहित्य में मिलते हैं। चित्रकला के इन विविध रूपों में जैन साधकों ने अपनी धार्मिक भावनाओं की सफल अभिव्यक्ति की है। उसके माध्यम से अन्तर्वृत्तियों का उद्घाटन मनोदशाओं का अभिव्यंजन तथा रूप-भावना और आकृति-सौन्दर्य का चित्रण बड़ी सफलतापूर्वक हुआ है।"
व्यक्ति और समाज को जोड़ने के लिए मातृभाषा अथवा जनभाषा का प्रयोग एक आवश्यक तत्त्व है। यह सभी को एकता के सूत्र में बाँधने का कार्य करने के साथ ही अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है। तीर्थंकर महावीर ने उस समय बोली जाने वाली प्राकृत को अपनी अभिव्यक्ति का साधन बनाया
और अपने दर्शन को जनता के समक्ष रखा। यह एक क्रान्तिकारी कदम था यही कारण है कि जैन साहित्य प्राकृत में अधिकांशतः प्राप्त होता है। इस माध्यम ने आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्र से भ्रष्टाचार दूर कर सर्वोदयवादी