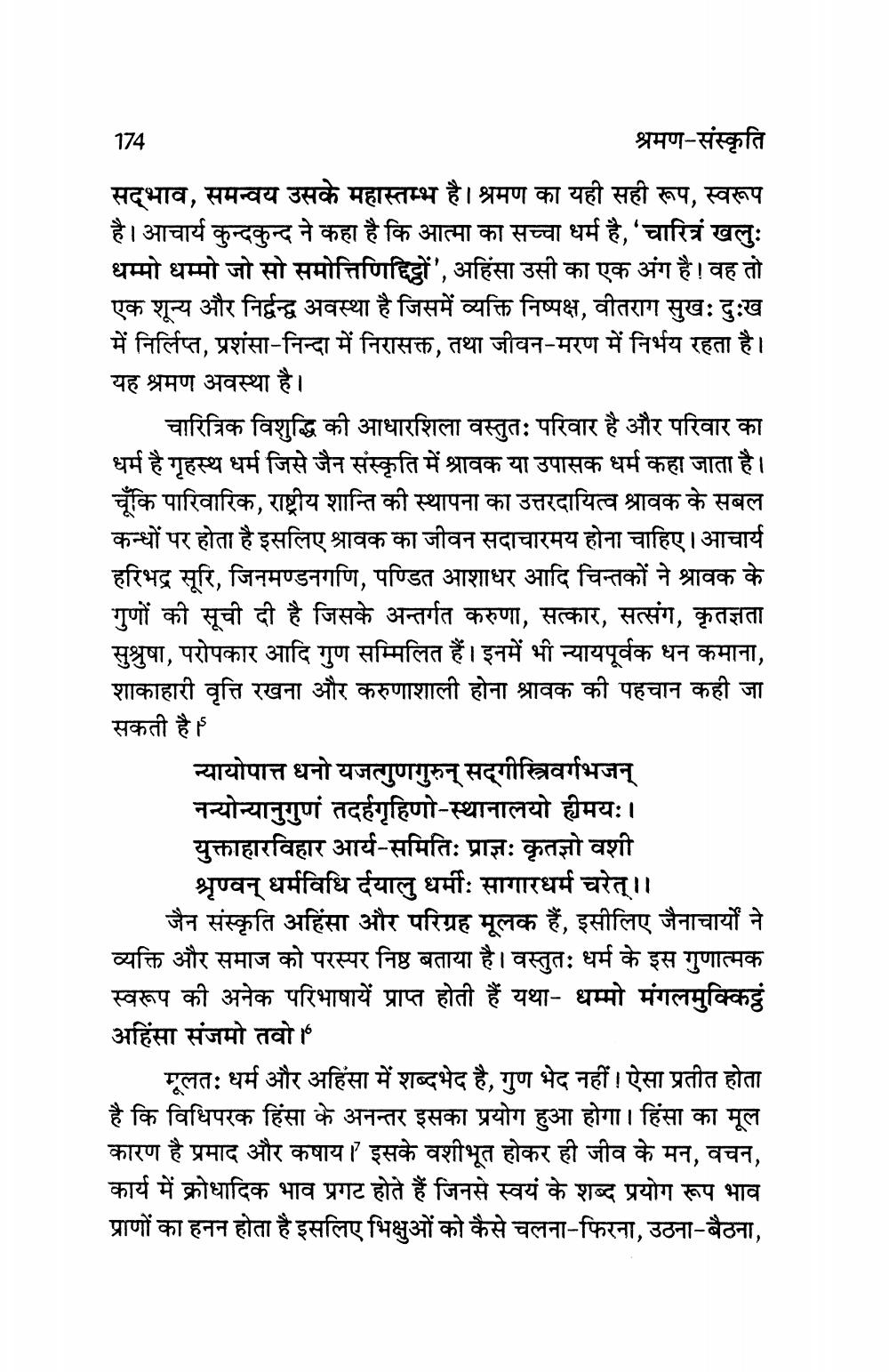________________
174
श्रमण-संस्कृति
सद्भाव, समन्वय उसके महास्तम्भ है। श्रमण का यही सही रूप, स्वरूप है। आचार्य कुन्दकुन्द ने कहा है कि आत्मा का सच्चा धर्म है, 'चारित्रं खलुः धम्मो धम्मो जो सो समोत्तिणिद्रिों', अहिंसा उसी का एक अंग है। वह तो एक शून्य और निर्द्वन्द्व अवस्था है जिसमें व्यक्ति निष्पक्ष, वीतराग सुखः दुःख में निर्लिप्त, प्रशंसा-निन्दा में निरासक्त, तथा जीवन-मरण में निर्भय रहता है। यह श्रमण अवस्था है।
चारित्रिक विशुद्धि की आधारशिला वस्तुतः परिवार है और परिवार का धर्म है गृहस्थ धर्म जिसे जैन संस्कृति में श्रावक या उपासक धर्म कहा जाता है। चूँकि पारिवारिक, राष्ट्रीय शान्ति की स्थापना का उत्तरदायित्व श्रावक के सबल कन्धों पर होता है इसलिए श्रावक का जीवन सदाचारमय होना चाहिए। आचार्य हरिभद्र सूरि, जिनमण्डनगणि, पण्डित आशाधर आदि चिन्तकों ने श्रावक के गुणों की सूची दी है जिसके अन्तर्गत करुणा, सत्कार, सत्संग, कृतज्ञता सुश्रुषा, परोपकार आदि गुण सम्मिलित हैं। इनमें भी न्यायपूर्वक धन कमाना, शाकाहारी वृत्ति रखना और करुणाशाली होना श्रावक की पहचान कही जा सकती है।
न्यायोपात्त धनो यजत्गुणगुरुन् सद्गीस्त्रिवर्गभजन् नन्योन्यानुगुणं तदर्हगृहिणो-स्थानालयो हीमयः । युक्ताहारविहार आर्य-समितिः प्राज्ञः कृतज्ञो वशी
श्रृण्वन् धर्मविधि दयालु धर्मीः सागारधर्म चरेत्।।
जैन संस्कृति अहिंसा और परिग्रह मूलक हैं, इसीलिए जैनाचार्यों ने व्यक्ति और समाज को परस्पर निष्ठ बताया है। वस्तुतः धर्म के इस गुणात्मक स्वरूप की अनेक परिभाषायें प्राप्त होती हैं यथा- धम्मो मंगलमुक्किट्ठ अहिंसा संजमो तवो।
मूलतः धर्म और अहिंसा में शब्दभेद है, गुण भेद नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि विधिपरक हिंसा के अनन्तर इसका प्रयोग हुआ होगा। हिंसा का मूल कारण है प्रमाद और कषाय। इसके वशीभूत होकर ही जीव के मन, वचन, कार्य में क्रोधादिक भाव प्रगट होते हैं जिनसे स्वयं के शब्द प्रयोग रूप भाव प्राणों का हनन होता है इसलिए भिक्षुओं को कैसे चलना-फिरना, उठना-बैठना,