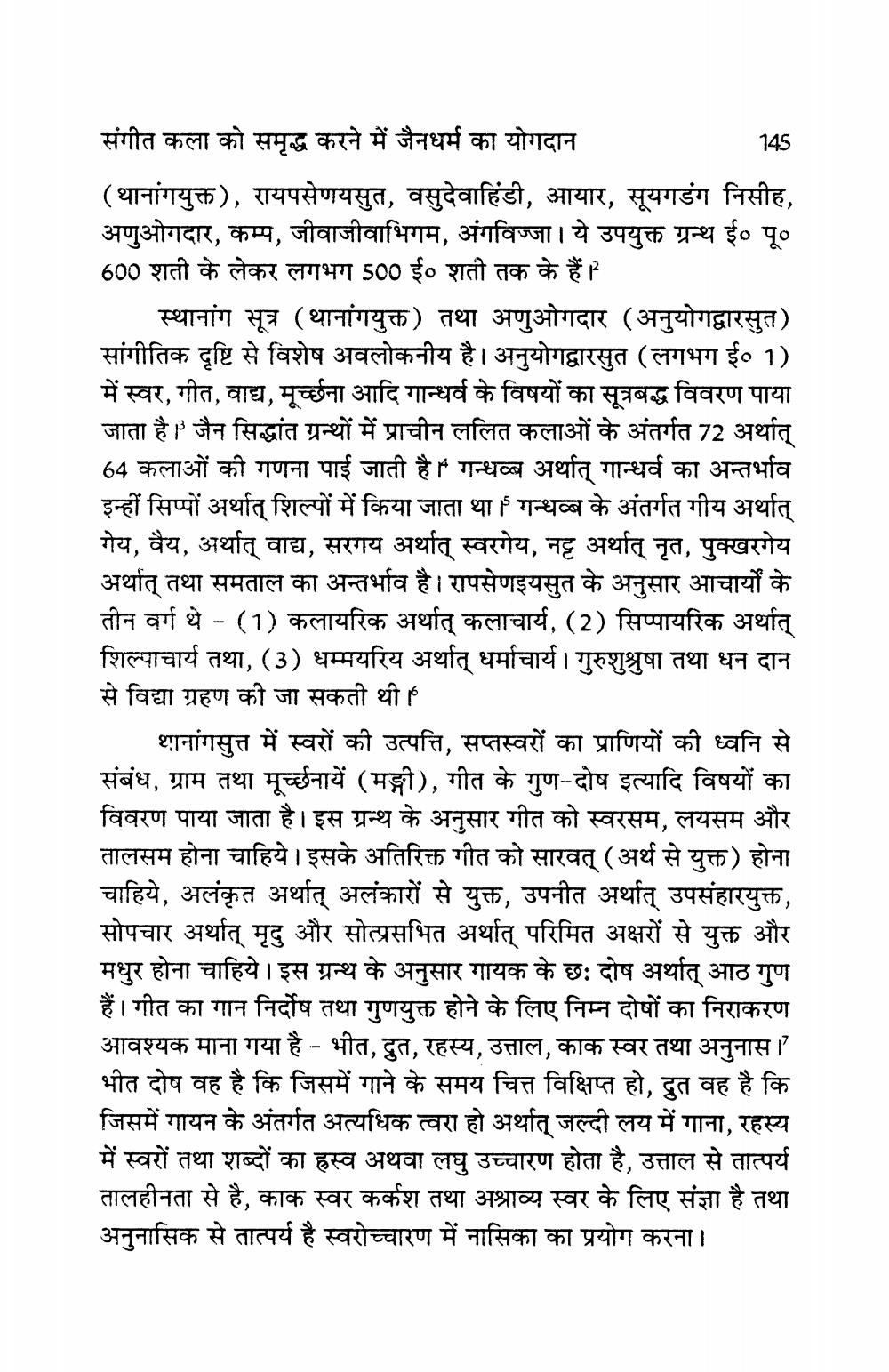________________
संगीत कला को समृद्ध करने में जैनधर्म का योगदान
145
(थानांगयुक्त), रायपसेणयसुत, वसुदेवाहिंडी, आयार, सूयगडंग निसीह, अणुओगदार, कम्प, जीवाजीवाभिगम, अंगविज्जा । ये उपयुक्त ग्रन्थ ई० पू० 600 शती के लेकर लगभग 500 ई० शती तक के हैं ।
1
स्थानांग सूत्र (थानांगयुक्त) तथा अणुओगदार ( अनुयोगद्वारसुत) सांगीतिक दृष्टि से विशेष अवलोकनीय है। अनुयोगद्वारसुत (लगभग ई० 1 ) में स्वर, गीत, वाद्य, मूर्च्छना आदि गान्धर्व के विषयों का सूत्रबद्ध विवरण पाया जाता है। जैन सिद्धांत ग्रन्थों में प्राचीन ललित कलाओं के अंतर्गत 72 अर्थात् 64 कलाओं की गणना पाई जाती है । गन्धव्ब अर्थात् गान्धर्व का अन्तर्भाव इन्हीं सिप्पों अर्थात् शिल्पों में किया जाता था । गन्धव्ब के अंतर्गत गीय अर्थात् गेय, वैय, अर्थात् वाद्य, सरगय अर्थात् स्वरगेय, नट्ट अर्थात् नृत, पुक्खरगेय अर्थात् तथा समताल का अन्तर्भाव है । रापसेणइयसुत के अनुसार आचार्यों के तीन वर्ग थे (1) कलायरिक अर्थात् कलाचार्य, (2) सिप्पायरिक अर्थात् शिल्पाचार्य तथा, (3) धम्मयरिय अर्थात् धर्माचार्य । गुरुशुश्रुषा तथा धन दान से विद्या ग्रहण की जा सकती थी ।
थानांगसुत्त में स्वरों की उत्पत्ति, सप्तस्वरों का प्राणियों की ध्वनि से संबंध, ग्राम तथा मूर्च्छनायें (मङ्गी), गीत के गुण-दोष इत्यादि विषयों का विवरण पाया जाता है। इस ग्रन्थ के अनुसार गीत को स्वरसम, लयसम और तालसम होना चाहिये । इसके अतिरिक्त गीत को सारवत् (अर्थ से युक्त) होना चाहिये, अलंकृत अर्थात् अलंकारों से युक्त, उपनीत अर्थात् उपसंहारयुक्त, सोपचार अर्थात् मृदु और सोत्प्रसभित अर्थात् परिमित अक्षरों से युक्त और मधुर होना चाहिये । इस ग्रन्थ के अनुसार गायक के छः दोष अर्थात् आठ गुण हैं । गीत का गान निर्दोष तथा गुणयुक्त होने के लिए निम्न दोषों का निराकरण आवश्यक माना गया है- भीत, द्रुत, रहस्य, उत्ताल, काक स्वर तथा अनुनास ।' भीत दोष वह है कि जिसमें गाने के समय चित्त विक्षिप्त हो, द्रुत वह है कि जिसमें गायन के अंतर्गत अत्यधिक त्वरा हो अर्थात् जल्दी लय में गाना, रहस्य में स्वरों तथा शब्दों का ह्रस्व अथवा लघु उच्चारण होता है, उत्ताल से तात्पर्य तालहीनता से है, काक स्वर कर्कश तथा अश्राव्य स्वर के लिए संज्ञा है तथा अनुनासिक से तात्पर्य है स्वरोच्चारण में नासिका का प्रयोग करना ।