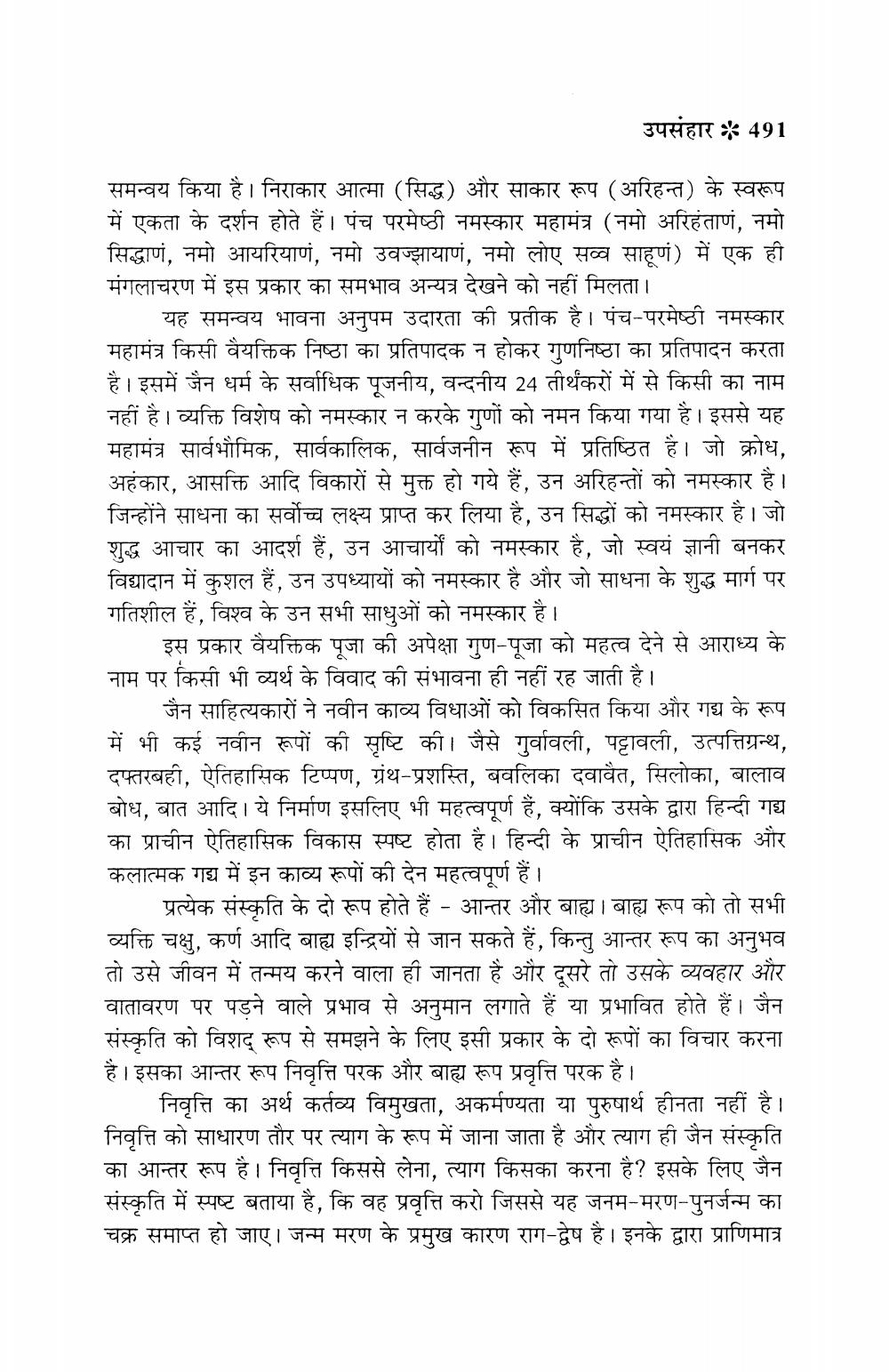________________
उपसंहार * 491
समन्वय किया है। निराकार आत्मा (सिद्ध) और साकार रूप (अरिहन्त) के स्वरूप में एकता के दर्शन होते हैं। पंच परमेष्ठी नमस्कार महामंत्र (नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोए सव्व साहूणं) में एक ही मंगलाचरण में इस प्रकार का समभाव अन्यत्र देखने को नहीं मिलता।
यह समन्वय भावना अनुपम उदारता की प्रतीक है। पंच-परमेष्ठी नमस्कार महामंत्र किसी वैयक्तिक निष्ठा का प्रतिपादक न होकर गुणनिष्ठा का प्रतिपादन करता है। इसमें जैन धर्म के सर्वाधिक पूजनीय, वन्दनीय 24 तीर्थंकरों में से किसी का नाम नहीं है। व्यक्ति विशेष को नमस्कार न करके गुणों को नमन किया गया है। इससे यह महामंत्र सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वजनीन रूप में प्रतिष्ठित है। जो क्रोध, अहंकार, आसक्ति आदि विकारों से मुक्त हो गये हैं, उन अरिहन्तों को नमस्कार है। जिन्होंने साधना का सर्वोच्च लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, उन सिद्धों को नमस्कार है। जो शुद्ध आचार का आदर्श हैं, उन आचार्यों को नमस्कार है, जो स्वयं ज्ञानी बनकर विद्यादान में कुशल हैं, उन उपध्यायों को नमस्कार है और जो साधना के शुद्ध मार्ग पर गतिशील हैं, विश्व के उन सभी साधुओं को नमस्कार है।
इस प्रकार वैयक्तिक पूजा की अपेक्षा गुण-पूजा को महत्व देने से आराध्य के नाम पर किसी भी व्यर्थ के विवाद की संभावना ही नहीं रह जाती है।
जैन साहित्यकारों ने नवीन काव्य विधाओं को विकसित किया और गद्य के रूप में भी कई नवीन रूपों की सृष्टि की। जैसे गुर्वावली, पट्टावली, उत्पत्तिग्रन्थ, दफ्तरबही, ऐतिहासिक टिप्पण, ग्रंथ-प्रशस्ति, बवलिका दवावैत, सिलोका, बालाव बोध, बात आदि। ये निर्माण इसलिए भी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उसके द्वारा हिन्दी गद्य का प्राचीन ऐतिहासिक विकास स्पष्ट होता है। हिन्दी के प्राचीन ऐतिहासिक और कलात्मक गद्य में इन काव्य रूपों की देन महत्वपूर्ण हैं।
प्रत्येक संस्कृति के दो रूप होते हैं - आन्तर और बाह्य । बाह्य रूप को तो सभी व्यक्ति चक्षु, कर्ण आदि बाह्य इन्द्रियों से जान सकते हैं, किन्तु आन्तर रूप का अनुभव तो उसे जीवन में तन्मय करने वाला ही जानता है और दूसरे तो उसके व्यवहार और वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव से अनुमान लगाते हैं या प्रभावित होते हैं। जैन संस्कृति को विशद् रूप से समझने के लिए इसी प्रकार के दो रूपों का विचार करना है। इसका आन्तर रूप निवृत्ति परक और बाह्य रूप प्रवृत्ति परक है।
निवृत्ति का अर्थ कर्तव्य विमुखता, अकर्मण्यता या पुरुषार्थ हीनता नहीं है। निवृत्ति को साधारण तौर पर त्याग के रूप में जाना जाता है और त्याग ही जैन संस्कृति का आन्तर रूप है। निवृत्ति किससे लेना, त्याग किसका करना है? इसके लिए जैन संस्कृति में स्पष्ट बताया है, कि वह प्रवृत्ति करो जिससे यह जनम-मरण-पुनर्जन्म का चक्र समाप्त हो जाए। जन्म मरण के प्रमुख कारण राग-द्वेष है। इनके द्वारा प्राणिमात्र