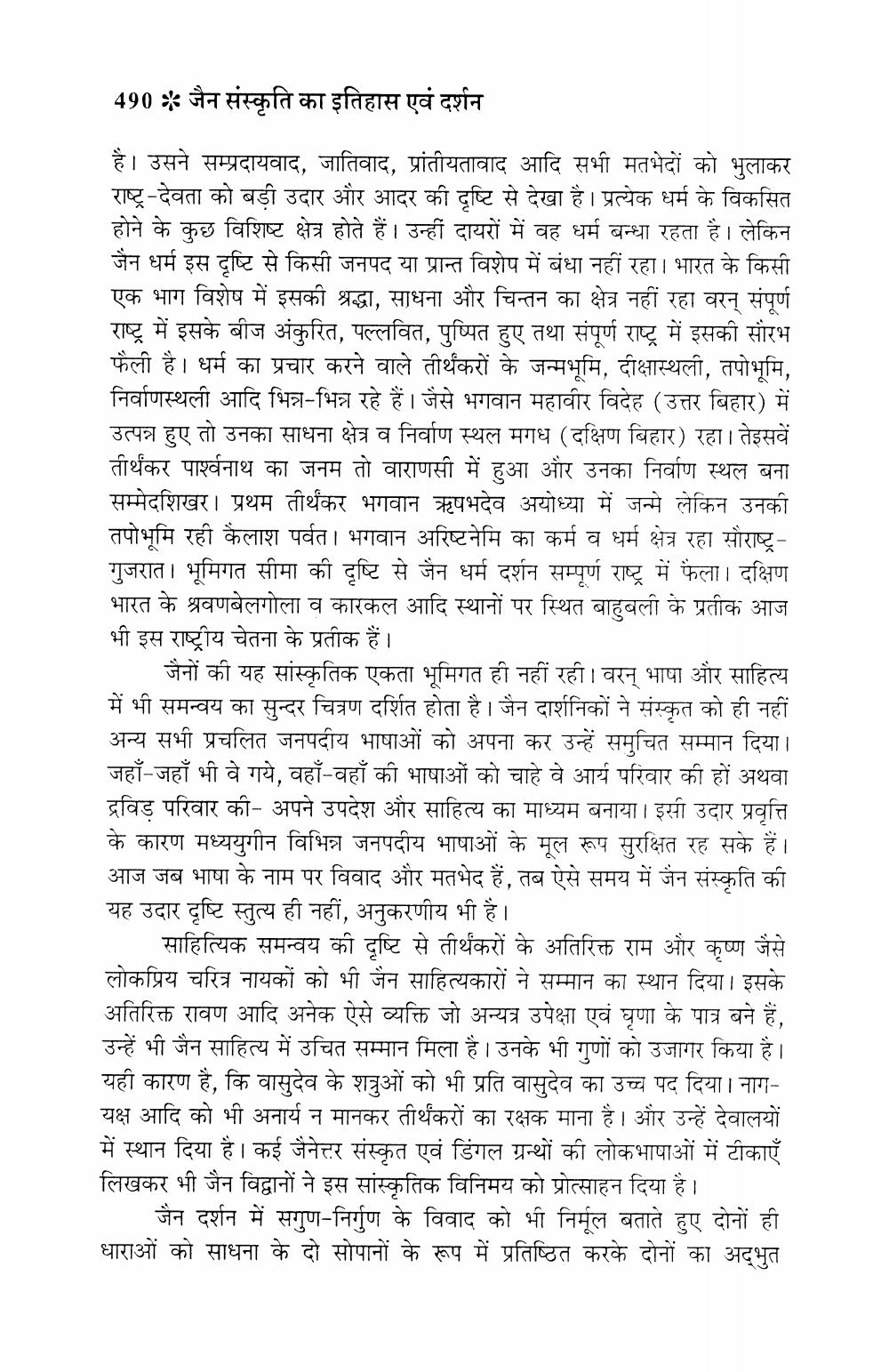________________
490 * जैन संस्कृति का इतिहास एवं दर्शन
है। उसने सम्प्रदायवाद, जातिवाद, प्रांतीयतावाद आदि सभी मतभेदों को भुलाकर राष्ट्र-देवता को बड़ी उदार और आदर की दृष्टि से देखा है। प्रत्येक धर्म के विकसित होने के कुछ विशिष्ट क्षेत्र होते हैं। उन्हीं दायरों में वह धर्म बन्धा रहता है। लेकिन जैन धर्म इस दृष्टि से किसी जनपद या प्रान्त विशेप में बंधा नहीं रहा। भारत के किसी एक भाग विशेष में इसकी श्रद्धा, साधना और चिन्तन का क्षेत्र नहीं रहा वरन् संपूर्ण राष्ट्र में इसके बीज अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित हए तथा संपूर्ण राष्ट्र में इसकी सौरभ फैली है। धर्म का प्रचार करने वाले तीर्थंकरों के जन्मभूमि, दीक्षास्थली, तपोभूमि, निर्वाणस्थली आदि भिन्न-भिन्न रहे हैं। जैसे भगवान महावीर विदेह (उत्तर बिहार) में उत्पन्न हुए तो उनका साधना क्षेत्र व निर्वाण स्थल मगध (दक्षिण बिहार) रहा। तेइसवें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जनम तो वाराणसी में हुआ और उनका निर्वाण स्थल बना सम्मेदशिखर। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव अयोध्या में जन्मे लेकिन उनकी तपोभूमि रही कैलाश पर्वत। भगवान अरिष्टनेमि का कर्म व धर्म क्षेत्र रहा सौराष्ट्रगुजरात। भूमिगत सीमा की दृष्टि से जैन धर्म दर्शन सम्पूर्ण राष्ट्र में फैला। दक्षिण भारत के श्रवणबेलगोला व कारकल आदि स्थानों पर स्थित बाहुबली के प्रतीक आज भी इस राष्ट्रीय चेतना के प्रतीक हैं।
जैनों की यह सांस्कृतिक एकता भूमिगत ही नहीं रही। वरन भाषा और साहित्य में भी समन्वय का सुन्दर चित्रण दर्शित होता है। जैन दार्शनिकों ने संस्कृत को ही नहीं अन्य सभी प्रचलित जनपदीय भाषाओं को अपना कर उन्हें समुचित सम्मान दिया। जहाँ-जहाँ भी वे गये, वहाँ-वहाँ की भाषाओं को चाहे वे आर्य परिवार की हों अथवा द्रविड़ परिवार की- अपने उपदेश और साहित्य का माध्यम बनाया। इसी उदार प्रवृत्ति के कारण मध्ययुगीन विभिन्न जनपदीय भाषाओं के मूल रूप सुरक्षित रह सके हैं। आज जब भाषा के नाम पर विवाद और मतभेद हैं, तब ऐसे समय में जैन संस्कृति की यह उदार दृष्टि स्तुत्य ही नहीं, अनुकरणीय भी है।
साहित्यिक समन्वय की दृष्टि से तीर्थंकरों के अतिरिक्त राम और कृष्ण जैसे लोकप्रिय चरित्र नायकों को भी जैन साहित्यकारों ने सम्मान का स्थान दिया। इसके अतिरिक्त रावण आदि अनेक ऐसे व्यक्ति जो अन्यत्र उपेक्षा एवं घृणा के पात्र बने हैं, उन्हें भी जैन साहित्य में उचित सम्मान मिला है। उनके भी गुणों को उजागर किया है। यही कारण है, कि वासुदेव के शत्रुओं को भी प्रति वासुदेव का उच्च पद दिया। नागयक्ष आदि को भी अनार्य न मानकर तीर्थंकरों का रक्षक माना है। और उन्हें देवालयों में स्थान दिया है। कई जैनेत्तर संस्कृत एवं डिंगल ग्रन्थों की लोकभाषाओं में टीकाएँ लिखकर भी जैन विद्वानों ने इस सांस्कृतिक विनिमय को प्रोत्साहन दिया है।
जैन दर्शन में सगुण-निर्गुण के विवाद को भी निर्मूल बताते हुए दोनों ही धाराओं को साधना के दो सोपानों के रूप में प्रतिष्ठित करके दोनों का अद्भुत