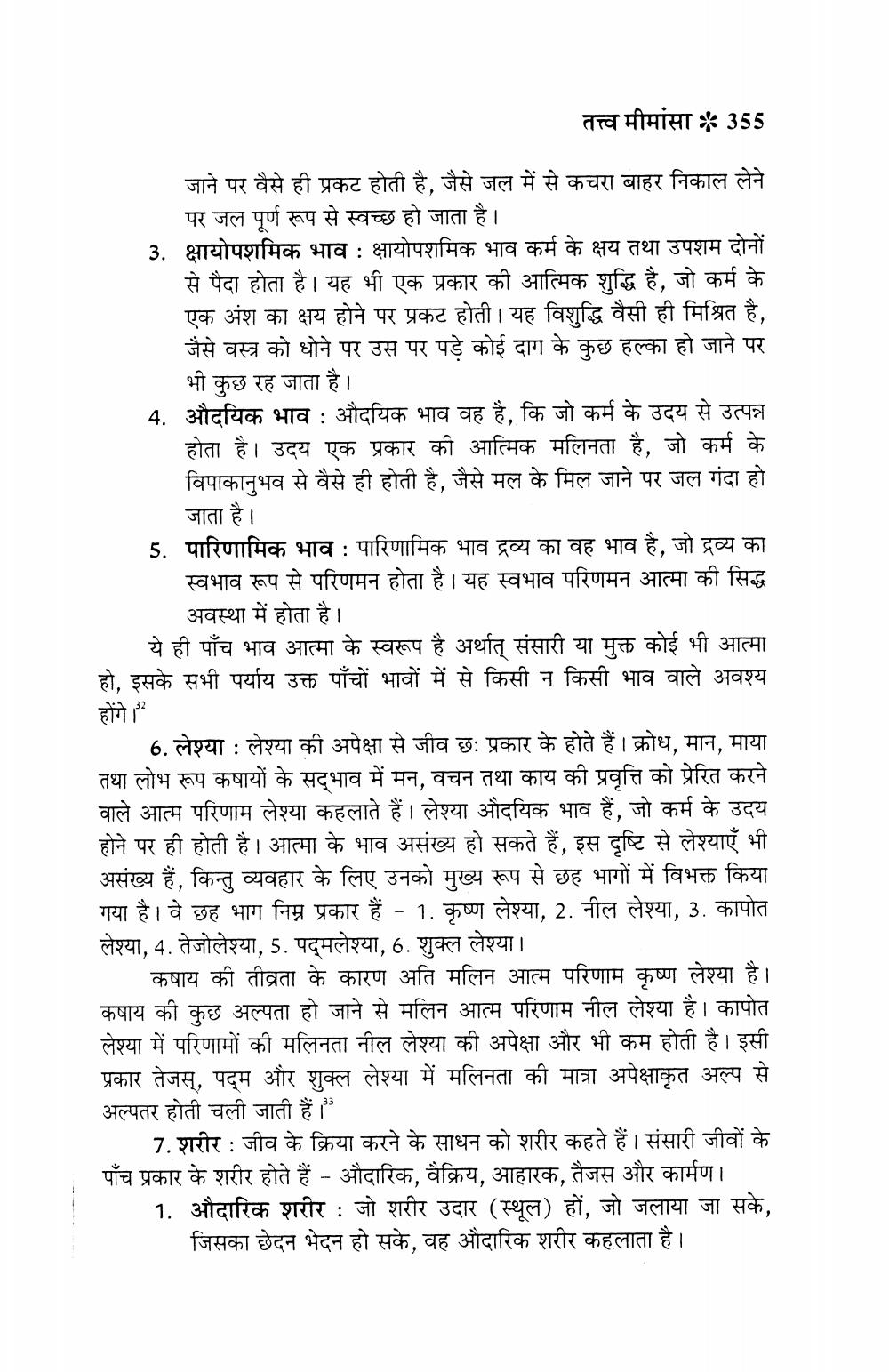________________
तत्त्वमीमांसा 355
जाने पर वैसे ही प्रकट होती है, जैसे जल में से कचरा बाहर निकाल लेने पर जल पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाता है ।
3. क्षायोपशमिक भाव : क्षायोपशमिक भाव कर्म के क्षय तथा उपशम दोनों से पैदा होता है। यह भी एक प्रकार की आत्मिक शुद्धि है, जो कर्म के एक अंश का क्षय होने पर प्रकट होती । यह विशुद्धि वैसी ही मिश्रित है, जैसे वस्त्र को धोने पर उस पर पड़े कोई दाग के कुछ हल्का हो जाने पर भी कुछ रह जाता है।
4. औदयिक भाव : औदयिक भाव वह है, कि जो कर्म के उदय से उत्पन्न होता है । उदय एक प्रकार की आत्मिक मलिनता है, जो कर्म के विपाकानुभव से वैसे ही होती है, जैसे मल के मिल जाने पर जल गंदा हो जाता है।
5. पारिणामिक भाव : पारिणामिक भाव द्रव्य का वह भाव है, जो द्रव्य का स्वभाव रूप से परिणमन होता है । यह स्वभाव परिणमन आत्मा की सिद्ध अवस्था में होता है।
ये ही पाँच भाव आत्मा के स्वरूप है अर्थात् संसारी या मुक्त कोई भी आत्मा हो, इसके सभी पर्याय उक्त पाँचों भावों में से किसी न किसी भाव वाले अवश्य होंगे। 2
6. लेश्या : लेश्या की अपेक्षा से जीव छः प्रकार के होते हैं। क्रोध, मान, माया तथा लोभ रूप कषायों के सद्भाव मन, वचन तथा काय की प्रवृत्ति को प्रेरित करने वाले आत्म परिणाम लेश्या कहलाते हैं । लेश्या औदयिक भाव हैं, जो कर्म के उदय होने पर ही होती है। आत्मा के भाव असंख्य हो सकते हैं, इस दृष्टि से लेश्याएँ भी असंख्य हैं, किन्तु व्यवहार के लिए उनको मुख्य रूप से छह भागों में विभक्त किया गया है। वे छह भाग निम्न प्रकार हैं 1. कृष्ण लेश्या, 2. नील लेश्या, 3. कापोत लेश्या, 4. तेजोलेश्या, 5. पद्मलेश्या, 6. शुक्ल लेश्या ।
कषाय की तीव्रता के कारण अति मलिन आत्म परिणाम कृष्ण लेश्या है। कषाय की कुछ अल्पता हो जाने से मलिन आत्म परिणाम नील लेश्या है । कापोत लेश्या में परिणामों की मलिनता नील लेश्या की अपेक्षा और भी कम होती है। इसी प्रकार तेजस्, पद्म और शुक्ल लेश्या में मलिनता की मात्रा अपेक्षाकृत अल्प से अल्पतर होती चली जाती हैं।
7. शरीर : जीव के क्रिया करने के साधन को शरीर कहते हैं । संसारी जीवों के पाँच प्रकार के शरीर होते हैं- औदारिक, वैक्रिय, आहारक, तैजस और कार्मण ।
1. औदारिक शरीर : जो शरीर उदार (स्थूल) हों, जो जलाया जा सके, जिसका छेदन भेदन हो सके, वह औदारिक शरीर कहलाता है ।