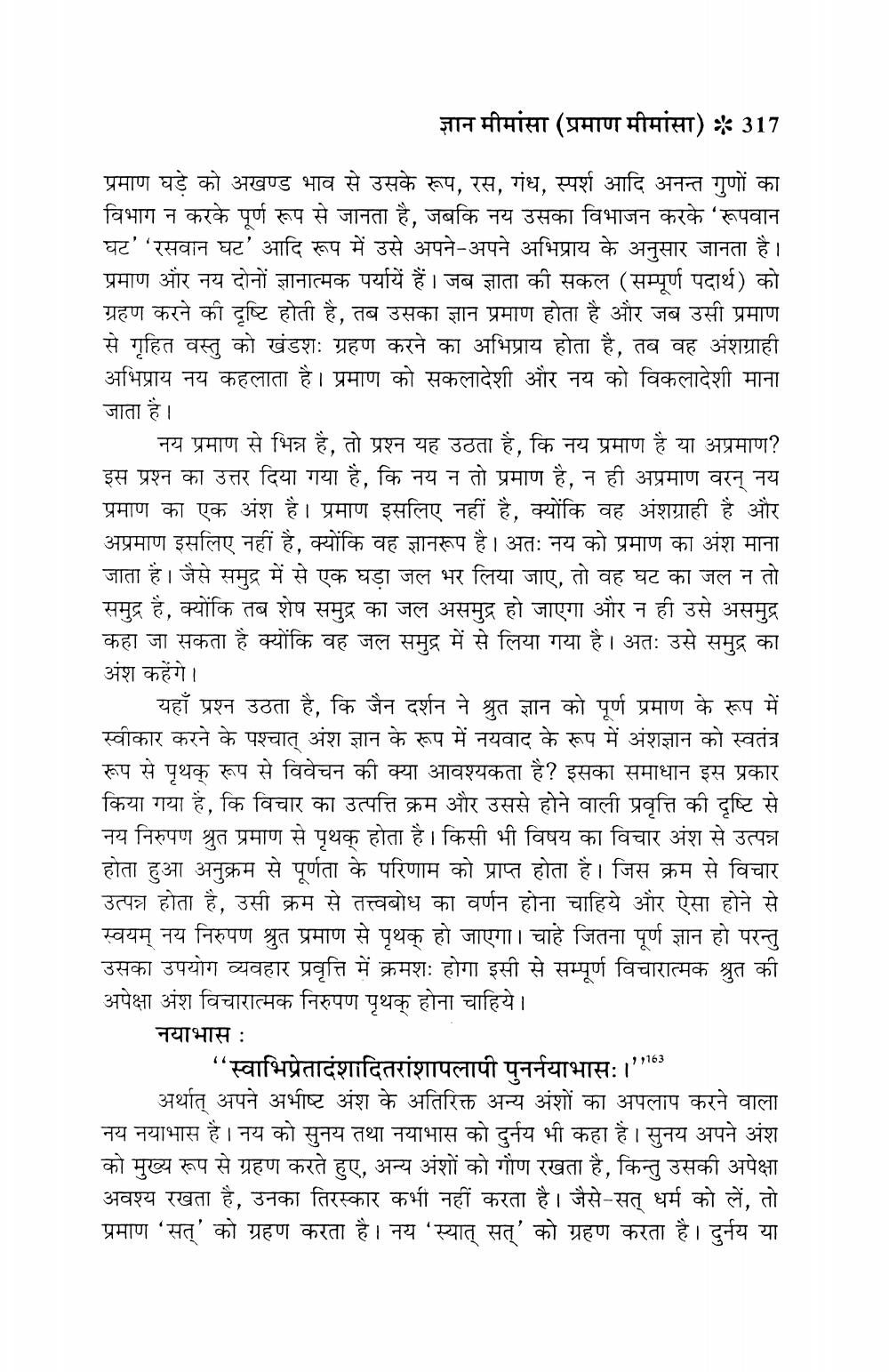________________
ज्ञान मीमांसा (प्रमाण मीमांसा)* 317
प्रमाण घड़े को अखण्ड भाव से उसके रूप, रस, गंध, स्पर्श आदि अनन्त गुणों का विभाग न करके पूर्ण रूप से जानता है, जबकि नय उसका विभाजन करके 'रूपवान घट' 'रसवान घट' आदि रूप में उसे अपने-अपने अभिप्राय के अनुसार जानता है। प्रमाण और नय दोनों ज्ञानात्मक पर्यायें हैं। जब ज्ञाता की सकल (सम्पूर्ण पदार्थ) को ग्रहण करने की दृष्टि होती है, तब उसका ज्ञान प्रमाण होता है और जब उसी प्रमाण से गृहित वस्तु को खंडशः ग्रहण करने का अभिप्राय होता है, तब वह अंशग्राही अभिप्राय नय कहलाता है। प्रमाण को सकलादेशी और नय को विकलादेशी माना जाता है।
नय प्रमाण से भिन्न है, तो प्रश्न यह उठता है, कि नय प्रमाण है या अप्रमाण? इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है, कि नय न तो प्रमाण है, न ही अप्रमाण वरन् नय प्रमाण का एक अंश है। प्रमाण इसलिए नहीं है, क्योंकि वह अंशग्राही है और अप्रमाण इसलिए नहीं है, क्योंकि वह ज्ञानरूप है। अतः नय को प्रमाण का अंश माना जाता है। जैसे समुद्र में से एक घड़ा जल भर लिया जाए, तो वह घट का जल न तो समुद्र है, क्योंकि तब शेष समुद्र का जल असमुद्र हो जाएगा और न ही उसे असमुद्र कहा जा सकता है क्योंकि वह जल समुद्र में से लिया गया है। अतः उसे समुद्र का अंश कहेंगे।
यहाँ प्रश्न उठता है, कि जैन दर्शन ने श्रुत ज्ञान को पूर्ण प्रमाण के रूप में स्वीकार करने के पश्चात् अंश ज्ञान के रूप में नयवाद के रूप में अंशज्ञान को स्वतंत्र रूप से पृथक् रूप से विवेचन की क्या आवश्यकता है? इसका समाधान इस प्रकार किया गया है, कि विचार का उत्पत्ति क्रम और उससे होने वाली प्रवृत्ति की दृष्टि से नय निरुपण श्रुत प्रमाण से पृथक् होता है। किसी भी विषय का विचार अंश से उत्पन्न होता हुआ अनुक्रम से पूर्णता के परिणाम को प्राप्त होता है। जिस क्रम से विचार उत्पन्न होता है, उसी क्रम से तत्त्वबोध का वर्णन होना चाहिये और ऐसा होने से स्वयम् नय निरुपण श्रुत प्रमाण से पृथक् हो जाएगा। चाहे जितना पूर्ण ज्ञान हो परन्तु उसका उपयोग व्यवहार प्रवृत्ति में क्रमशः होगा इसी से सम्पूर्ण विचारात्मक श्रुत की अपेक्षा अंश विचारात्मक निरुपण पृथक् होना चाहिये। नयाभास :
"स्वाभिप्रेतादशादितरांशापलापी पुनर्नयाभासः।13 अर्थात् अपने अभीष्ट अंश के अतिरिक्त अन्य अंशों का अपलाप करने वाला नय नयाभास है। नय को सुनय तथा नयाभास को दुर्नय भी कहा है। सुनय अपने अंश को मुख्य रूप से ग्रहण करते हुए, अन्य अंशों को गौण रखता है, किन्तु उसकी अपेक्षा अवश्य रखता है, उनका तिरस्कार कभी नहीं करता है। जैसे-सत् धर्म को लें, तो प्रमाण 'सत्' को ग्रहण करता है। नय ‘स्यात् सत्' को ग्रहण करता है। दुर्नय या